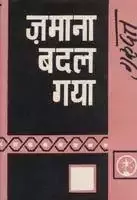|
बहुभागीय पुस्तकें >> जमाना बदल गया - भाग 1 जमाना बदल गया - भाग 1गुरुदत्त
|
361 पाठक हैं |
||||||
सन् 1857 से सन् 1957 के बीच के भारतीय जीवन पर आधारित उपन्यास...
इस पुस्तक का सेट खरीदें।
प्रस्तुत हैं पुस्तक के कुछ अंश
भूमिका
एक कवि ने लिखा है :
तू भी बदल फलक कि ज़माना बदल गया।
वह कह रहा है कि हे भगवान् ! तू भी बदल। अर्थात् हमारे भाग्य को बदल, क्योंकि सब कुछ बदल गया है।
भगवान् हमारे भाग्य को बदलेगा अथवा नहीं, पता नहीं, परन्तु ज़माना तो बदल ही रहा है। क्यों ? इसलिए कि हम बदल रहे हैं।
हमारे बदलने में भी एक कारण है। इसी कारण’ की विवेचना में यह पुस्तक लिखी गयी है।
ऐसा माना जाता है कि भारत प्राचीन काल में एक उन्नत देश था। यहां के रहने वाले, कम से कम चरित्र में, संसार के अन्य पुरुषों से बहुत श्रेष्ठ थे। उस काल के मनुष्यों से भी और आजकल के मनुष्यों से भी। साथ ही इस कथन में संदेह किया जाता है कि भौतिक दृष्टि से भारत एक पिछड़ा हुआ देश था तथा आज का संसार और भारत प्राचीन काल के भारत से बहुत आगे निकल चुका है।
इस विषय में हमारा यह मत है कि भौतिक उन्नति आवश्यकता की देन है। एक मनुष्य जब किसी आवश्यकता को अनुभव करता है तो फिर उस वस्तु की प्राप्ति के लिए यत्न करता है। मानव असीम शक्ति का स्वामी होते हुए भी उन वस्तुओं को प्राप्त कर लेता है। भौतिक वैभव और शारीरिक सुख-सुविधाओं की जब आवश्यकता हुई तो उसके लिए यत्न किया गया और जहां-जहां जिस-जिसने भी यत्न किया, वह सफलता पा गया। प्राचीन भारत के रहने वाले बहुत कम सुख-सुविधाओं की इच्छा करते थे। उन्होंने इसके लिए यत्न नहीं किया और उन सुख-सुविधाओं के साधन उनको प्राप्त नहीं हुए।
हमारा प्राचीन तत्त्व दर्शन (फिलासफी) इस कथन का प्रमाण है। प्राचीन काल के विद्वान क्या चाहते थे, वह उस जीवन की मीमांसा से प्रकट होता है जो उस समय के ग्रन्थों में वर्णित है। कुछ विद्वानों का मत है कि आवश्यकताएं जीवन-मीमांसा की निर्माण करती हैं। परन्तु यह बात सत्य नहीं। आवश्यकताओं की उपज इच्छा से है। इच्छाएं मन में पैदा होती हैं। यह ठीक है कि इंद्रियों से अनुभव किया अभाव ही मन में इच्छाओं को उत्पन्न करता है। परन्तु प्राचीन आर्य विद्वानों ने तो इन्द्रिय दमन के सिद्धान्त का आविष्कार कर और उनके लाभों को अनुभव कर इन्द्रियों द्वारा अनुभूत अभाव की अवहेलना करके दिखा दी थी। शरीर कोमल गद्दों पर लेटने की इच्छा करता है, परन्तु एक आर्य-मीमांसक यह विचार करता है कि कोमल गद्दों पर सोने से वह प्रातः ब्रह्ममुहूर्त में नहीं उठ सकेगा और उस समय के योग-ध्यान तथा चिन्तन से वंचित रह जाएगा। उसकी विचार शक्ति शारीरिक सुख-प्राप्ति की इच्छा पर विजय पा जाती है और वह गद्दों के सुख की इच्छा को छोड़ तख्तपोश’ पर सोने लगाता है। सांसारिक सुखों को त्याग कर वह वन में चला जाता है।
कहने का अभिप्राय यह है कि भौतिक उन्नति की आवश्यकता उत्पन्न नहीं की गई और उसके लिए यत्न नहीं किया गया। भारत उस दिशा में पिछड़ा हुआ है। यह पिछड़ापन ठीक था अथवा गलत, एक भिन्न प्रश्न है। हम तो यह मानते हैं कि भारत का भौतिक विकास में पिछड़ा जाना इसकी अयोग्यता के कारण नहीं था, प्रत्युत् इसकी इच्छा के अनुरूप था।
एक मत यह है कि भौतिक उन्नति की अनिच्छा और इस दिशा में उन्नति का अभाव भारत में सदा नहीं रहा। इसमें भी सच्चाई प्रतीत होती है। यदि आर्य लोग संसार की अन्य जातियों की अपेक्षा प्राचीन काल में भी पिछड़े हुए होते तो उनमें अनेकानेक चक्रवर्ती सम्राट, जो भू-मण्डल को विजय करते रहे थे, न हो सकते। इसके साथ ही हम इतने लम्बे काल तक संसार की अन्य जातियों से संघर्ष में जीवित न रह सकते।
तू भी बदल फलक कि ज़माना बदल गया।
वह कह रहा है कि हे भगवान् ! तू भी बदल। अर्थात् हमारे भाग्य को बदल, क्योंकि सब कुछ बदल गया है।
भगवान् हमारे भाग्य को बदलेगा अथवा नहीं, पता नहीं, परन्तु ज़माना तो बदल ही रहा है। क्यों ? इसलिए कि हम बदल रहे हैं।
हमारे बदलने में भी एक कारण है। इसी कारण’ की विवेचना में यह पुस्तक लिखी गयी है।
ऐसा माना जाता है कि भारत प्राचीन काल में एक उन्नत देश था। यहां के रहने वाले, कम से कम चरित्र में, संसार के अन्य पुरुषों से बहुत श्रेष्ठ थे। उस काल के मनुष्यों से भी और आजकल के मनुष्यों से भी। साथ ही इस कथन में संदेह किया जाता है कि भौतिक दृष्टि से भारत एक पिछड़ा हुआ देश था तथा आज का संसार और भारत प्राचीन काल के भारत से बहुत आगे निकल चुका है।
इस विषय में हमारा यह मत है कि भौतिक उन्नति आवश्यकता की देन है। एक मनुष्य जब किसी आवश्यकता को अनुभव करता है तो फिर उस वस्तु की प्राप्ति के लिए यत्न करता है। मानव असीम शक्ति का स्वामी होते हुए भी उन वस्तुओं को प्राप्त कर लेता है। भौतिक वैभव और शारीरिक सुख-सुविधाओं की जब आवश्यकता हुई तो उसके लिए यत्न किया गया और जहां-जहां जिस-जिसने भी यत्न किया, वह सफलता पा गया। प्राचीन भारत के रहने वाले बहुत कम सुख-सुविधाओं की इच्छा करते थे। उन्होंने इसके लिए यत्न नहीं किया और उन सुख-सुविधाओं के साधन उनको प्राप्त नहीं हुए।
हमारा प्राचीन तत्त्व दर्शन (फिलासफी) इस कथन का प्रमाण है। प्राचीन काल के विद्वान क्या चाहते थे, वह उस जीवन की मीमांसा से प्रकट होता है जो उस समय के ग्रन्थों में वर्णित है। कुछ विद्वानों का मत है कि आवश्यकताएं जीवन-मीमांसा की निर्माण करती हैं। परन्तु यह बात सत्य नहीं। आवश्यकताओं की उपज इच्छा से है। इच्छाएं मन में पैदा होती हैं। यह ठीक है कि इंद्रियों से अनुभव किया अभाव ही मन में इच्छाओं को उत्पन्न करता है। परन्तु प्राचीन आर्य विद्वानों ने तो इन्द्रिय दमन के सिद्धान्त का आविष्कार कर और उनके लाभों को अनुभव कर इन्द्रियों द्वारा अनुभूत अभाव की अवहेलना करके दिखा दी थी। शरीर कोमल गद्दों पर लेटने की इच्छा करता है, परन्तु एक आर्य-मीमांसक यह विचार करता है कि कोमल गद्दों पर सोने से वह प्रातः ब्रह्ममुहूर्त में नहीं उठ सकेगा और उस समय के योग-ध्यान तथा चिन्तन से वंचित रह जाएगा। उसकी विचार शक्ति शारीरिक सुख-प्राप्ति की इच्छा पर विजय पा जाती है और वह गद्दों के सुख की इच्छा को छोड़ तख्तपोश’ पर सोने लगाता है। सांसारिक सुखों को त्याग कर वह वन में चला जाता है।
कहने का अभिप्राय यह है कि भौतिक उन्नति की आवश्यकता उत्पन्न नहीं की गई और उसके लिए यत्न नहीं किया गया। भारत उस दिशा में पिछड़ा हुआ है। यह पिछड़ापन ठीक था अथवा गलत, एक भिन्न प्रश्न है। हम तो यह मानते हैं कि भारत का भौतिक विकास में पिछड़ा जाना इसकी अयोग्यता के कारण नहीं था, प्रत्युत् इसकी इच्छा के अनुरूप था।
एक मत यह है कि भौतिक उन्नति की अनिच्छा और इस दिशा में उन्नति का अभाव भारत में सदा नहीं रहा। इसमें भी सच्चाई प्रतीत होती है। यदि आर्य लोग संसार की अन्य जातियों की अपेक्षा प्राचीन काल में भी पिछड़े हुए होते तो उनमें अनेकानेक चक्रवर्ती सम्राट, जो भू-मण्डल को विजय करते रहे थे, न हो सकते। इसके साथ ही हम इतने लम्बे काल तक संसार की अन्य जातियों से संघर्ष में जीवित न रह सकते।
कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी
हमारा इसमें यह मत है और इसके प्राचीन इतिहास में प्रचुर मात्रा में
प्रमाण भी मिलते हैं कि भारत जहां तत्त्व-दर्शन की दृष्टि से संसार के
अन्य देशों की अपेक्षा बहुत उन्नत था, वहां भौतिक उन्नति की दृष्टि से भी
अन्य देशों की अपेक्षा बढ़ा हुआ था। यह कहना तो कठिन है कि वर्तमान युगीन
भौतिक उन्नति से आगे था या नहीं ? इतना तो निश्चय ही है कि असुरों और
दानवों को सदा पराजित करने वाले भौतिक विकास में उनसे अधिक ही उन्नत रहे
होंगे।
कदाचित् आज जितनी उन्नति इस देश में न हुई हो। इसमें भी देश की अयोग्यता कारण नहीं थी, प्रत्युत आवश्यकता का न होना ही कारण था। आर्य-मीमांसा में तपस्या के जीवन की बहुत महिमा रही है और भौतिक सुख-सुविधाएं तपस्या में बाधक मानी जाती रही हैं। अतः इनकी प्राप्ति उसी सीमा तक वांछनीय मानी गई थी, जितने से व्यक्ति अथवा समाज का जीवन चल सके। जब-जब भी समाज पर विपत्ति आई, तब-तब ही भौतिक उन्नति की ओर ध्यान गया और उसमें उतनी उन्नति कर ली गई, जितनी उस विपत्ति को टालने के लिए आवश्यक थी। जब जितनी उन्नति से विपत्ति टल गई, उतनी उन्नति कर आध्यात्मिक उन्नति में संलग्न हो गए। यह रही है जीवन-मीमांसा भारत के प्राचीन आर्यों की। उस समय आर्यों के विपक्षी इतने प्रबल और सुख-सुविधा सम्पन्न नहीं थे, जितने के आज के यूरोपियन तथा अमेरिकन हो गए हैं। आज उनसे अपने को सुरक्षित और अप्रभावित रखने के लिए उनसे भी अधिक उन्नत होने की आवश्यकता है। उस काल में विपक्षी इतने प्रबल नहीं थे, अतः उस समय इतनी उन्नति की आवश्यकता थी ही नहीं।
दुर्घटना यह हुई की भारत के इतिहास में एक ऐसा समय आ गया जब आत्मा, मन और शरीर के विकास में संतुलन टूट गया। तब भारत संसार की अन्य जातियों की अपेक्षा भौतिक उन्नति से पिछड़ गया। भारत देश पर विपत्ति भी आई। परन्तु हमने इस विपत्ति को टालने के लिए भी भौतिक उन्नति करने की ओर ध्यान नहीं दिया। परिणाम यह हुआ कि सात सौ वर्ष हमने मुसलमानों की दासता में व्यतीत किए और लगभग दो सौ वर्ष तक हम अंग्रेजों के दमन-चक्र में पिसते रहे।
यह दुर्घटना कैसे हुई ? यह दुःखद् कथा है। महाभारत काल के अनन्तर ढाई हज़ार वर्ष तक भारत चैन की बंशी बजाता रहा। उस काल में दुर्भाग्य से दो जीवन-मीमांसाएं ऐसी उत्पन्न होकर पनपीं, जिन्होंने देश के विद्वानों का मानसिक संतुलन जर्जर करके रख दिया। वे मीमांसाएं थीं बौद्ध और जैन जीवन-मीमांसाएं। महात्मा बुद्ध तथा महावीर स्वामी की अपनी शिक्षा क्या थी और क्या नहीं थी, इसमें मतभेद उत्पन्न हो सकता है, परन्तु जैनधर्म और बौद्धधर्म जिस रूप में प्रचलित हुए, वे मानसिक संतुलन को तोड़ने वाले सिद्ध हुए।
इन मतों से जो विशेष बात हुई, वह यह कि आर्य शास्त्रों की धुरी अर्थात् वेद की अवहेलना की गई। वेद से सम्बन्ध विच्छेद हुआ तो उन सब शास्त्रों से भी सम्बन्ध टूटा जो वेदों को आधार मानकर लिखे गए थे। मनु इत्यादि की स्मृतियां भी अस्वीकार हो गईं। अन्य अनेकों शास्त्र विद्याओं को पढ़ना-लिखना बंद हो गया।
यहां इतना समझ लेना चाहिए कि शास्त्र के अर्थ ज्ञान-विज्ञान की पुस्तकें हैं। उस समय का रसायनशास्त्र, चिकित्साशास्त्र, ज्योतिष और कला-कौशल सम्बन्धी शास्त्र वेद ज्ञान से सम्बन्धित थे। जब बौद्ध और जैनियों ने इन वेदों की अवहेलना की तो ये शास्त्र भी जीवन-चर्या से बाहर हो गए।
बौद्ध तथा जैनमत द्वारा एक यह बात भी प्रसिद्ध की गई कि महात्मा बुद्ध अथवा महावीर स्वामी से पहले अन्धकार था; ये महापुरुष ही प्रकाश देने वाले हुए हैं; और पीछे आने वाली सब विचारों की परख के लिए वे कसौटी हो गए। इससे वह पूर्ण ज्ञान भण्डार, जो वेदों के काल से वंचित हो रहा था, अस्वीकृत हो गया और नया ज्ञान उस गति से निर्माण नहीं हो सका, जिस गति से इसकी आवश्यकता थी।
बौद्ध मतानुयायियों ने तो पढ़ने-पढ़ाने में भी अरुचि उत्पन्न करने का यत्न किया। ब्राह्मणों अर्थात् वेदों के ज्ञाता विद्वानों की निंदा की गई। यह निंदा उनकी ओर से की गई, जिन्होंने वेद के दर्शन भी नहीं किए थे।
सबसे बड़ी बात यह हुई कि तपस्या की महिमा की भी निंदा की गई। जहां बुद्ध को तपस्या कराने वाले तपस्या का गलत अर्थ जानते थे और उन्होंने तपस्या से शरीर के विनाश का मार्ग बताया था, वहां बुद्ध ने सब प्रकार की तपस्या को ही निंदनीय बता दिया।
देश में भिक्षुओं की संख्या असीम हो गई। महाराजा अशोक को इन भिक्षुओं के निवास के लिए चौरासी हज़ार विहार निर्माण करने की आवश्यकता पड़ गई। जैन पंथ इतना विनाशकारी नहीं था, जितना बौद्ध-पंथ। उसमें मुख्य कारण यह था कि बौद्धों में ज्ञान से ऊपर कर्म की श्रेष्ठता को माना गया था।
बौद्धकालीन वेद-निन्दकों की प्रतिक्रिया नवीन वेदांती श्री गौड़-पादाचार्य ने उपस्थित की। ये श्री शंकराचार्य के दादा गुरु थे। अपने दादा गुरु के मत का बृहत् प्रचार शंकराचार्य ने किया। श्री स्वामी शंकराचार्य ने एक बात और की। अपने दादा गुरू के मत को भगवद्गीता, उपनिषद् एवं ब्रह्मसूत्रों में से निकालने का उन्होंने यत्न किया।
नवीन वेदान्त के मुख्य चार सिद्धान्त हैं—प्रथम यह कि ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या, जीवो ब्रह्मैव नाऽपराः’। द्वितीय—नैषा तर्केण मतिरापनेया। तृतीय, ज्ञानकर्मणोर्विरोधं पर्वतवदकम्पयं यथोक्तं और चतुर्थ यह कि न जीविते मरणे वा गृधिं कुर्वीतारण्यमियादिति च पद्मं, ततो न पुनरियात् इति संन्यासशासनात्’
ये चारों सिद्धांत अवैदिक हैं। ये भारत में ज्ञानहीनता, कर्मों के लिए अनुत्तरदायित्व, बुद्धि के स्थान पर निष्ठा की स्थापना और मनुष्य को प्रत्येक आयु में ही संन्यास की प्रेरणा देने वाले सिद्ध हुए। दुर्भाग्य से ये चारों सिद्धान्त तत्कालीन भारतीय समाज में इतने प्रचारित हुए कि विद्वान तो संसार को छोड़ वनों को चल पड़े, गृहस्थी प्रत्येक प्रकार के खोटे कर्मों में लीन हो उसका उत्तरदायित्व स्वीकार करने से इन्कार कर बैठे। कुछ जो कर्मों से ऊब गए थे, बुद्धि का प्रयोग छोड़ पत्थर की मूर्तियों में ही भगवान की निष्ठा बना बैठे। और छोटे-छोटे बच्चे छोटी-छोटी अवस्था में ही साधु बनने लगे तथा युवावस्था प्राप्त होने पर अनाचार करने लगे।
मन, आत्मा तथा शरीर का संतुलन टूट गया और देश पराधीन हो गया। पराधीन होने पर भी जगत् मिथ्या, जगत् मिथ्या की कूक लगाते हुए विचारक समाज को दासता में भी आनन्द का आभास कराने का यत्न करते रहे। भारतीय मानव में शारीरिक, मानसिक और आत्मिक पतन आरम्भ हुआ और एक सहस्र वर्ष के लगभग दासता की श्रृंखलाओं में बंधे रहने पर भी, वह अपने को देवता मानता रहा। इस मिथ्या वातावरण में मानव सो गया।
सोयी हुई आत्मा जागी और समाज ने करवट ली। परन्तु अभी भी भारतीय मानव बाहरी समाज को देख चकाचौंध हो रहा है और संतुलित अवस्था को प्राप्त नहीं कर सका है।
भौतिक उन्नति, जो सोते समय भारत के पड़ोसी देशों ने की है, को देख हम पागल हो उनके पीछे भाग पड़े हैं और शरीर, मन तथा आत्मा का संतुलन नहीं पा सके हैं। यही कारण है कि जहां हम ऐटामिक शक्ति को प्राप्त कर रहे हैं, वहां आज ऐटामिक शक्ति वाले देशों की हीन मानसिक अवस्था तथा सोयी हुई आत्मा को भी ग्रहण कर रहे हैं।
सन् 1857 से कथा आरम्भ करके 1957 तक क्या हुआ, इन घटनाओं की पृष्ठभूमि में, पशुता तथा मानवता में संघर्ष का चित्रण करने का यत्न किया गया है। इस भारतीय समाज में मानवता की हत्या और पशुता की उन्नति में किन-किन वस्तुओं ने सहायता की है, उसका दिग्दर्शन कराने का यत्न किया गया है। क्या हम 1857 से आगे निकल गए हैं तो किस दसा में ? यह एक समस्या है। इस कथा में इसी पर प्रकाश डालने का यत्न किया गया है। घटनाओं का चित्रण इतिहास, किवदन्तियों और स्वयं देखी बातों के आधार पर किया है।
इस लम्बे काल की कथा का यह प्रथम अंश है। इसमें 1857 से 1907 तक के राजनीतिक, धार्मिक तथा सामाजिक परिवर्तनों का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत है। विवरण को अधिक-से-अधिक व्यापक करने का यत्न किया गया है। इस पर भी यह इतिहास की पुस्तक न होने से पूर्ण नहीं है, भाव अवश्य पूर्ण हैं। मानव का ह्रास द्रुतगति से हुआ है। आर्थिक तथा राजनीतिक उन्नति भी मानव ह्रास को रोक नहीं सकी। यही इस काल में हुआ और हो रहा है।
यह उपन्यास है। इसको तथ्य से संयुक्त रख अधिक-से-अधिक रोचक बनाने का यत्न किया गया है।
देश के कुछ महात्माओं का उल्लेख इसमें आया है। परन्तु यह उनकी जीवन कथा नहीं है। बदलते ज़माने का दर्शन कराने के लिए उनका यत्र-तत्र उल्लेख मात्र ही है। किसी महापुरुष अथवा किसी मत-मतांतर के मान-अपमान करने का उद्देश्य भी नहीं है। सब घटनाओं पर तटस्थ रह कर विवेचना करने का यत्न किया गया है।
शेष तो अपने पाठकों के विचार करने की बात है।
कदाचित् आज जितनी उन्नति इस देश में न हुई हो। इसमें भी देश की अयोग्यता कारण नहीं थी, प्रत्युत आवश्यकता का न होना ही कारण था। आर्य-मीमांसा में तपस्या के जीवन की बहुत महिमा रही है और भौतिक सुख-सुविधाएं तपस्या में बाधक मानी जाती रही हैं। अतः इनकी प्राप्ति उसी सीमा तक वांछनीय मानी गई थी, जितने से व्यक्ति अथवा समाज का जीवन चल सके। जब-जब भी समाज पर विपत्ति आई, तब-तब ही भौतिक उन्नति की ओर ध्यान गया और उसमें उतनी उन्नति कर ली गई, जितनी उस विपत्ति को टालने के लिए आवश्यक थी। जब जितनी उन्नति से विपत्ति टल गई, उतनी उन्नति कर आध्यात्मिक उन्नति में संलग्न हो गए। यह रही है जीवन-मीमांसा भारत के प्राचीन आर्यों की। उस समय आर्यों के विपक्षी इतने प्रबल और सुख-सुविधा सम्पन्न नहीं थे, जितने के आज के यूरोपियन तथा अमेरिकन हो गए हैं। आज उनसे अपने को सुरक्षित और अप्रभावित रखने के लिए उनसे भी अधिक उन्नत होने की आवश्यकता है। उस काल में विपक्षी इतने प्रबल नहीं थे, अतः उस समय इतनी उन्नति की आवश्यकता थी ही नहीं।
दुर्घटना यह हुई की भारत के इतिहास में एक ऐसा समय आ गया जब आत्मा, मन और शरीर के विकास में संतुलन टूट गया। तब भारत संसार की अन्य जातियों की अपेक्षा भौतिक उन्नति से पिछड़ गया। भारत देश पर विपत्ति भी आई। परन्तु हमने इस विपत्ति को टालने के लिए भी भौतिक उन्नति करने की ओर ध्यान नहीं दिया। परिणाम यह हुआ कि सात सौ वर्ष हमने मुसलमानों की दासता में व्यतीत किए और लगभग दो सौ वर्ष तक हम अंग्रेजों के दमन-चक्र में पिसते रहे।
यह दुर्घटना कैसे हुई ? यह दुःखद् कथा है। महाभारत काल के अनन्तर ढाई हज़ार वर्ष तक भारत चैन की बंशी बजाता रहा। उस काल में दुर्भाग्य से दो जीवन-मीमांसाएं ऐसी उत्पन्न होकर पनपीं, जिन्होंने देश के विद्वानों का मानसिक संतुलन जर्जर करके रख दिया। वे मीमांसाएं थीं बौद्ध और जैन जीवन-मीमांसाएं। महात्मा बुद्ध तथा महावीर स्वामी की अपनी शिक्षा क्या थी और क्या नहीं थी, इसमें मतभेद उत्पन्न हो सकता है, परन्तु जैनधर्म और बौद्धधर्म जिस रूप में प्रचलित हुए, वे मानसिक संतुलन को तोड़ने वाले सिद्ध हुए।
इन मतों से जो विशेष बात हुई, वह यह कि आर्य शास्त्रों की धुरी अर्थात् वेद की अवहेलना की गई। वेद से सम्बन्ध विच्छेद हुआ तो उन सब शास्त्रों से भी सम्बन्ध टूटा जो वेदों को आधार मानकर लिखे गए थे। मनु इत्यादि की स्मृतियां भी अस्वीकार हो गईं। अन्य अनेकों शास्त्र विद्याओं को पढ़ना-लिखना बंद हो गया।
यहां इतना समझ लेना चाहिए कि शास्त्र के अर्थ ज्ञान-विज्ञान की पुस्तकें हैं। उस समय का रसायनशास्त्र, चिकित्साशास्त्र, ज्योतिष और कला-कौशल सम्बन्धी शास्त्र वेद ज्ञान से सम्बन्धित थे। जब बौद्ध और जैनियों ने इन वेदों की अवहेलना की तो ये शास्त्र भी जीवन-चर्या से बाहर हो गए।
बौद्ध तथा जैनमत द्वारा एक यह बात भी प्रसिद्ध की गई कि महात्मा बुद्ध अथवा महावीर स्वामी से पहले अन्धकार था; ये महापुरुष ही प्रकाश देने वाले हुए हैं; और पीछे आने वाली सब विचारों की परख के लिए वे कसौटी हो गए। इससे वह पूर्ण ज्ञान भण्डार, जो वेदों के काल से वंचित हो रहा था, अस्वीकृत हो गया और नया ज्ञान उस गति से निर्माण नहीं हो सका, जिस गति से इसकी आवश्यकता थी।
बौद्ध मतानुयायियों ने तो पढ़ने-पढ़ाने में भी अरुचि उत्पन्न करने का यत्न किया। ब्राह्मणों अर्थात् वेदों के ज्ञाता विद्वानों की निंदा की गई। यह निंदा उनकी ओर से की गई, जिन्होंने वेद के दर्शन भी नहीं किए थे।
सबसे बड़ी बात यह हुई कि तपस्या की महिमा की भी निंदा की गई। जहां बुद्ध को तपस्या कराने वाले तपस्या का गलत अर्थ जानते थे और उन्होंने तपस्या से शरीर के विनाश का मार्ग बताया था, वहां बुद्ध ने सब प्रकार की तपस्या को ही निंदनीय बता दिया।
देश में भिक्षुओं की संख्या असीम हो गई। महाराजा अशोक को इन भिक्षुओं के निवास के लिए चौरासी हज़ार विहार निर्माण करने की आवश्यकता पड़ गई। जैन पंथ इतना विनाशकारी नहीं था, जितना बौद्ध-पंथ। उसमें मुख्य कारण यह था कि बौद्धों में ज्ञान से ऊपर कर्म की श्रेष्ठता को माना गया था।
बौद्धकालीन वेद-निन्दकों की प्रतिक्रिया नवीन वेदांती श्री गौड़-पादाचार्य ने उपस्थित की। ये श्री शंकराचार्य के दादा गुरु थे। अपने दादा गुरु के मत का बृहत् प्रचार शंकराचार्य ने किया। श्री स्वामी शंकराचार्य ने एक बात और की। अपने दादा गुरू के मत को भगवद्गीता, उपनिषद् एवं ब्रह्मसूत्रों में से निकालने का उन्होंने यत्न किया।
नवीन वेदान्त के मुख्य चार सिद्धान्त हैं—प्रथम यह कि ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या, जीवो ब्रह्मैव नाऽपराः’। द्वितीय—नैषा तर्केण मतिरापनेया। तृतीय, ज्ञानकर्मणोर्विरोधं पर्वतवदकम्पयं यथोक्तं और चतुर्थ यह कि न जीविते मरणे वा गृधिं कुर्वीतारण्यमियादिति च पद्मं, ततो न पुनरियात् इति संन्यासशासनात्’
ये चारों सिद्धांत अवैदिक हैं। ये भारत में ज्ञानहीनता, कर्मों के लिए अनुत्तरदायित्व, बुद्धि के स्थान पर निष्ठा की स्थापना और मनुष्य को प्रत्येक आयु में ही संन्यास की प्रेरणा देने वाले सिद्ध हुए। दुर्भाग्य से ये चारों सिद्धान्त तत्कालीन भारतीय समाज में इतने प्रचारित हुए कि विद्वान तो संसार को छोड़ वनों को चल पड़े, गृहस्थी प्रत्येक प्रकार के खोटे कर्मों में लीन हो उसका उत्तरदायित्व स्वीकार करने से इन्कार कर बैठे। कुछ जो कर्मों से ऊब गए थे, बुद्धि का प्रयोग छोड़ पत्थर की मूर्तियों में ही भगवान की निष्ठा बना बैठे। और छोटे-छोटे बच्चे छोटी-छोटी अवस्था में ही साधु बनने लगे तथा युवावस्था प्राप्त होने पर अनाचार करने लगे।
मन, आत्मा तथा शरीर का संतुलन टूट गया और देश पराधीन हो गया। पराधीन होने पर भी जगत् मिथ्या, जगत् मिथ्या की कूक लगाते हुए विचारक समाज को दासता में भी आनन्द का आभास कराने का यत्न करते रहे। भारतीय मानव में शारीरिक, मानसिक और आत्मिक पतन आरम्भ हुआ और एक सहस्र वर्ष के लगभग दासता की श्रृंखलाओं में बंधे रहने पर भी, वह अपने को देवता मानता रहा। इस मिथ्या वातावरण में मानव सो गया।
सोयी हुई आत्मा जागी और समाज ने करवट ली। परन्तु अभी भी भारतीय मानव बाहरी समाज को देख चकाचौंध हो रहा है और संतुलित अवस्था को प्राप्त नहीं कर सका है।
भौतिक उन्नति, जो सोते समय भारत के पड़ोसी देशों ने की है, को देख हम पागल हो उनके पीछे भाग पड़े हैं और शरीर, मन तथा आत्मा का संतुलन नहीं पा सके हैं। यही कारण है कि जहां हम ऐटामिक शक्ति को प्राप्त कर रहे हैं, वहां आज ऐटामिक शक्ति वाले देशों की हीन मानसिक अवस्था तथा सोयी हुई आत्मा को भी ग्रहण कर रहे हैं।
सन् 1857 से कथा आरम्भ करके 1957 तक क्या हुआ, इन घटनाओं की पृष्ठभूमि में, पशुता तथा मानवता में संघर्ष का चित्रण करने का यत्न किया गया है। इस भारतीय समाज में मानवता की हत्या और पशुता की उन्नति में किन-किन वस्तुओं ने सहायता की है, उसका दिग्दर्शन कराने का यत्न किया गया है। क्या हम 1857 से आगे निकल गए हैं तो किस दसा में ? यह एक समस्या है। इस कथा में इसी पर प्रकाश डालने का यत्न किया गया है। घटनाओं का चित्रण इतिहास, किवदन्तियों और स्वयं देखी बातों के आधार पर किया है।
इस लम्बे काल की कथा का यह प्रथम अंश है। इसमें 1857 से 1907 तक के राजनीतिक, धार्मिक तथा सामाजिक परिवर्तनों का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत है। विवरण को अधिक-से-अधिक व्यापक करने का यत्न किया गया है। इस पर भी यह इतिहास की पुस्तक न होने से पूर्ण नहीं है, भाव अवश्य पूर्ण हैं। मानव का ह्रास द्रुतगति से हुआ है। आर्थिक तथा राजनीतिक उन्नति भी मानव ह्रास को रोक नहीं सकी। यही इस काल में हुआ और हो रहा है।
यह उपन्यास है। इसको तथ्य से संयुक्त रख अधिक-से-अधिक रोचक बनाने का यत्न किया गया है।
देश के कुछ महात्माओं का उल्लेख इसमें आया है। परन्तु यह उनकी जीवन कथा नहीं है। बदलते ज़माने का दर्शन कराने के लिए उनका यत्र-तत्र उल्लेख मात्र ही है। किसी महापुरुष अथवा किसी मत-मतांतर के मान-अपमान करने का उद्देश्य भी नहीं है। सब घटनाओं पर तटस्थ रह कर विवेचना करने का यत्न किया गया है।
शेष तो अपने पाठकों के विचार करने की बात है।
-गुरुदत्त
भाग एक
प्रथम परिच्छेद
1
ब्रह्मनाल के शिवालय में जल चढ़ाकर रामरक्खामल्ल घर को आ रहा था। साठ वर्ष
का वृद्ध होते हुए भी, उसकी कमर सीधी थी; छाती चौड़ी, बांहें लम्बी और
ऊंचाई पांच फिट नौ इंच थी। देवता पर चढ़ाने से बची लस्सी का लोटा उसके हाथ
में था। करंडी की चादर नंगे वदन पर लपेटे और रेशमी धोती पहने, पांव में
लकड़ी की खड़ाऊं धारण किये हुए था।
वह खट-खट सड़क पर चला आ रहा था। अभी दिन निकला नहीं था। पूर्व के आकाश पर अरुणिमा, भगवान सूर्य के आगमन की अभी सूचना ही लायी थी। वह सूहा’ बाजार में से चलता हुआ अपनी गली कूचा हिंगना की ओर जा रहा था। दुकानें अभी खुली नहीं थीं। सड़क पर बहुत कम लोग आ-जा रहे थे। अधिकांश आने-जाने वाले प्रातः भ्रमण अथवा स्नान के लिये रावी नदी की ओर लम्बे-लम्बे पग उठाते हुए चले जा रहे थे।
रामरक्खामल्ल अपनी गली में प्रवेश करने लगा तो एक प्रौड़ावस्था का आदमी कुशासन, अंगोछा, लोटा और रूमाली बगल में दबाये गली से निकला और सामने रामरक्खामल्ल को देख उससे बोला, भापा ! राम राम !
नमस्ते भैया !’ रामरक्खामल्ल ने उत्तर में कहा।
वह दूसरा आदमी जानता था कि रामरक्खामल्ल शिवालय में जल चढ़ाकर आया है, परन्तु आर्य समाजियों की भांति नमस्ते कहकर अभिवादन कर रहा है। इससे वह मुस्कराया और चल दिया। वह रावी नदी के किनारे स्नान पूजा के लिए जा रहा था। रामरक्खामल्ल अभी दस कदम ही गया था कि एक अन्य व्यक्ति अपने मकान के दरवाजे को ताला लगाता हुआ मिला। उसकी बगल में भी आसन और हाथ में अंगोछा इत्यादि थे। अब रामरक्खामल्ल ने उससे पूछ लिया, शिवराम ! बहू घर पर नहीं है क्या ?’
है तो, भापा ! पर वह सो रही है और नीचे दरवाजा बन्द करने नहीं आयी। इसी कारण बाहर से ताला लगाकर जा रहा हूं।
तुम्हारा साथी तो चला गया ?’
राधेलाल ?’
नहीं, सोहन। अभी-अभी गली के फाटक के पास मिला था।’
उसने आवाज तो लगाई थी। बहू को जगा न सकने के कारण ताला ढूंढ़ना पड़ा और वह, शायद यह समझ कि मैं नहीं आ रहा, चला गया है। बस अभी भागकर पकड़ लूंगा।’
और राधेलाल ?’
वह सोहनलाल के साथ नहीं था ?’
नहीं।’
तो पहले निकल गया होगा।’
शिवलाल ने राम ! राम !!’ की और गली के बाहर की ओर चल पड़ा। रामरक्खामल्ल अपने घर की ओर चला आया। खट-खट’ खड़ाऊं का शब्द गली की भूमि पर हो रहा था। गली में पक्का फर्श नहीं था। चलने वालों के पांव से मिट्टी फर्श की भांति ठोस हो गयी थी। वर्षा के दिन में अवश्य कीचड़ हो जाता था और थोड़ी भी असावधानी से चलने वाला फिसलकर गिर सकता था।
गली के चौक में कुआं था। कुएं की जगत पर एक ओर स्त्रियों के स्नान के लिए पर्देदार जगह बनी हुई थी और दूसरी ओर खुला स्थान था, जिस पर पुरुष नहाते थे। कुएं से जल निकालने के लिये दो चरखियां लगी थीं। एक पर्दे के भीतर, स्त्रियों के लिये और एक बाहर की ओर पुरुषों के लिये।
रामरक्खामल्ल का मकान चौक के कुएं के ठीक ऊपर ही था। रामरक्खामल्ल कुएं के पास से मकान में जाने लगा तो कुएं की जगत पर बैठे एक स्नान करते युवक ने उसको आवाज दे दी—बड़े भापा ! राम-राम !’
अरे महानारायण ! अभी नहा ही रहे हो ?’
जी ! आज नींद नहीं खुली।’
पांच बज रहे हैं। बेटा ! कुछ पूजा-पाठ, जप-ध्यान कर लिया करो।’
वह मैं दुकान खोलने के बाद कर लेता हूं।’
रामरक्खामल्ल मुस्कराया और घर के भीतर घुस गया। एक स्त्री सिर से पांव तक चादर लपेटे घर की सीढ़ियों पर बुहारी दे रही थी। रामरक्खामल्ल ने कहा, बेटा लाज ! तनिक जल्दी उठा करो।’
लाजवंती रामरक्खामल्ल के भाई विष्णुनारायण की विधवा लड़की थी। उसकी आयु इक्कीस वर्ष के लगभग थी। वह खड़ी हो गई और बोली, बड़े भापा ! आप चलिए, मैं दो मिनट में आई।’
इस प्रकार रामरक्खामल्ल मकान के ऊपर की छत पर जा पहुंचा। घर में एक पूजा-गृह बना था। उसमें एक ओर चौकी पर पीतल के बने ठाकुर रखे थे। उनके आगे फूल चढ़े थे और पीतल की प्याली में घिसा चन्दन रखा था। रामरक्खामल्ल का भाई विष्णुनारायण पूजा-गृह में हवन-कुंड रखे, उसमें समिधा सजा रहा था। हवन-कुंड के एक ओर एक थाली में सामग्री तथा कर्पूर रखा था। समीप एक कटोरे में घी था। एक लोटा जल और एक पात्र आहुति-शेष लेने के लिए भी वहां पर पड़ा था।
रामरक्खामल्ल ने अपना लस्सी का लोटा ठाकुर के सामने चौकी पर रख दिया और स्वयं कुंड के एक ओर आसन पर बैठ गया। उसके बैठते ही दो स्त्रियां आईं। एक विष्णुनारायण के बायें हाथ की ओर वाले आसन पर और दूसरी रामरक्खामल्ल के बायें हाथ की ओर आसन पर बैठ गई। वे इन दोनों भाइयों की पत्नियां थीं।
रामरक्खामल्ल का भाई विष्णुनारायण अधेड़ आयु का व्यक्ति था। चालीस वर्ष की आयु होगी। अभी कुछ ही बाल सफेद हुए थे। रामरक्खामल्ल उससे बीस वर्ष बड़ा था और उसके भी सिर और मूंछों के कई बाल सफेद हो चुके थे।
वह खट-खट सड़क पर चला आ रहा था। अभी दिन निकला नहीं था। पूर्व के आकाश पर अरुणिमा, भगवान सूर्य के आगमन की अभी सूचना ही लायी थी। वह सूहा’ बाजार में से चलता हुआ अपनी गली कूचा हिंगना की ओर जा रहा था। दुकानें अभी खुली नहीं थीं। सड़क पर बहुत कम लोग आ-जा रहे थे। अधिकांश आने-जाने वाले प्रातः भ्रमण अथवा स्नान के लिये रावी नदी की ओर लम्बे-लम्बे पग उठाते हुए चले जा रहे थे।
रामरक्खामल्ल अपनी गली में प्रवेश करने लगा तो एक प्रौड़ावस्था का आदमी कुशासन, अंगोछा, लोटा और रूमाली बगल में दबाये गली से निकला और सामने रामरक्खामल्ल को देख उससे बोला, भापा ! राम राम !
नमस्ते भैया !’ रामरक्खामल्ल ने उत्तर में कहा।
वह दूसरा आदमी जानता था कि रामरक्खामल्ल शिवालय में जल चढ़ाकर आया है, परन्तु आर्य समाजियों की भांति नमस्ते कहकर अभिवादन कर रहा है। इससे वह मुस्कराया और चल दिया। वह रावी नदी के किनारे स्नान पूजा के लिए जा रहा था। रामरक्खामल्ल अभी दस कदम ही गया था कि एक अन्य व्यक्ति अपने मकान के दरवाजे को ताला लगाता हुआ मिला। उसकी बगल में भी आसन और हाथ में अंगोछा इत्यादि थे। अब रामरक्खामल्ल ने उससे पूछ लिया, शिवराम ! बहू घर पर नहीं है क्या ?’
है तो, भापा ! पर वह सो रही है और नीचे दरवाजा बन्द करने नहीं आयी। इसी कारण बाहर से ताला लगाकर जा रहा हूं।
तुम्हारा साथी तो चला गया ?’
राधेलाल ?’
नहीं, सोहन। अभी-अभी गली के फाटक के पास मिला था।’
उसने आवाज तो लगाई थी। बहू को जगा न सकने के कारण ताला ढूंढ़ना पड़ा और वह, शायद यह समझ कि मैं नहीं आ रहा, चला गया है। बस अभी भागकर पकड़ लूंगा।’
और राधेलाल ?’
वह सोहनलाल के साथ नहीं था ?’
नहीं।’
तो पहले निकल गया होगा।’
शिवलाल ने राम ! राम !!’ की और गली के बाहर की ओर चल पड़ा। रामरक्खामल्ल अपने घर की ओर चला आया। खट-खट’ खड़ाऊं का शब्द गली की भूमि पर हो रहा था। गली में पक्का फर्श नहीं था। चलने वालों के पांव से मिट्टी फर्श की भांति ठोस हो गयी थी। वर्षा के दिन में अवश्य कीचड़ हो जाता था और थोड़ी भी असावधानी से चलने वाला फिसलकर गिर सकता था।
गली के चौक में कुआं था। कुएं की जगत पर एक ओर स्त्रियों के स्नान के लिए पर्देदार जगह बनी हुई थी और दूसरी ओर खुला स्थान था, जिस पर पुरुष नहाते थे। कुएं से जल निकालने के लिये दो चरखियां लगी थीं। एक पर्दे के भीतर, स्त्रियों के लिये और एक बाहर की ओर पुरुषों के लिये।
रामरक्खामल्ल का मकान चौक के कुएं के ठीक ऊपर ही था। रामरक्खामल्ल कुएं के पास से मकान में जाने लगा तो कुएं की जगत पर बैठे एक स्नान करते युवक ने उसको आवाज दे दी—बड़े भापा ! राम-राम !’
अरे महानारायण ! अभी नहा ही रहे हो ?’
जी ! आज नींद नहीं खुली।’
पांच बज रहे हैं। बेटा ! कुछ पूजा-पाठ, जप-ध्यान कर लिया करो।’
वह मैं दुकान खोलने के बाद कर लेता हूं।’
रामरक्खामल्ल मुस्कराया और घर के भीतर घुस गया। एक स्त्री सिर से पांव तक चादर लपेटे घर की सीढ़ियों पर बुहारी दे रही थी। रामरक्खामल्ल ने कहा, बेटा लाज ! तनिक जल्दी उठा करो।’
लाजवंती रामरक्खामल्ल के भाई विष्णुनारायण की विधवा लड़की थी। उसकी आयु इक्कीस वर्ष के लगभग थी। वह खड़ी हो गई और बोली, बड़े भापा ! आप चलिए, मैं दो मिनट में आई।’
इस प्रकार रामरक्खामल्ल मकान के ऊपर की छत पर जा पहुंचा। घर में एक पूजा-गृह बना था। उसमें एक ओर चौकी पर पीतल के बने ठाकुर रखे थे। उनके आगे फूल चढ़े थे और पीतल की प्याली में घिसा चन्दन रखा था। रामरक्खामल्ल का भाई विष्णुनारायण पूजा-गृह में हवन-कुंड रखे, उसमें समिधा सजा रहा था। हवन-कुंड के एक ओर एक थाली में सामग्री तथा कर्पूर रखा था। समीप एक कटोरे में घी था। एक लोटा जल और एक पात्र आहुति-शेष लेने के लिए भी वहां पर पड़ा था।
रामरक्खामल्ल ने अपना लस्सी का लोटा ठाकुर के सामने चौकी पर रख दिया और स्वयं कुंड के एक ओर आसन पर बैठ गया। उसके बैठते ही दो स्त्रियां आईं। एक विष्णुनारायण के बायें हाथ की ओर वाले आसन पर और दूसरी रामरक्खामल्ल के बायें हाथ की ओर आसन पर बैठ गई। वे इन दोनों भाइयों की पत्नियां थीं।
रामरक्खामल्ल का भाई विष्णुनारायण अधेड़ आयु का व्यक्ति था। चालीस वर्ष की आयु होगी। अभी कुछ ही बाल सफेद हुए थे। रामरक्खामल्ल उससे बीस वर्ष बड़ा था और उसके भी सिर और मूंछों के कई बाल सफेद हो चुके थे।
|
|||||
अन्य पुस्तकें
लोगों की राय
No reviews for this book