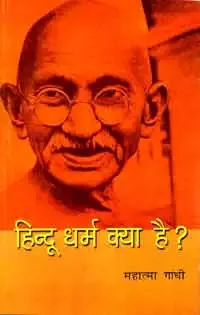|
जीवनी/आत्मकथा >> सत्य के प्रयोग सत्य के प्रयोगमहात्मा गाँधी
|
57 पाठक हैं |
||||||
प्रस्तुत है महात्मा गाँधी की आत्मकथा ....
यहदुःखद घटना तो मेरे दक्षिण अफ्रीका छोड़ने के बाद घटी, पर सार्वजनिकसंस्थाओं के लिए स्थायी कोष रखने के सम्बन्ध में मेरे विचार बदल चुके थे।अनेकानेक सार्वजनिक संस्थाओं की उत्पत्ति और उनके प्रबन्ध की जिम्मेदारीसंभालने के बाद मैं इस ढृढ़ निर्णय पर पहुँचा हूँ कि किसी भी सार्वजनिकसंस्था को स्थायी कोष पर निभने का प्रयत्न नहीं करना चाहिये। इसमे उसकी नैतिक अधोगति का बीज छिपा रहता हैं।
सार्वजनिक संस्था का अर्थ हैं, लोगों की स्वीकृति और लोगों के धन से चलने वाली संस्था। ऐसी संस्थाको जब लोगों की सहायता न मिले तो उसे जीवित रहने का अधिकार ही नहीं रहता। देखा यह गया हैं कि स्थायी सम्पत्ति के भरोसे चलने वाली संस्था लोकमत सेस्वतंत्र हो जाती है और कितनी ही बार वह उल्टा आचरण भी करती हैं। हिन्दुस्तान में हमे पग-पग पर इसका अनुभव होता हैं। कितनी ही धार्मिक मानीजानेवाली संस्थाओं के हिसाब-किताब का कोई ठिकाना नहीं रहता। उनके ट्रस्टीही उनके मालिक बन बैठे है और वे किसी के प्रति उत्तरदायी भी नहीं हैं। जिसतरह प्रकृति स्वयं प्रतिदिन उत्पन्न करती हैं और प्रतिदिन खाती हैं, वैसी ही व्यवस्था सार्वजनिक संस्थाओ की भी होनी चाहिये, इसमे मुझे कोई शंकानहीं हैं। जिस संस्था को लोग मदद देने के लिए तैयार न हो, उसे सार्वजनिक संस्था के रुप में जीवित रहने का अधिकार ही नहीं हैं। प्रतिवर्ष मिलनेवाला चन्दा ही उन संस्थाओ की अपनी लोकप्रियता और उनके संचालको की प्रामाणिकता की कसौटी हैं, और मेरी यह राय हैं कि हर एक संस्था को इसकसौटी पर कसा जाना चाहिये।
मेरे यह लिखने से कोई गलतफहमी न होनी चाहिये। ऊपरी टीका उन संस्थाओं पर लागू नहीं होती, जिन्हे मकान इत्यादि कीआवश्यकता होती हैं। सार्वजनिक संस्थाओ के दैनिक खर्च का आधार लोगों से मिलने वाला चन्दा ही होना चाहिये।
ये विचार दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह के दिनों में ढृढ़ हुए। छह वर्षो की यह महान लड़ाई स्थायी कोषके बिना चली, यद्यपि उसके लिए लाखो रुपयों की आवश्यकता थी। मुझे ऐसे अवसरो की याद है कि जब अगले दिन का खर्च कहाँ से आयेगा, इसकी मुझे खबर न होतीथी। लेकि आगे जिन विषयो की चर्चा की जाने वाली है, उनका उल्लेख यहाँ नहीँ करुँगा। पाठको को मेरे इस मत का समर्थन इस कथा के उचित प्रसंग पर यथास्थानमिल जायेगा।
|
|||||