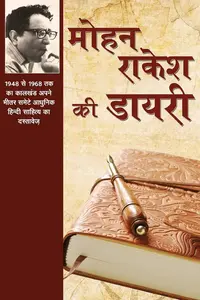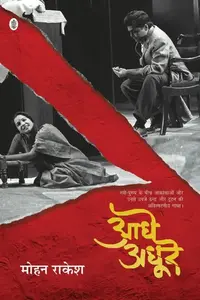|
यात्रा वृत्तांत >> आखिरी चट्टान तक आखिरी चट्टान तकमोहन राकेश
|
320 पाठक हैं |
|||||||
"विचारों की गहराई और यात्रा के अनुभवों का संगम : मोहन राकेश का आख़िरी चट्टान तक यात्रा-वृत्तान्त"
धूप में जिस्म सुखाकर कपड़े पहनने तक मैं पुल के कैनवस को देखता रहा। एक ऊँचा मेहराब जो हर चीज़ को अपनी तरफ़ खींच रहा था-पानी को, नावों को, लोगों को। दो लड़के उस मेहराब के ऊपर से पानी की तरफ झाँक रहे थे। उनमें से एक ने पानी में ढेला फेंका। उससे कुछ छींटें उड़कर मेरे ऊपर पड़े। फिर दूसरे लड़के ने ढेला फेंका। इस बार भी उसी तरह छींटें पड़े। लड़के दो-एक मिनट यह खेलते रहे। फिर दौड़ते हुए पुल से सड़क पर चले गये। मेरे पास की कुछ ज़मीन भी छींटों ये भींग गयी थी। उससे जो गन्ध उठ रही थी, वह इतनी परिचित थी कि मेरी अजनबीपन की अनुभूति कुछ हद तक दूर होने लगी। मैंने गीली मिट्टी को पैर के नाख़ून से थोड़ा कुरेद दिया, फिर ऊपर की तरफ़ एक अनजान कच्चे रास्ते पर चल दिया।
वह रास्ता घरों के बीच से जाती एक गली-सी थी। एक घर के बरामदे में कुछ बच्चे खेल रहे थे। वहीं पास ही एक स्त्री खरल में चावल पीस रही थी। एक युवक फ़र्श पर टाँगें फैलाये अख़बार पढ़ रहा था। यह उस घर की अपनी दोपहर थी। मुझे अपने उस घर की याद आयी जिसमें मेरे बचपन के कई साल गुज़रे थे। उस घर की अपनी ही सुबह, अपनी ही दोपहर और अपनी ही शाम होती थी। सुबह स्कूल जाने की हलचल, दोपहर को रंगीन रोशनदानों से आती धूप की उदासी और शाम को बाहर बैठक में पिताजी के दोस्तों का अभाव। वह सुबह, दोपहर और शाम हमारे घर की संस्कृति थी। अब जिन घरों के पास से गुज़र रहा था उनमें से हर घर की भी अपनी एक अलग संस्कृति थी-रोज़मर्रा के छोटे-छोटे टुकड़ों से बनी संस्कृति जो उस घर के हर व्यक्ति के आज और कल को किसी-न-किसी रूप में निर्धारित कर रही थी-साथ उस पूरे समूह के आज और कल को जिसकी व्यापक संस्कृति का निर्माण इन छोटी-छोटी संस्कृतियों के योग से होता है।
आगे खेत थे। खेतों के साथ मिट्टी की ऊँची मेंड़ें बनी थीं। बरसात से उनकी रक्षा के लिए उन्हें नारियल के पत्तों की चटाइयों से ढँका गया था। सामने मैदान की खुली धूप में एक मज़दूर ईंटें तोड़ रहा था। पास ही तीन-चार ढाँचों जैसे बच्चे, जिनके सिर उनके शरीरों की तुलना में काफ़ी बड़े लगते थे, एक-दूसरे पर रोड़े फेंक रहे थे। उनसे कुछ हटकर एक स्त्री अपना सूखा स्तन बच्चे के मुँह में दिये बार-बार उसके गालों की रूखी चमड़ी को चूम रही थी। यह उस परिवार की अपनी दोपहर थी-एक और छोटी-सी संस्कृति!
रात को अर्णाकुलम् में वहाँ के आम्बलम् का वार्षिकोत्सव था। उस अवसर पर आम्बलम् को चारों ओर से दीयों से सजाया गया था। अन्दर देवालय के चारों ओर की जालियाँ अपने एक-एक झरोखे में टिमटिमाते दीयों की रोशनी में मोम की बनी-सी लग रही थीं। देवालय के सामने का स्वर्ण-स्तम्भ, काँपती लौ के नगीनों से जड़ा, किरणों की डोरियों में गुँथा, अपने और उत्सव के महत्त्व का विज्ञापन कर रहा था। स्तम्भ के आसपास की भीड़ में कुछ देर धक्के खाने के बाद में आम्बलम् के पिछले भाग की ओर चला गया। उधर उस समय और ज्यादा हलचल थी। तीन बड़े-बड़े हाथी सामने आ रहे थे। लोगों की बहुत बड़ी भीड़ उन्हें घेरे थी। हाथी सुनहरे आभूषणों से सजे थे और उनके हौदों के ऊपर भी सुनहरे छत्र लगे थे। बीच के हाथी की पीठ पर मन्दिर के देवता को लाया जा रहा था। वहाँ लोगों से पता चला कि देवता को कई दिन इसी तरह हाथी की पीठ पर मन्दिर के चारों ओर घुमाया जाता है। वह रात आराट् की थी-अर्थात् देवता को जलस्नान कराने की। आराट् के साथ वह उत्सव समाप्त हो जाता था।
|
|||||
- प्रकाशकीय
- समर्पण
- वांडर लास्ट
- दिशाहीन दिशा
- अब्दुल जब्बार पठान
- नया आरम्भ
- रंग-ओ-बू
- पीछे की डोरियाँ
- मनुष्य की एक जाति
- लाइटर, बीड़ी और दार्शनिकता
- चलता जीवन
- वास्को से पंजिम तक
- सौ साल का गुलाम
- मूर्तियों का व्यापारी
- आगे की पंक्तियाँ
- बदलते रंगों में
- हुसैनी
- समुद्र-तट का होटल
- पंजाबी भाई
- मलबार
- बिखरे केन्द्र
- कॉफ़ी, इनसान और कुत्ते
- बस-यात्रा की साँझ
- सुरक्षित कोना
- भास्कर कुरुप
- यूँ ही भटकते हुए
- पानी के मोड़
- कोवलम्
- आख़िरी चट्टान