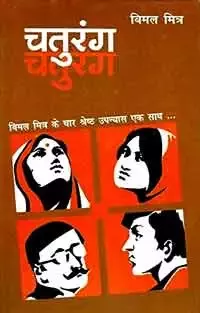|
अतिरिक्त >> रोकड़ जो मिली नहीं रोकड़ जो मिली नहींविमल मित्र
|
122 पाठक हैं |
||||||
रोकड़ जो मिली नहीं पुस्तक का आई पैड संस्करण
आई पैड संस्करण
‘रोकड़ जो मिली नहीं’ वस्तुतः मनुष्य के भाग्य का इतिहास है।
आज के युग में मनुष्य टेकनालॉजी के तर्क से पैसे को ही सब कुछ मानकर किस
प्रकार के अनौतिक कार्य करता है और अन्ततः सुख उसे समृद्धि से नहीं मिलता
है। इस उपन्यास में ‘सोने के हार की चोरी’ की खोज के माध्यम
से मानव की कमजोरियों का रहस्य समझने का प्रयत्न किया गया है ‘ब्लैक
का प्रिंस’ का इतिहास पैसे के पीछे पागल लोगों का इतिहास है। जासूसी
कथा शिल्प के माध्यम से रचनाकार के कलकत्ता महानगर के काले पक्ष को उजागर
करने का आश्चर्यजनक प्रयत्न किया है। कौतूहल मनोरंजन आदि तत्त्वों से
युक्त होने के बावजूद यह ‘रहस्य रोमांच’ से भिन्न एक
साहित्यिक रचना है यही इसका रहस्य है सुनीतिमित्र, झगड़ू और ब्लैक प्रिंस
तो सामाजिक व्यवस्ता के उस पक्ष का परिणाम है जो रोटी के लिए पूँजी की भूख
पैदा करते हैं। अपराधों के सामाजिक और मनोविज्ञानिक कारण क्या हैं यह
पुस्तक पढ़कर समझा जा सकता है, क्योंकि अपराध इसमें स्वयं प्रतीक के रुप
में प्रयुक्त है। वस्तुतः इन्हीं कारणों से पुस्तक रोचक और कौतूहलपरक ही
नहीं शैली की दृष्टि से आकर्षक भी है।
रोकड़ जो मिली नहीं
एक
इस उपन्यास के अन्त में एक चिट्ठी है। उसी चिट्ठी में मेरे इस उपन्यास का
अन्त हुआ है। आप लोग उस चिट्ठी को पहले ही नहीं पढ़ लें। वैसा कीजिएगा तो
कहानी पढ़ने के आनन्द से आप वंचित हो जाइएगा।
तीर्थ के देवता तीर्थ-पथ के अन्त में वास करते हैं। तीर्थ-पथ को तय किये बिना तीर्थ के देवता के दर्शन नहीं होते। तीर्थ यात्रा में चूँकि यातना झेलनी पड़ती है, इसीलिए तीर्थ के देवता का इतना माहात्म्य है, तीर्थस्थान पहुँचने से इतने आनन्द की प्राप्ति होती है। इसी तरह मनुष्य का जीवन हुआ करता है। मनुष्य के जीवन का आरम्भ क्योंकि जन्म से होता है इसीलिए वह अन्त में जन्मांतर में पहुँचकर अमृतमय हो जाता है। तमाम नदियों का अन्त चूँकि समुद्र में होता है इसलिए समुद्र ही क्या सब कुछ है और नदी कुछ भी नहीं ?
लिखने बैठा हूँ तो सोचता हूँ, उपन्यास की शुरुआत कहाँ से करूँ, किसको केन्द्र मान कर लिखूँ ? किसके बारे में कहानी शुरू करूँ ? सुनीति मित्र को लेकर ? वह क्या इस कहानी की नायिका है ? या लीला हंसराज को लेकर शुरू करूँ ? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अपने मास्टर साहब कालीपद को लेकर शुरू करूँ तो भी काम चल सकता है। वही कालीपद मास्टर साहब जो पहले खादी पहना करते थे, जो ब्रह्मचर्य पालन को जीवन का धर्म मान कर चलते थे। या अगर दुर्गा देवी को लेकर शुरू करूँ तो भी बुरा नहीं होगा। वह सब न कर अगर पार्क स्ट्रीक के ब्लैक प्रिंस को लेकर शुरू करूँ तो भी कोई हर्ज नहीं।
शुरू करने का एक और उपाय है। वह है सोने का एक हार।
मामूली सोने के जिस हार को उपलक्ष्य बनाने के कारण इतनी छोटी संख्या का हिसाब जो गलत हो गया, उसी को लेकर शुरूआत की जा सकती है। दिखा सकता हूँ कि डेढ़ सौ रुपये का एक मामूली हार किस तरह इस उपन्यास का एक असाधारण उपादन हो गया।
कर तो सकता हूँ सब कुछ, मगर असली बात है। आज का युग गति और व्यस्तता का युग है। हम इसी व्यस्तता-युग के अभिशप्त प्राणी हैं। हम आज आराम या अवकाश-ग्रहण की बात नहीं सोच सकते। प्रत्येक आदमी के जीवन में एक समय आता है जब उसे अवकाश ग्रहण करना पड़ता है, कर्म क्षेत्र से दूर हटकर खड़ा होना पड़ता है। वहीं सुखद और स्वास्थ्यकारी होता है। मगर हम ऐसा नहीं कर पाते। हम दुनिया को छोड़कर इतनी आसानी से नहीं जाना चाहते, किसी के लिए तिल भर भी जगह नहीं छोड़ना चाहते। हम चलना जानते हैं, रुकना नहीं।
लेकिन जब शुरू करना ही है तो इतनी भूमिका की जरूरत ही क्या ? लेखन को ही जब धर्म के रूप में स्वीकार कर लिया है तो चिन्ता फिक्र की दुहाई दूँ तो आप मानने को तैयार नहीं होइएगा। फिर भी मन ही मन बड़ा ही क्लेश होता है। सोचता हूँ, मैं यह क्या कर रहा हूँ। आदमी को पहचानने और उसकी पहचान कराने की जिम्मेदारी जान-बूझकर अपने माथे पर क्यों ले रहा हूँ !
यही वजह है कि जब कोई हिसाब नहीं मिलता है तो कभी-कभी जी में होता है अपने जीवन को ही धिक्कारूँ ! बार-बार कहने को मन होता है कि मैंने यह क्या किया ? इतने दिनों के बाद मैंने किनती बड़ी ग़लती की। मुझमें जो इतना अहंकार था कि मैं आदमी को पहचानता हूँ, उस अहंकार को क्या इस तरह चूर होना चाहिए था।
इसीलिए तो सोचता हूँ, बावजूद इतने-इतने आदमियों को देखने, इतने आदमियों से मिलने और इतनी मोटी -मोटी किताबें लिखने के, मैं कुछ भी न जान सका, किसी को भी पहचान न सका। यह चिरपरिचित दुनिया किसी-किसी दिन मुझे अजनबी जैसी लगती है। चारों ओर का समाज अचानक एक अजनबी चेहरा पहन कर मेरे सामने खड़ा हो जाता है। देखकर मैं स्तंभित हो जाता हूँ, चौंक पड़ता हूँ, अपने आपको ही नये सिरे से पहचानने की कोशिश करने लगता हूँ।
सुनीति की ही बात लें। सुनीति मित्र के साथ ही जिस तरह की घटना हुई, उसी पर सोचकर देख लें। सुनीति को मैं क्या थोड़े दिनों से जानता था ?
जब सुनीति हमारे घर पर पहले-पहल आयी थी, उस समय भैया की लड़की ज्यादा से ज्यादा पाँच या छह साल की होगी। भैया की वह पहली सन्तान है, अतः बड़ी ही लाडली थी। सभी उसे बेहद प्यार करते थे। एक बात उसके मुँह से निकल जाये तो सभी कहते, ‘‘आह कितनी अक्लमन्द है।’
इतनी कम उम्र में जब इतनी अक्लमन्द है तो ब़ड़ी होने पर कितनी अक्लमन्द होगी, यह सोचकर सभी रोमांचित हो उठते थे।
वही लड़की जब चार साल की हो गयी तो भैया ने उसे नर्सरी स्कूल में दाखिल करा दिया।
हमारे ज़माने में चाहे जो कुछ हुआ हो, मगर इस युग में सभी अपनी-अपनी लड़की को इन्दिरा गाँधी बनाना चाहते हैं। लड़कियों को सजा-धजाकर उनकी माताएँ उन्हें यूनिफार्म पहनाती हैं और उसके बाद फ्लास्क हाथ में लिए गली पार करती हुई स्कूल की बस के लिए इन्तज़ार करती रहती हैं। जिनकी माताएँ गृहस्थी के कामों के कारण वक्त नहीं निकाल पाती हैं, उनके बाप, चाचा या भाइयों को यह जिम्मेदारी ओढ़नी पड़ती है।
यह नया रिवाज चल पड़ा है।
पहले यह सब रिवाज नहीं था। आज जो बच्चे जितने ही बड़े स्कूल में पढ़ते हैं, जितनी ही कीमती बस पर सवार होकर स्कूल जाते हैं, उनके माँ-बाप की उतनी ही इज्ज्त होती है। जिन बच्चों के स्कूल की फीस ज्यादा है, बस में जिन्हें ज्यादा किराया चुकाना पड़ता है, वे समाज और मुहल्ले में ईर्ष्या की दृष्टि से देखे जाते हैं। बच्चों की स्कूल बस पर जो नाम लिखा रहता है, असली कीमत उसी की है। उस नाम को देखते ही हम अन्दाज लगा लेंगे कि तुम्हारे पिता का कितना सम्मान है, उन्हें दफ्तर में कितनी तनख्वाह मिलती है, तुम्हारा खान-पान किस तरह का है।
सचमुच पहले यह सब नहीं था। वीथि के कारण भैया को भी इस समस्या के सामने खड़ा होना पड़ा। भैया अच्छी नौकरी पर हैं, महीनें में उन्हें दो हजार रुपये तनख्वाह मिलती है, अतः उनकी लड़की का मुहल्ले के महाकाली विद्यालय में दाखिला नहीं कराया जा सकता है। महाकाली विद्यालय की माहवार फीस मात्र दस रुपये है। इससे भैया की इज्जत पर पानी फिर जायेगा, साथ-साथ हमारे खानदान की भी इज्जत धूल में मिल जायेगी।
दरअसल इस युग में इस मिथ्या सम्मान को लेकर ही हम जीवन जी रहे हैं। धर्म बच रहा है या नहीं, इसे देखने की जरूरत हम महसूस नहीं करते, सत्य जीवित है या नहीं, इस पर हम विचार नहीं करते। बाहरी आदमी के सामने हमारा मिथ्या सम्मान बना रहे तो हम जी जायें।
मगर मैं इतनी बातें क्यों कह रहा हूँ और कौन इतना सुनेगा ? कहानी कहना मेरा काम है, इसीलिए मुझे कहानी ही लिखनी चाहिए। मैं हमेशा इस बात पर विश्वास करता आया हूँ कि आदमी अभी जिस तरह से रह रहा हूँ, उस तरह नहीं रहेगा, उसका समाज भी इस तरह नहीं रहेगा। तब अच्छाई-बुराई का अर्थ बदल जायेगा, पाप-पुण्य के अर्थ में परिवर्तन आयेगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि प्राचीन मूल्य लौट आयें। आदमी फिर से धर्म, सत्य और ईश्वर की महिमा को मर्यादा प्रदान करने लगे।
तब हो सकता है, सुनीति मित्र की कहानी आदमी को सचमुच ही अच्छी लगने लगे। हो सकता है सही तौर पर तब सुनीति मित्र का मूल्यांकन हो। और इसी भरोसे आज मैं सुनीति मित्र की कहानी लिखने बैठा हूँ।
शुरू में सुनीति मित्र से मेरी कोई जान-पहचान नहीं थी। किसी खास घटना या स्थिति के कारण ही आदमी से आदमी की जान-पहचान होती है। तब हाँ, रक्त या आत्मीयता का सम्बन्ध हो तो बात ही अलग है।
मगर दुनिया-भर के आदमी से खून के रिश्ते में बँधना मुमकिन नहीं है। दुनिया में इतने-इतने आदमी हैं, विविध कारणों से एक दूसरे के सम्पर्क में आते हैं। लेकिन ऐसा होने से ही क्या सभी एक-दूसरे को जानने-पहचानने लगते हैं ? घनिष्ठता के सूत्र में बँध जाते हैं ?
भैया की लड़की के लिए एक मास्टरनी की जरूरत पड़ी।
भैया को हमेशा काम में व्यस्त रहना पड़ता है। उनके पास वक्त नहीं है कि लड़की के लिए मास्टरनी की तलाश करें। दफ्तर जाना पड़ता है, दफ्तर की जिम्मेदारी निभानी पड़ती है। दफ्तर के काम से कलकत्ते से बाहर जाना पड़ता है। वीथि के लिए जो कुछ भी करना है, सब कुछ भाभी जी को ही करना पड़ता है।
और मैं ?
मैं ठहरा आलसी आदमी। हर तरह का काम रहने पर भी मैं निकम्मा हूँ। अतः मुझ पर ही इस काम की जिम्मेदारी लादी गयी-यानी वीथि के लिए मास्टरनी की तलाश करने की जिम्मेदारी।
तीन नंबर गवाह नामक एक उपन्यास में भी मैं लिख चुका हूँ और अब भी यह स्वीकार करता हूँ कि मैं तब ऐसी एक नौकरी कर रहा था जिसमें मुझे फुर्सत और काम दोनों अधिक से अधिक तादात में मिलते थे।
सभ्य भाषा में कहूँ तो कहना पड़ेगा कि तब मैं गुप्तचर का काम करता था।
‘गुप्तचर’ शब्द सुनने में खराब लगता है। मगर चाहे खराब ही क्यों न लगे, मेरा असली काम वही था।
मैं ठहरा पुलिस का आदमी। पुलिस का आदमी रहने पर भी मुझे रोज-रोज दफ्तर नहीं जाना पड़ता था। मुझे स्वाधीनतापूर्वक समाज के हर तबके के आदमी से हेल-मेल बढ़ाकर अनैतिकता की छिपी हुई खबरों का पता लगाना पड़ता था और ठीक समय पर इसकी लिखित सूचना अपने अफसर को देनी पड़ती थी ! उसके बाद एक दिन जाल बिछाकर मुजरिम को पकड़ना पड़ता था।
कहा जा सकता है कि तब मैं सरकार के अपराध निरोध विभाग का एक वरिष्ठ अफ़सर था।
इसके बारे में यहाँ ज्यादा लिखना जरूरी नहीं है। इतना कहना ही काफी होगा कि इसी काम के सिलसिले में सुनीति मित्र से मेरी जान-पहचान हुई।
तीर्थ के देवता तीर्थ-पथ के अन्त में वास करते हैं। तीर्थ-पथ को तय किये बिना तीर्थ के देवता के दर्शन नहीं होते। तीर्थ यात्रा में चूँकि यातना झेलनी पड़ती है, इसीलिए तीर्थ के देवता का इतना माहात्म्य है, तीर्थस्थान पहुँचने से इतने आनन्द की प्राप्ति होती है। इसी तरह मनुष्य का जीवन हुआ करता है। मनुष्य के जीवन का आरम्भ क्योंकि जन्म से होता है इसीलिए वह अन्त में जन्मांतर में पहुँचकर अमृतमय हो जाता है। तमाम नदियों का अन्त चूँकि समुद्र में होता है इसलिए समुद्र ही क्या सब कुछ है और नदी कुछ भी नहीं ?
लिखने बैठा हूँ तो सोचता हूँ, उपन्यास की शुरुआत कहाँ से करूँ, किसको केन्द्र मान कर लिखूँ ? किसके बारे में कहानी शुरू करूँ ? सुनीति मित्र को लेकर ? वह क्या इस कहानी की नायिका है ? या लीला हंसराज को लेकर शुरू करूँ ? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अपने मास्टर साहब कालीपद को लेकर शुरू करूँ तो भी काम चल सकता है। वही कालीपद मास्टर साहब जो पहले खादी पहना करते थे, जो ब्रह्मचर्य पालन को जीवन का धर्म मान कर चलते थे। या अगर दुर्गा देवी को लेकर शुरू करूँ तो भी बुरा नहीं होगा। वह सब न कर अगर पार्क स्ट्रीक के ब्लैक प्रिंस को लेकर शुरू करूँ तो भी कोई हर्ज नहीं।
शुरू करने का एक और उपाय है। वह है सोने का एक हार।
मामूली सोने के जिस हार को उपलक्ष्य बनाने के कारण इतनी छोटी संख्या का हिसाब जो गलत हो गया, उसी को लेकर शुरूआत की जा सकती है। दिखा सकता हूँ कि डेढ़ सौ रुपये का एक मामूली हार किस तरह इस उपन्यास का एक असाधारण उपादन हो गया।
कर तो सकता हूँ सब कुछ, मगर असली बात है। आज का युग गति और व्यस्तता का युग है। हम इसी व्यस्तता-युग के अभिशप्त प्राणी हैं। हम आज आराम या अवकाश-ग्रहण की बात नहीं सोच सकते। प्रत्येक आदमी के जीवन में एक समय आता है जब उसे अवकाश ग्रहण करना पड़ता है, कर्म क्षेत्र से दूर हटकर खड़ा होना पड़ता है। वहीं सुखद और स्वास्थ्यकारी होता है। मगर हम ऐसा नहीं कर पाते। हम दुनिया को छोड़कर इतनी आसानी से नहीं जाना चाहते, किसी के लिए तिल भर भी जगह नहीं छोड़ना चाहते। हम चलना जानते हैं, रुकना नहीं।
लेकिन जब शुरू करना ही है तो इतनी भूमिका की जरूरत ही क्या ? लेखन को ही जब धर्म के रूप में स्वीकार कर लिया है तो चिन्ता फिक्र की दुहाई दूँ तो आप मानने को तैयार नहीं होइएगा। फिर भी मन ही मन बड़ा ही क्लेश होता है। सोचता हूँ, मैं यह क्या कर रहा हूँ। आदमी को पहचानने और उसकी पहचान कराने की जिम्मेदारी जान-बूझकर अपने माथे पर क्यों ले रहा हूँ !
यही वजह है कि जब कोई हिसाब नहीं मिलता है तो कभी-कभी जी में होता है अपने जीवन को ही धिक्कारूँ ! बार-बार कहने को मन होता है कि मैंने यह क्या किया ? इतने दिनों के बाद मैंने किनती बड़ी ग़लती की। मुझमें जो इतना अहंकार था कि मैं आदमी को पहचानता हूँ, उस अहंकार को क्या इस तरह चूर होना चाहिए था।
इसीलिए तो सोचता हूँ, बावजूद इतने-इतने आदमियों को देखने, इतने आदमियों से मिलने और इतनी मोटी -मोटी किताबें लिखने के, मैं कुछ भी न जान सका, किसी को भी पहचान न सका। यह चिरपरिचित दुनिया किसी-किसी दिन मुझे अजनबी जैसी लगती है। चारों ओर का समाज अचानक एक अजनबी चेहरा पहन कर मेरे सामने खड़ा हो जाता है। देखकर मैं स्तंभित हो जाता हूँ, चौंक पड़ता हूँ, अपने आपको ही नये सिरे से पहचानने की कोशिश करने लगता हूँ।
सुनीति की ही बात लें। सुनीति मित्र के साथ ही जिस तरह की घटना हुई, उसी पर सोचकर देख लें। सुनीति को मैं क्या थोड़े दिनों से जानता था ?
जब सुनीति हमारे घर पर पहले-पहल आयी थी, उस समय भैया की लड़की ज्यादा से ज्यादा पाँच या छह साल की होगी। भैया की वह पहली सन्तान है, अतः बड़ी ही लाडली थी। सभी उसे बेहद प्यार करते थे। एक बात उसके मुँह से निकल जाये तो सभी कहते, ‘‘आह कितनी अक्लमन्द है।’
इतनी कम उम्र में जब इतनी अक्लमन्द है तो ब़ड़ी होने पर कितनी अक्लमन्द होगी, यह सोचकर सभी रोमांचित हो उठते थे।
वही लड़की जब चार साल की हो गयी तो भैया ने उसे नर्सरी स्कूल में दाखिल करा दिया।
हमारे ज़माने में चाहे जो कुछ हुआ हो, मगर इस युग में सभी अपनी-अपनी लड़की को इन्दिरा गाँधी बनाना चाहते हैं। लड़कियों को सजा-धजाकर उनकी माताएँ उन्हें यूनिफार्म पहनाती हैं और उसके बाद फ्लास्क हाथ में लिए गली पार करती हुई स्कूल की बस के लिए इन्तज़ार करती रहती हैं। जिनकी माताएँ गृहस्थी के कामों के कारण वक्त नहीं निकाल पाती हैं, उनके बाप, चाचा या भाइयों को यह जिम्मेदारी ओढ़नी पड़ती है।
यह नया रिवाज चल पड़ा है।
पहले यह सब रिवाज नहीं था। आज जो बच्चे जितने ही बड़े स्कूल में पढ़ते हैं, जितनी ही कीमती बस पर सवार होकर स्कूल जाते हैं, उनके माँ-बाप की उतनी ही इज्ज्त होती है। जिन बच्चों के स्कूल की फीस ज्यादा है, बस में जिन्हें ज्यादा किराया चुकाना पड़ता है, वे समाज और मुहल्ले में ईर्ष्या की दृष्टि से देखे जाते हैं। बच्चों की स्कूल बस पर जो नाम लिखा रहता है, असली कीमत उसी की है। उस नाम को देखते ही हम अन्दाज लगा लेंगे कि तुम्हारे पिता का कितना सम्मान है, उन्हें दफ्तर में कितनी तनख्वाह मिलती है, तुम्हारा खान-पान किस तरह का है।
सचमुच पहले यह सब नहीं था। वीथि के कारण भैया को भी इस समस्या के सामने खड़ा होना पड़ा। भैया अच्छी नौकरी पर हैं, महीनें में उन्हें दो हजार रुपये तनख्वाह मिलती है, अतः उनकी लड़की का मुहल्ले के महाकाली विद्यालय में दाखिला नहीं कराया जा सकता है। महाकाली विद्यालय की माहवार फीस मात्र दस रुपये है। इससे भैया की इज्जत पर पानी फिर जायेगा, साथ-साथ हमारे खानदान की भी इज्जत धूल में मिल जायेगी।
दरअसल इस युग में इस मिथ्या सम्मान को लेकर ही हम जीवन जी रहे हैं। धर्म बच रहा है या नहीं, इसे देखने की जरूरत हम महसूस नहीं करते, सत्य जीवित है या नहीं, इस पर हम विचार नहीं करते। बाहरी आदमी के सामने हमारा मिथ्या सम्मान बना रहे तो हम जी जायें।
मगर मैं इतनी बातें क्यों कह रहा हूँ और कौन इतना सुनेगा ? कहानी कहना मेरा काम है, इसीलिए मुझे कहानी ही लिखनी चाहिए। मैं हमेशा इस बात पर विश्वास करता आया हूँ कि आदमी अभी जिस तरह से रह रहा हूँ, उस तरह नहीं रहेगा, उसका समाज भी इस तरह नहीं रहेगा। तब अच्छाई-बुराई का अर्थ बदल जायेगा, पाप-पुण्य के अर्थ में परिवर्तन आयेगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि प्राचीन मूल्य लौट आयें। आदमी फिर से धर्म, सत्य और ईश्वर की महिमा को मर्यादा प्रदान करने लगे।
तब हो सकता है, सुनीति मित्र की कहानी आदमी को सचमुच ही अच्छी लगने लगे। हो सकता है सही तौर पर तब सुनीति मित्र का मूल्यांकन हो। और इसी भरोसे आज मैं सुनीति मित्र की कहानी लिखने बैठा हूँ।
शुरू में सुनीति मित्र से मेरी कोई जान-पहचान नहीं थी। किसी खास घटना या स्थिति के कारण ही आदमी से आदमी की जान-पहचान होती है। तब हाँ, रक्त या आत्मीयता का सम्बन्ध हो तो बात ही अलग है।
मगर दुनिया-भर के आदमी से खून के रिश्ते में बँधना मुमकिन नहीं है। दुनिया में इतने-इतने आदमी हैं, विविध कारणों से एक दूसरे के सम्पर्क में आते हैं। लेकिन ऐसा होने से ही क्या सभी एक-दूसरे को जानने-पहचानने लगते हैं ? घनिष्ठता के सूत्र में बँध जाते हैं ?
भैया की लड़की के लिए एक मास्टरनी की जरूरत पड़ी।
भैया को हमेशा काम में व्यस्त रहना पड़ता है। उनके पास वक्त नहीं है कि लड़की के लिए मास्टरनी की तलाश करें। दफ्तर जाना पड़ता है, दफ्तर की जिम्मेदारी निभानी पड़ती है। दफ्तर के काम से कलकत्ते से बाहर जाना पड़ता है। वीथि के लिए जो कुछ भी करना है, सब कुछ भाभी जी को ही करना पड़ता है।
और मैं ?
मैं ठहरा आलसी आदमी। हर तरह का काम रहने पर भी मैं निकम्मा हूँ। अतः मुझ पर ही इस काम की जिम्मेदारी लादी गयी-यानी वीथि के लिए मास्टरनी की तलाश करने की जिम्मेदारी।
तीन नंबर गवाह नामक एक उपन्यास में भी मैं लिख चुका हूँ और अब भी यह स्वीकार करता हूँ कि मैं तब ऐसी एक नौकरी कर रहा था जिसमें मुझे फुर्सत और काम दोनों अधिक से अधिक तादात में मिलते थे।
सभ्य भाषा में कहूँ तो कहना पड़ेगा कि तब मैं गुप्तचर का काम करता था।
‘गुप्तचर’ शब्द सुनने में खराब लगता है। मगर चाहे खराब ही क्यों न लगे, मेरा असली काम वही था।
मैं ठहरा पुलिस का आदमी। पुलिस का आदमी रहने पर भी मुझे रोज-रोज दफ्तर नहीं जाना पड़ता था। मुझे स्वाधीनतापूर्वक समाज के हर तबके के आदमी से हेल-मेल बढ़ाकर अनैतिकता की छिपी हुई खबरों का पता लगाना पड़ता था और ठीक समय पर इसकी लिखित सूचना अपने अफसर को देनी पड़ती थी ! उसके बाद एक दिन जाल बिछाकर मुजरिम को पकड़ना पड़ता था।
कहा जा सकता है कि तब मैं सरकार के अपराध निरोध विभाग का एक वरिष्ठ अफ़सर था।
इसके बारे में यहाँ ज्यादा लिखना जरूरी नहीं है। इतना कहना ही काफी होगा कि इसी काम के सिलसिले में सुनीति मित्र से मेरी जान-पहचान हुई।
|
|||||
अन्य पुस्तकें
लोगों की राय
No reviews for this book