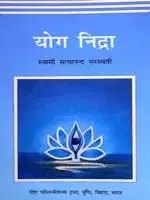|
योग >> योग निद्रा योग निद्रास्वामी सत्यानन्द सरस्वती
|
545 पाठक हैं |
||||||
योग निद्रा मनस और शरीर को अत्यंत अल्प समय में विक्षाम देने के लिए अभूतपूर्व प्रक्रिया है।
अन्य अभ्यास
दिन-प्रतिदिन की घटनाओं का पुनरावलोकन स्मृति बढ़ाने तथा अपनी दैनिक क्रियाओं एवं प्रतिक्रियाओं के अवलोकन के लिए बहुत उपयोगी है। इस अभ्यास को बाद में हफ्ते के एक दिन की स्मृति, फिर महीने के एक दिन की, फिर वर्ष के एक दिन की स्मृति में बदल दीजिये अथवा बचपन की किसी घटना की स्मृति में बदल दीजिये; स्मृति का दायरा और भी बढ़ जायेगा। किसी घटना को स्मृति में दुहराना तथा उसके बाद मस्तिष्क का बारीकी से संपूर्ण अवलोकन करना अत्यंत आवश्यक है। इस क्रिया को बार-बार दोहराने से आपको आश्चर्य होगा कि मन सब चीजों का कितना सुन्दर चित्रांकन करता है। पूर्व अभ्यास की एक प्रक्रिया है - किसी उत्तेजक स्थिति, घटना या पीड़ा को याद कर उसको साक्षी भाव से देखना। यदि साक्षी भाव बनाये रखा जाये तो यह कुसंस्कार को उभारने की एक सशक्त प्रक्रिया है। यदि साक्षी भाव को और भी सशक्त बना लिया जाये तो इसका प्रभाव सकारात्मक रूप से निर्माण की क्रिया में संलग्न हो जाता है। यह भाव व्यक्ति को पीड़ा-मुक्त भी करता है और भविष्य में होने वाली उसी प्रकार की अन्य घटनाओं के प्रभाव से भी बचाता है। साँसों को भी दृश्य देखने का जरिया बनाया जा सकता है। जैसे, हल्के से साँस अंदर लेना और समस्त अशुद्धता को साँस द्वारा बाहर निकाल देना। दर्द और बेचैनी की अनुभूति साँसों को उस भाग में ले जाकर पुनः बाहर निकालने से कम की जा सकती है। प्राण विद्या का विज्ञान भी इस तरह के दर्द और बेचैनी हो हटाने में सार्थक हो सकता है। जैसे, दर्द के स्थान को पहले सुनहरी किरणों में स्नान करते हुए देखें, फिर गर्म किरणों में। इस तरह से कल्पना में देखने के कार्य द्वारा कोशिकाओं के पुनर्निर्माण में सुविधा होती है तथा शरीर से रोग दूर होकर स्वास्थ्य की उपलब्धि होती है।
सहानुभूति एवं सुरक्षा की भावना का विकास करना तथा दूसरों के हृदय में घुस कर उनकी भावना को जानने का प्रयास करना भी महत्त्वपूर्ण है। आप अपने को एक गुब्बारे के अन्दर आराम से बैठा हुआ देखें। अब अपने गुब्बारे को मन ही मन फैलाते जायें और उसमें अनेक लोगों को अपने पास बैठे हुए देखें। अब इन सभी को अपने-अपने कमरे में देखें। अगर इस दृश्य में कठिनाई आती है, बेचैनी होती है तो अपने को आरामदायक स्थान पर ले जाइये और पुनः अपनी भावनाओं को विस्तृत करना प्रारम्भ कीजिए। इस विस्तार में सभी लोग आ सकते हैं, शहर के, मुहल्ले के, नगर के, दुनिया के, ब्रह्माण्ड के सभी दृश्य इसमें कल्पित किये जा सकते हैं।
दृश्यों को देखने की अन्य संभावनाएँ भी हैं, जिनका अभ्यास थोड़ी गहराई में जाने के बाद किया जा सकता है। मनुष्य में निर्माण की अपार शक्ति है, इसका उपयोग योग निद्रा के अभ्यास में कल्पना में देखने के कार्य द्वारा अपने व्यक्तित्व के निर्माण में किया जा सकता है।
शरीर व मन से परे
योग निद्रा का प्रारम्भिक उद्देश्य तो यही है कि शरीर व मन को विश्राम प्राप्त हो, लेकिन अभ्यास के अन्तिम चरण में व्यक्ति शरीर व मन से भी सम्बन्ध-विच्छेद करने का अभ्यास करता है। तनाव, परेशानियाँ, दबाव आदि तभी असर करते हैं जब व्यक्ति शरीर व मन के साथ जुड़ा रहता है। गहरी निद्रा के समय यह सम्बन्ध अपने आप टूट जाता है, यहाँ तक कि व्यक्ति अपना नाम, शरीर व स्थान तक भूल जाता है। उसी प्रकार योग निद्रा के अभ्यास के समय गहरे विश्राम के क्षण में साधक को अपने व्यक्तित्व को शरीर व मन से पृथक् कर लेना चाहिये।
पंचकोष
आधुनिक मनोविज्ञान मन के तीन स्तर मानता है - चेतन, अवचेतन एवं अचेतन। वेदांत और योग दर्शन में इन्हें मानव व्यक्तित्व के स्थूल, सूक्ष्म एवं कारण आयामों के रूप में जाना जाता है। व्यक्तित्व के इन तीन आयामों को पुनर्विभाजित कर इन्हें पाँच कोषों में विभक्त किया गया है। यही पाँच कोष मनुष्य के शरीर व मन की सभी अवस्थाओं का संचालन करते रहते हैं, चाहे वह स्थूल आयाम से सम्बन्धित हों अथवा सबसे सूक्ष्म आयाम से।
इन पाँच कोषों को सहज ही मनोवैज्ञानिक आयामों, शारीरिक अवस्थाओं तथा सजगता के विभिन्न स्तरों से जोड़ा जा सकता है, जैसा कि निम्नांकित रेखाचित्र में दर्शाया गया है।
पंचकोष
आनन्दमय कोष
अचेतन मन
समांगी सजगता;
अचेतन
गहरी निद्रा: ध्यानात्मक सजगता
विज्ञानमय कोष सूक्ष्म एवं कारण आयामों की सजगता
मनोवैज्ञानिक आयाम
अवचेतन मन
स्वप्निल सजगता
शारीरिक अवस्था
मनोमय कोष मानसिक एवं भावनात्मक प्रक्रियाओं की सजगता
प्राणमय कोष शारीरिक क्रियाओं, जैसे, पाचन के प्रति सजगता
चेतन मन
जागरूक सजगता
अन्नमय कोष भौतिक शरीर की चेतना
इन पाँच कोषों को योग शास्त्रों में निम्नलिखित प्रकार से पारिभाषित किया गया है -
अन्नमय कोष - मनुष्य का स्थूल शरीर जो रक्त, हड्डी, चर्बी, त्वचा आदि से बना हुआ है, ज्ञानेन्द्रियों द्वारा संतुलित किया जाता है। यह चेतना का स्थूल स्तर है।
प्राणमय कोष - यह मानव संरचना में अन्तर्निहित ऊर्जा जालक है, जिसमें प्राणशक्ति प्रवाहित होती है। इस स्तर पर शारीरिक क्रियाओं, जैसे, पाचन तथा रक्त-संचरण की सजगता रहती है।
मनोमय कोष वह स्थान है जहाँ से चेतना अवचेतन में प्रवेश करती है, किन्तु मन की ऊपरी सतह तक ही रहती है।
विज्ञानमय कोष - यह स्थान मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास से सम्बन्ध रखता है, जहाँ व्यक्ति साधारण मनुष्यों से परे आत्म सम्बन्धी ज्ञान प्राप्त करता है। शरीर के इस भाग का स्वप्न से सम्बन्ध रहता है, क्योंकि स्वप्न शरीर के विभिन्न अनुभवों अथवा विभिन्न प्रकार के आत्म सम्बन्धी ज्ञान पर आधारित रहते हैं।
आनन्दमय कोष - यह चिदानन्द की अवस्था है जहाँ व्यक्ति को दु:ख व सुख का अनुभव नहीं होता। इस अवस्था का वर्णन करना कठिन है, क्योंकि यह अनुभव से सम्बन्धित है, पर यह मानव के लिए बहुत उपयोगी है। आनन्द का अर्थ बहुधा सुख, खुशी अथवा शारीरिक आनन्द से लिया जाता है। आनन्दमय कोष का अर्थ है शरीर व मन की वह स्थिति जहाँ दु:ख व सुख की भावना ही नहीं होती। इस समय सभी अवस्थायें एक समान लगती हैं। मन की इस अवस्था को सुख-दुःख से परे चिदानन्द की अवस्था कहा गया है। इसको और अच्छी तरह समझाने के लिए एक उदाहरण और प्रस्तुत है। व्यक्ति यदि दु:ख व सुख का अनुभव करता है तो मानसिक उतार-चढ़ाव की स्थिति से अवश्य गुजरना पड़ता है। इसका अर्थ है कि दर्द भी एक अनुभूति है। आनन्द, की अवस्था में मन की सूक्ष्मतम अवस्था तक वह उद्वेलित नहीं होता, वह अनुभव के दायरे से बाहर हो जाता है।
योग निद्रा का नियमित अभ्यास मनुष्य को आनन्दमय कोष की अवस्था तक पहुँचाता है, जहाँ केवल मूल अवचेतन का ही राज्य रहता है, अन्य कुछ नहीं। यह योग निद्रा की गहराई का वह स्तर है जहाँ चिदानन्द के सिवा और कुछ नहीं है। इस एक समान अवस्था को 'योग तारावली' में आदि शंकराचार्य ने इस प्रकार वर्णित किया है -
"जब मन मायारहित हो जाता है, जब अहंकार स्थिर हो जाता है, जब इन्द्रियाँ अपना कार्य बंद कर देती हैं, जब इन्द्रियों और मन के सारे सम्बन्ध समाप्त हो जाते हैं, उस समय चिदानन्द की प्राप्ति होती है।"
|
|||||
अन्य पुस्तकें
लोगों की राय
No reviews for this book