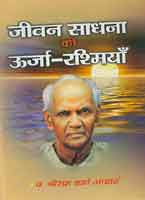|
आचार्य श्रीराम शर्मा >> मानवीय मस्तिष्क विलक्षण कंप्यूटर मानवीय मस्तिष्क विलक्षण कंप्यूटरश्रीराम शर्मा आचार्य
|
17 पाठक हैं |
||||||
शरीर से भी विलक्षण मस्तिष्क...
रोग शारीरिक नहीं, मानसिक
कोलंबिया विश्वविद्यालय के जीव-विज्ञानी डॉ० एच० सिक्स ने अपने अनुसंधानों से
यह निष्कर्ष निकाला है कि यदि शरीर को रासायनिक दोषों से और जेट व्याधियों से
मुक्त रखा जा सके तो मनुष्य आसानी से आठ सौ वर्ष जी सकता है। वे कहते
हैं—अधिक सक्रियता, दौड़-धूप, उत्तेजना और गर्मी-शरीर को संतप्त करके उसकी
जीवनी शक्ति के भंडार को बेतरह खर्च करती है। यदि भीतरी अवयवों पर अतिरिक्त
दबाव न पड़े और उन्हें स्वाभाविकसरल रीति से काम करने दिया जाए तो वे इतने
समर्थ रह सकते हैं कि क्षतिपूर्ति का काम आसानी से चलता रहे। नशेबाजी से लेकर
वासना, क्रोध, चिंता आदि के आवेशों तक कितने ही ऐसे कारण हैं, जो जितने
अनावश्यक उससे ज्यादा हानिकारक है। शांत, सरल, संतुष्ट और प्रसन्न जीवन जीने
से निरर्थक उत्तेजना से बचा जा सकता है और जीवनी-शक्ति के क्षरण को बचाकर
लंबा जीवन जिया जा सकता है।
अंतःचेतना का जो स्तर होता है उसी के अनुरूप मन, मस्तिष्क, नाड़ी संस्थान एवं
अवयवों के क्रियाकलाप का ढाँचा विनिर्मित होता है और ढर्रा चलता है। आंतरिक
उद्वेग की ऊष्मा सारे ढाँचे को प्रभावित करती है और इतना ताप पैदा कर देती है
जिससे जीवन तत्त्व भाड़ में भुनने वाले चने की तरह अपनी कोमलता और सरलता से
वंचित होते रहें। मनोविकार एक प्रकार की ऐसी आग है जो भीतर ही भीतर जलते रहते
हैं, जिससे स्वास्थ्य के लिए उत्तरदायी तत्त्व स्वतः ही विनष्ट होते चले
जायें। इंद्रिय भोगों की ललक और संग्रह स्वामित्व की ललक इन्हें वासना और
तृष्णा कहा जाता है। यह न बुझने वाली अग्नि-शिखाएँ जिनके भीतर जल रही होंगी
वे अपनी शांति और समस्वरता निरंतर खोते चले जायेंगे।
जिन्हें चिंता, भय, क्रोध, असंतोष सवार रहते हैं, जो निराश और अवसादग्रस्त
बैठे रहते हैं। ईर्ष्या, द्वेष, प्रतिशोध, कपट और मत्सर की दुष्प्रवृत्तियाँ
जिन पर सवार रहती हैं उनका अंतकरण निरंतर उद्विग्न रहता है। मन में तनिक भी
संतोष-समाधान नहीं होता। यह उद्विग्नता सारी अंतःस्थिति में ज्वार-भाटा उठाती
और उसे बेतरह मथती रहती हैं, तो इस विषम स्थिति में ग्रस्त किसी भी व्यक्ति
का स्वास्थ्य संतुलित नहीं रह सकता।
अनावश्यक ताप पैदा करने वाले मनोविकार-विक्षोभ एवं उद्देश्यों से बचने और
शांत-संतुलित, संतुष्ट और हँसी-खुशी का नियमित जीवन जीने का प्रयत्न करना
चाहिए। आहार सीमित और समय पर हो। सादा और अनुत्तेजक साथ ही भूख से कम मात्रा
में। ऐसी सावधानी बरतने से पेट में वह ताप उत्पन्न नहीं होता जिसके कारण तीन
चौथाई मनुष्यों को अपनी जीवनी शक्ति से बुरी तरह हाथ धोना पड़ता है।
अंतरंग में बढ़ी हुई उत्तेजना श्वास-प्रश्वास की गति को तीव्र करती है। क्रोध
की स्थिति में नाड़ी की, हृदय की गति बहुत बढ़ जाती है। काम सेवन के समय भी
यह चाल बहुत तेज हो जाती है। बढ़े हुए श्वास आम तौर से और की शक्ति का क्षरण
ही करते हैं। श्वास-प्रश्वास क्रिया के तीव्र और मंद रहने का भी आयुष्य से
बड़ा संबंध है। जो जीव हाँफते हैं, जिनके श्वास तेज चलते हैं, वे अधिक समय
नहीं जीते। उनकी आयु जल्दी ही समाप्त हो जाती है। इसके अतिरिक्त जिसकी साँस
मंद चलती है वे अधिक दिन जीवित रहते हैं।
"साइंस ऑफ माइंड" (मस्तिष्क विज्ञान) पत्रिका के जनवरी १६५६ अंक में डॉ०
बारबरा बेल का एक लेख छपा है-'मेन्टल मीनु (मस्तिष्क की भोजन तालिका)। इस लेख
में विद्वान् लेखक ने बताया है कि मनुष्य का शरीर स्वस्थ रहता है या अस्वस्थ
इसकी अधिकांश पहचान उसकी आहार व्यवस्था को देखकर लगाया जा सकता है, पर यह
आवश्यक नहीं कि शरीर से स्वस्थ व्यक्ति स्वस्थ और सुखी हो ही जब तक कि वह
मानसिक दृष्टि से भी स्वस्थ नहीं हो।
'मस्तिष्क स्वस्थ है या नहीं, यह जानने के लिए उसके विचार मानसिक विश्लेषण और
चिंतन की दिशा जानना आवश्यक है। विचार आत्मा का भोजन और पेय होते हैं।
मस्तिष्क की स्वस्थता और आत्मा की सुख-शांति के लिए सुव्यवस्थित और अच्छे
विचारों का मस्तिष्क में निरंतर उठते रहना आवश्यक है। प्राचीन काल के इतिहास
पर दृष्टि डालने से पता चलता है कि तब लोग अधिकांश इसी प्रयत्न में रहते थे
कि मन निम्न और अधोगामी बनने न पाए, इसके लिए कष्टसाध्य तीर्थ यात्राएं,
सत्संग और नित्य स्वाध्याय के कार्यक्रमों का-आध्यात्मिक धार्मिक और
वैराग्यपूर्ण चिंतन का स्रोत मस्तिष्क में निरंतर प्रवाहित बनाये रहते थे।
उसी का प्रतिफल था कि तब लोग स्वल्प साधनों में ही अपार सुख-शांति का
रसास्वादन करते थे।
विचार और भावनाओं की अदृश्य शक्ति का हमारे भारतीय शास्त्रों में गहन अध्ययन
हुआ है और यह निष्कर्ष निकाला गया है कि स्थूल रूप से मनुष्य का जैसा भी कुछ
जीवन है, उसकी भावनाओं का ही परिणाम है, भले ही उनका संबंध इस जीवन से न हो,
पर कोई भी कष्ट या दुःख, रोग-शोक या बीमारी हमारे पूर्वकृत कर्मों और उसके
पूर्व पैदा हुए मन के दुर्भावों का ही प्रतिफल होता है।
बुरे विचार रक्त में विकार उत्पन्न करते हैं और तभी रोगाणुओं की वृद्धि होती
है। यह विचार और भावनाओं के आवेश पर है कि उनका प्रभाव धीरे होता है या
शीघ्र, पर यह निश्चित है कि मन के भीतर अदृश्य रूप से जैसे अच्छे या बुरे
विचार उठते रहते हैं, उसी तरह के रक्त कण शरीर को सशक्त या कमजोर बनाते रहते
हैं, मनोभावों की तीव्रता की स्थिति में प्रभाव भी तीव्र होता है। यदि कोई
विचार हल्के उठते हैं तो उससे शरीर की स्थूल प्रकृति धीरे-धीरे प्रभावित होती
रहती है और उसका कोई दृश्य रूप कुछ समय के बाद देखने में आता है।
इंग्लैंड के डॉक्टर जॉन हंटर बड़े योग्य चिकित्साशास्त्री थे। उन्होंने
बड़े-बड़े रोगों को ठीक करने में सफलता पाई, किंतु उनकी धर्मपत्नी कुछ उग्र
स्वभाव की थीं, फलस्वरूप उन्हें भी प्रायः क्रोध आ जाया करता था और उसके कारण
वे स्वयं ही अस्वस्थ रहा करते थे।
एक बार डॉक्टरों को किसी सभा में भाग लेते समय किसी व्यक्ति से सहमति न होने
पर उन्हें जोर का गुस्सा आया, उससे शरीर का रक्त चाप एकाएक बढ़ गया। दिल का
दौरा पड़ा और हंटर की वहीं मृत्यु हो गई। डॉक्टरों ने खोज करके बताया कि उस
समय उनके रक्त का दबाव २३० था, जबकि सामान्य स्थिति में १३० ही रहता है। इस
बढ़े हुए दबाव के कारण शरीर की कोई भी शिरा फट सकती है। इसी प्रकार सामान्य
अवस्था में किसी की हृदयगति यदि ८० प्रति मिनट होती है तो क्रोध की अवस्था
में धड़कन बढ़कर १२० प्रति मिनट तक हो जाती है। रक्त का दबाव और धड़कन में
वृद्धि के साथ ही शरीर की दूसरी सब ग्रंथियाँ जीवन में काम आने वाले शारीरिक
रस निरर्थक मात्रा में पटक देती हैं। उससे शरीर की व्यवस्था और रचनात्मक
शक्ति कमजोर पड़ जाती है और मनुष्य रोगी या बीमार हो जाता है।
भारतीय योगियों ने इस तथ्य का अत्यंत सूक्ष्म अध्ययन किया है और में बताया
है-
चित्ते विधुरिते देहः संक्षोभमनुयात्यलम्।
संक्षोभात्साम्यमुत्सृज्य वहति प्राणवायवः
असमं बहति प्राणे नाड्यो यांति विसंस्थितिम्।
काश्चिन्नाड्यः प्रपूर्णत्वं याति काश्चिच्च रिक्तताम्।
कुजीर्णत्वमजीर्णत्वमतिजीर्णत्वमेव वा।
दोषायैव प्रयात्यन्नं प्राणसंचारदुष्क्रमात्।।
तथान्नानि नयत्यंतः प्राणवातः स्वमाश्रयम्।
यान्यन्नानि निरोधेन तिष्ठन्त्यंतः शरीरके।
तान्येव व्याधितां यांति परिणामस्वभावतः।।
एवमाधेर्भवेद्वयाधिस्तस्याभावाच्च नश्यति।।
अर्थात-चित्त में उत्पन्न हुए विकार से ही शरीर में दोष पैदा होते हैं। शरीर
में क्षोभ या दोष उत्पन्न होने से प्राणों के प्रसार में विषमता आती है और
प्राणों की गति में विकार होने से नाड़ियों के परस्पर संबंध में खराबी आ जाती
है। कुछ नाड़ियों की शक्ति का तो स्राव हो जाता है, कुछ में जमाव हो जाता है।
प्राणों की गति में खराबी से अन्न अच्छी तरह नहीं पचता। कभी कम, कभी अधिक
पचता है। प्राणों के सूक्ष्म यंत्रों में अन्न के स्थूल कण पहुँच जाते हैं और
जमा होकर सड़ने लगते हैं, उसी से रोग उत्पन्न होते हैं, इस प्रकार आधि
(मानसिक रोग) से ही व्याधि (शारीरिक रोग) उत्पन्न होते हैं। उन्हें ठीक करने
के लिए मनुष्य को औषधि की उतनी आवश्यकता नहीं जितनी यह कि मनुष्य अपने बुरे
स्वभाव और मनोविकारों को ठीक कर ले।
पाश्चात्य वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक और डॉक्टर अब उपरोक्त तथ्यों को और भी
गहराई तक समझने लगे हैं। 'दि फील्ड ऑफ डिसीजेज' में सर बी० डब्ल्यू रिचर्ड्सन
ने लिखा है कि-"मानसिक उद्वेग एवं चिंताओं के कारण प्रायः पुंसियाँ निकल आती
हैं, कैंसर, मिर्गी और पागलपन आदि हालत में भी सबसे पहले मानसिक जगत् में ही
विकार बढ़े होते हैं।"
वैज्ञानिकों ने दीर्घकाल तक शरीर की थकावट के कारणों की जाँच में जो प्रयोग
किये हैं, उनका कहना है कि लोगों की थकावट का कारण शारीरिक परिश्रम नहीं होता
वरन् उतावलापन, घबराहट, चिंता, विषम मनःस्थिति या अत्यधिक भावुकता होती है।
निराशा जनित घबराहट, अधूरी आशाएँ और शक्ति से अधिक कामनायें, भावुकता की
परस्पर विरोधी उलझनें भी रोगी में थकान लाती हैं। हीन भावना से भी शरीर टूटता
है। थकान से बचने के लिए आवश्यक है कि मन में सदैव प्रसन्नता और आशावादी
विचारों का संचार किये रखा जाये।
अमेरिका में हुए मनोवैज्ञानिक शोध में डॉक्टरों के एक चिकित्सा दल ने अपनी
अंतिम रिपोर्ट इस प्रकार दी है-"शारीरिक थकावट के १०० रोगियों में से ६० को
कोई शारीरिक रोग न था वरन् वे मानसिक दृष्टि से दूषित व्यक्ति थे। अपच के ७०,
गर्दन के दर्द के पीछे के ७५ सिरदर्द और चक्कर आने के ८०-८०, गले के दर्द के
६० और पेट में वायु विकार के ६६ प्रतिशत रोगी केवल भावनाओं के दुष्परिणाम से
पीड़ित थे। पेट में अल्सर जैसे दर्द और मूत्राशय में सूजन जैसी बीमारियों के
५० प्रतिशत रोगी भी निर्विवाद रूप से अपने दुर्गुणों के कारण पीड़ित थे, शेष
के बारे में कोई निश्चित राय इसलिए नहीं बनाई जा सकी, क्योंकि उनका विस्तृत
मानसिक अध्ययन नहीं किया जा सका।"
इसी प्रकार डॉ० टुके ने 'इन्फ्लुएन्स ऑफ दि माइंड अपान दि बाडी' नामक अपनी
पुस्तक में लिखा है कि पागलपन, मूढता, लकवा, अधिक पसीना आना, पांडुरोग, बालों
का शीघ्र गिरना, रक्त-हीनता, घबराहट, गर्भाशय में बच्चों की शारीरिक विकृति,
चर्मरोग, फोड़े-फुसियाँ, एग्जिमा आदि अनेक बीमारियाँ केवल मानसिक क्षोभ से ही
उत्पन्न होती हैं।
मानसिक स्थिति में विकृति आते ही शरीर का ढाँचा लड़खड़ाने लगता है। स्पष्टतः
सारे शरीर पर मन का नियंत्रण है। उसका एक अचेतन भाग रक्त-संचार,
श्वास-प्रश्वास, आकुंचन-प्रकुंचन, निद्रा, पलक झपकना, पाचन, मल-विसर्जन आदि
स्वसंचालित क्रियाकलापों पर नियंत्रण करता है और दूसरा सचेतन भाग विभिन्न
प्रकार के जीवन व्यवहारों के लिए दशों इंद्रियों को–अंग-प्रत्यंगों को सक्रिय
करता है। शरीर और मन का अविच्छिन्न संबंध है। जो इस तथ्य को जानते हैं उन्हें
विदित है कि मन को असंतुलित करने का अर्थ न केवल शोक-संतापों में डूबकर
असंतोष एवं उद्वेग की आग में जलना है वरन् अच्छे-भले शरीर को भी रोगी बना
डालना है। अगणित शारीरिक रोग मानसिक असंतुलन के कारण ही उत्पन्न होते हैं।
ऐसे ही रोगों में एक जुकाम भी है।
अनेकों कठिन बीमारियों के इलाज ढूँढ़ निकाले गये हैं, पर एक रोग आज भी ऐसा है
जो अनेकों औषधियों के उपरांत भी काबू में नहीं आ रहा है वह है-जुकाम।
शरीरशास्त्रियों के अनुसार जुकाम के भी विषाणु होते हैं। पर उनकी प्रकृति
अन्य सजातीयों से सर्वथा भिन्न है। चेचक आदि का आक्रमण एक बार हो जाने के
उपरांत शरीर में उस रोग से लड़ने की शक्ति उत्पन्न होती है। फलतः नये आक्रमण
का खतरा नहीं रहता, पर जुकाम के बारे में यह बात नहीं है। वह बार-बार और
लगातार होता रहता है। एक बार जिस दवा से अच्छा हुआ था, दूसरी बार उससे अच्छा
नहीं होता, जबकि यह बात दूसरी बीमारियों पर लागू नहीं होती।
कनाडा के एक शरीरशास्त्री और मनोविज्ञानी डॉ० डानियल कोपान का मत है-"जुकाम
उतना शारीरिक रोग नहीं जितना मानसिक है।" जब मनुष्य थका, हारा और निठाल होता
है तो उसे अपनी असफलताएँ निकट दीखती हैं, उस लांछन से बचने के लिए वह जुकाम
बुला लेता है, ताकि दूसरे उसकी हार का दोष इस आपत्ति के सिर मढ़ते हुए उसे
निर्दोष ठहरा सकें। यह रोग वस्तुतः अंतर्मन का अनुदान है, जो व्यक्ति को
स्वल्प शारीरिक कष्ट देकर उसे असफलता के लांछन से बचाता है। ऐसा रोगी बहुत हद
तक पराजय की आत्म-प्रताड़ना से बच जाता है। जुकाम की दैवी विपत्ति टूट पड़ने
से वह हारा, उसकी योग्यता, हिम्मत एवं चेष्टा में कोई कमी नहीं थी। यह मान
लेने पर मनुष्य को सांत्वना की एक हल्की थपकी मिल जाती है। अंत.चेतना इसी
प्रयोजन के लिए जुकाम का ताना-बाना बुनती है।
कोपान ने अपनी मान्यता की पुष्टि में अनेकों प्रमाण प्रस्तुत किये हैं।
खिलाड़ी लोग प्रतियोगिता के दिनों, विद्यार्थी परीक्षा के दिनों, प्रत्याशी
चुनाव तिथि पर अक्सर जुकाम पीड़ित होते हैं और इनमें अधिकांश ऐसे होते हैं
जिन्हें अपनी सफलता पर संदेह होता है और हार की विभीषिका दिल को कमजोर करती
है।
जुकाम के विषाणु होते तो हैं और उनमें एक से दूसरे को छूत लगाने की भी क्षमता
होती है, पर उतने कष्टकारक नहीं होते जितने कि मनुष्यों को पीड़ित करते हैं।
चूहे, बंदर आदि के शरीर में जुकाम के विषाणु प्रवेश कराये गये, किंतु उनके
शरीर पर कोई असर नहीं हुआ।
जुकाम का कारण सर्दी है, यह मानना भी ठीक नहीं, क्योंकि ध्रुव प्रदेश में
कड़ाके की ठंड का सामना करते हुए पीढ़ियाँ बिता देने वाले एस्किमो लोगों में
से किसी को कभी भी जुकाम नहीं होता। उस क्षेत्र में अन्वेषण के लिए जाने वाले
खोजी दलों का भी यही कथन है कि जब तक वे ध्रुव प्रदेश में रहे तब तक उन्हें
जुकाम नहीं हुआ। पर्यवेक्षणों का निष्कर्ष यह है कि शीत ऋतु में कम और गर्मी
के दिनों में जुकाम का प्रकोप अधिक होता है।
जुकाम की कितनी ही दवाएँ आविष्कृत हुईं, पर वे सभी अपने प्रयोजन में असफल
रहीं। एस्प्रीन कुछ लाभ जरूर पहुँचाती है, पर उससे दूसरी प्रकार की नई उलझनें
उठ खड़ी होती हैं, जो मूल रोग से कम कष्टकारक नहीं हैं। वस्तुत: जुकाम की
शारीरिक नहीं मानसिक रोग कहना अधिक उपयुक्त होगा। इन दिनों अधिकांश रोगों के
मूल में मानसिक विकृतियाँ सामने आ रही हैं। शरीर के अंदरूनी अवयवों में आई
खराबी के कारण उत्पन्न होने वाली परेशानियाँ तो आसानी से दूर हो जाती हैं।
शरीर स्वयं ही उनकी सफाई कर लेता है, परंतु कई घातक रोग–जिन्हें दुःसाध्य भी
कहा जाता है, मनोविकारों की ही परिणति होते हैं। मिर्गी रोग को ही लें,
मिर्गी रोग से पीड़ित मनुष्य की कैसी दयनीय स्थिति होती है, यह किसी से छिपा
नहीं है। जब दौरा पड़ता है तो सारा शरीर विचित्र जकड़न एवं हड़कंप की ऐसी
स्थिति में फंस जाता है कि देखने वाले भी डरने-घबराने लगें। जहाँ सुरक्षा की
व्यवस्था न हो वहाँ दौरा पड़ जाय तो दुर्घटना भी हो सकती है। सड़क पर गिर कर
किसी वाहन की चपेट में आ जाने, आग की समीपता होने पर जल मरने की आशंका बनी ही
रहती है। मस्तिष्कीय जड़ता के कारण बुद्धि मंद होती जाती है और क्रिया कुशलता
की दृष्टि से पिछड़ता ही जाता है। दौरा पड़ने के बाद जब होश आता है तो रोगी
अनुभव करता है-मानो कई दिनों की बीमारी के बाद उठने जैसी अशक्तता ने उसे घेर
लिया है। लोग सोचते हैं मिर्गी होने की अपेक्षा यदि एक हाथ-पॉव चला जाता तो
कहीं अच्छा रहता।
मिर्गी क्या है ? इस संबंध में खोज-बीन करने पर इतना ही जाना जा सका है कि यह
अचेतन मन में पड़ी हुई किसी ग्रंथि का अवरोध है। मस्तिष्कीय संरचना के बारे
में बहुत कुछ खोज बीन हो चुकी है और उन खोजों के आधार पर इस निष्कर्ष पर
पहुंचा गया है कि मिर्गी रोग का कारण मन में जमी हुई गहरी ग्रंथियाँ हैं।
मानसिक संतुलन में प्रत्यक्ष या परोक्ष अवरोध उत्पन्न होने से कई प्रकार के
मानसिक रोग उत्पन्न होते हैं, इनमें विविध प्रकार की मिर्गी सदृश मूच्छाएँ भी
सम्मिलित हैं।
अमेरिका के मानसिक रोग विज्ञानी राबर्ट डी० राय ने विस्तृत सर्वेक्षण के बाद
लिखा है कि-कैंसर, हृदय रोग और क्षय रोगों को उत्पन्न करने में मनोविकृतियाँ
भी प्रमुख हैं। फिर भी ऐसे व्यक्तियों की संख्या बहुत है जो मानसिक विकृति से
ग्रस्त रहते हैं। इनमें से एक तिहाई ही इलाज के लिए आते हैं, दो तिहाई तो
अपनी स्थिति को समझ तक नहीं पाते और ऐसे ही अस्त-व्यस्त स्थिति में स्वयं
दुःख पाते और दूसरों को दुःख देते हुए भटकते रहते हैं। जीन माइनोल ने अपनी
पुस्तक 'दि फिलॉसफी ऑफ लोंग लाइफ' पुस्तक में लिखा है-जल्दी मृत्यु का एक
बहुत बड़ा कारण है-मृत्यु भय। लोग बुढ़ापा आने के साथ-साथ अथवा छुटपुट
बीमारियाँ उत्पन्न होते ही मृत्यु की आशंका से भयभीत रहने लगते हैं और वह डर
उसके मस्तिष्क की बाहरी पर्तों में इस कदर धंसता जाता है कि देर तक जी सकना
कठिन बन जाता है। वह डर ही सबसे बड़ा रोग है जो मृत्यु को अपेक्षाकृत जल्दी
ही समीप लाकर खड़ा कर देता है।
अरब देशों में कुछ शताब्दियों पूर्व एक प्रख्यात चिकित्सक हुआ है-हकीम
इब्नसीना। उसने अपनी पुस्तक 'कानून' में अपने ऐसे अनेकों चिकित्सा अनुभवों का
उल्लेख किया है कि अमुक प्रकार के मानसिक उभारों के कारण शरीर में अमुक
प्रकार की विकृतियाँ या बीमारियाँ उठ खड़ी होती हैं। चिकित्सा उपचार में उसने
दवादारू के स्थान पर उनकी मनःस्थिति बदलने के उपाय बरते और असाध्य लगने वाले
रोग आसानी से अच्छे हो गए।
'इलिनोयस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी' द्वारा संग्रहीत आँकडे यह बताते हैं कि
चिंतातुर व्यक्तियों को जिस भयभीत स्थिति में रहते हुए अपनी शांति गँवानी
पड़ती है, उसका वास्तविक अस्तित्व कम और काल्पनिक बबंडर अधिक होता है। जो
आशंका, आतंक उन पर छाया रहता है, उसका मूर्तिमान रूप कदाचित ही कभी सामने आता
है।
येल विश्वविद्यालय के मनोविज्ञान विभाग ने भयभीत मनःस्थिति का शरीर पर बुरा
प्रभाव पड़ने और स्वास्थ्य नष्ट होने की प्रतिक्रिया के अनेक तथ्य प्रस्तुत
करते हुए प्रमाणित किया है-चिंता अथवा भय की स्थिति में पड़े हुए व्यक्तियों
के दिल की धड़कन बढ़ जाती है, बड़ी तेज चलने लगती है, गला सूखता है, पसीना
छूटता है, कमजोरी अनुभव होती है और पेट बैठता-सा लगता है और सिर पर बोझ
लदा-सा अनुभव होता है, नींद घट जाती है और स्मरण शक्ति झीनी पड़ती चली जाती
हैं।
चिंता सामान्य और भयभीतता बढ़ी हुई स्थिति है। वस्तुतः दोनों एक ही बीमारी के
हल्के-भारी दो रूप हैं, उनका शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसका विश्लेषण
करते हुए आयोग ने बताया कि सिर दर्द की स्थिति में जो शारीरिक संतुलन बिगड़ता
हैउसकी तुलना में चिंता में ड्योढ़ी और भयभीत स्थिति में दूनी गड़बड़ी
उत्पन्न होती है। शरीर को इसी अनुपात में दबाव सहन करना पड़ता है।
आयोग ने एक आश्चर्यजनक तथ्य यह भी देखा है कि मानसिक रोगियों का इलाज
करते-करते स्वयं मानसोपचारक भी चिंतित रहने लगते हैं। अचेतन उन्हें भी बख्शता
नहीं। दूसरों को उपदेश देने और इलाज करने के बावजूद वे स्वयं भी सामान्य
कठिनाइयों में बेतरह उलझे पाये जाते हैं। आश्चर्य यह है कि अपनी जैसी स्थिति
में दूसरे व्यक्ति को रोगी गिनते हैं और अपने को निरोग। यह छूत की बीमारी
उन्हें अपने रोगियों से और वैसी ही बातों की उधेड़ बुन करते रहने के कारण लग
गई होती है। आयोग का सुझाव है कि मानसोपचार का कार्य बहुत ही सुदृढ़
मनःस्थिति के 'मस्त मौला' लोगों को करना चाहिए।
चिंतातुर व्यक्तियों का पूर्व इतिहास खोजने पर यह निष्कर्ष निकला है कि वे
दुराव रखने वाले और आडंबर बनाने वाले, बहानेबाज एवं ढोंगी रहे होते हैं।
छिपाव की वृत्ति अपने नये रूप के चिंता बनकर मस्तिष्क में जड़ जमाती है और
बढ़ने पर भयाक्रांत, आशंकाग्रस्त बना देती है, ऐसे मनुष्य पग-पग पर अपने ऊपर
कोई बड़ा संकट अब-तब आता देखते रहते हैं। यद्यपि उन आशंकाओं में एकाध का ही
सामना किसी-किसी को करना पड़ता है।
साइकोन्यूरोटिक की स्थिति यह है कि उसमें कई विचारों का समन्वय करके तर्क और
बुद्धि का ठीक तरह उपयोग नहीं हो पाता। कुछ एकांगी मान्यताएँ ही मस्तिष्क पर
छाई रहती हैं और मनुष्य बिना सोच विचार किये उन्हें ही सच मानता और अपनाये
रहता है। यह अविकसित मस्तिष्क का चिह्न है। इसे बाल बुद्धि कह सकते हैं। छोटे
बच्चों में भी तर्क शक्ति विकसित नहीं होती, वे इच्छाओं, उत्साहों और भावनाओं
में ही प्रेरित रहते हैं।
नशेबाजी और अपराधियों में भी इस रोग के लक्षण उभरे रहते हैं। वे अपनी आदतों
के विरुद्ध सुनते तो बहुत कुछ हैं, पर अचेतन उनसे प्रभावित नहीं होता और जो
आदत अपना ली गई है वह हर हालत में अपने ढर्रे पर चलती ही रहती है।
अंधविश्वासी तथा अति भावुक व्यक्ति भी आंशिक रूप में इसी व्यथा के चंगुल -
में फँसे होते हैं।
ऐक्जाइटी न्यूरोसिस-दुश्चिंता से अनेकानेक घिरे देखे पाये जा सकते हैं। चिंता
वास्तविक है या अवास्तविक ? निकट भविष्य में जिस आशंका की विभीषिका कल्पित की
गई है वह आने वाली भी है या नहीं ? इन दिनों जिस संकट में अपने को जकड़ा हुआ
मान लिया गया है वह अपनी मान्यता के अनुरूप भयंकर है भी या नहीं ? यह सोचने
को ऐसे लोगों को फुरसत ही नहीं होती। वे अपनी भयंकर कल्पना को निरंतर सोचते
और परिपुष्ट करते रहते हैं, अस्तु वह इतनी प्रबल एवं प्रभावशाली बन जाती हैं
कि अवास्तविक होते हुए भी वास्तविकता से भी अधिक त्रास देती है। वास्तविक
संकट आने पर शायद उतना कष्ट न सहना पड़ता जितना उस अवास्तविक कल्पना ने दे
डाला, इस निष्कर्ष पर पहुँच सकना उनसे बन ही नहीं पड़ता।
आब्सेसिव कंपलसिव न्यूरोसिस में भीतर की घुटन बाहर फूट पड़ती है। दुश्चिताएँ
मस्तिष्क के भीतर तक सीमित नहीं रहती वरन् उस दीवार को फोड़ कर बाहर निकल
पड़ती है और क्रिया के साथ संबद्ध होकर ऐसे आचरण प्रस्तुत करती है जो
उपहासास्पद होते हैं और दयनीय भी। यों उसे ऐसा लगता है मानो चिंताएँ, पीड़ा
एवं प्रताड़ना के रूप में उसे संत्रस्त कर रही है, अस्तु यह रोता कलपता एवं
सिर धुनता हुआ देखा जाता है। आँखों में से आँसू, सिर में दर्द, चेहरे पर छाई
विषाद की गहरी रेखा देखकर देखने वाला यही कह सकता है, इसे बहुत कुछ सहना पड़
रहा है और किसी भारी संकट से होकर गुजरना पड़ रहा है।
इस रोग का रोगी हर समय अपने इर्द-गिर्द अपवित्रता घिरी देखता है। आँतों में
मल, कंठ में कफ भरा रहने की शिकायत रहती है। हाथ, पैर, मुँह धोने और कुल्ला
करने की बार-बार आवश्यकता पड़ती है। बर्तन, कपड़े, फर्श, बिस्तर, फर्नीचर आदि
गंदे लगते हैं, इसलिए उन्हें अनेक बार धोते रहने पर भी संतोष नहीं होता और
वही क्रिया उलट-पुलट कर फिर करने को जी करता है। दूसरे पूछ सकते हैं अथवा
अपनी तर्क बुद्धि जबाव तलब कर सकती है कि यह सब बार-बार क्यों किया जा रहा
है? इसलिए अचेतन मन उसका उत्तर देने के लिए कुछ न कुछ बहाना भी गढ़ लेता है।
उससे उसे यह संतोष हो जाता है, यह क्रिया निरर्थक नहीं वरन् सार्थक की जा रही
है।
हताश हुए मनुष्य अपना मस्तिष्क संतुलन खो बैठते हैं और अवसाद ग्रस्त होकर
सामान्य शरीर संचालन के क्रियाकलापों तक से वंचित हो जाते हैं। खाने, सोने और
नित्य कर्म करने भर की याद तो रहती है, पर अन्य उत्तरदायित्वों और निर्धारित
कर्तव्यों को एक प्रकार से भूल ही जाते हैं। याद दिलाने पर ही कुछ कर पाते
हैं, अन्यथा खोये-खोये से, भूले-भाले से, जहाँ-तहाँ बैठे किसी स्वप्नलोक में
विचरते रहते हैं। गहरी निराशा से ऐसी या इससे मिलती-जुलती स्थिति बन जाती है,
इसे मानसिक चिकित्सा के संदर्भ में एजीटेटेड डिप्रेसिव साइकोसिस कहते हैं।
अपनी निजी उलझनों के संबंध में अत्यधिक उलझे रहना और उन्हीं पर उलट-पुलट कर
विचार करते रहना एक ऐसा गलत क्रम है जिससे मनुष्य संकीर्णता ग्रस्त हो जाता
है और उसे तरह-तरह के मनोविकार धर दबोचते हैं। इस स्थिति को न्यूरेस्थीनिया
कहते हैं।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की पिछली वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार अपने देश
में इस समय लगभग एक करोड़ से अधिक मानसिक रोगी हैं। इनमें से कम से कम आठ लाख
से अधिक तो ऐसे हैं जिन्हें पागल खानों में स्थान मिलना चाहिए अन्यथा वे
दूसरे लोगों की शांति भंग करते ही रहेंगे। ऐसे लोग जो मानसिक दृष्टि से छोटे
से छोटे बच्चों जैसी अविकसित स्थिति में रह कर गुजार रहे हैं लगभग १६ लाख से
अधिक है।
मनुष्य समाज में बढ़ रही मानसिक अक्षमता और विकारग्रस्तता का प्रमुख कारण यह
है कि हमारा थोड़ा-बहुत ध्यान स्वास्थ्य की उपयोगिता समझने पर तो गया भी है,
पर मानसिक स्वास्थ्य की बात एक प्रकार से विस्मृत ही कर दी गई है। मानसिक
दृष्टि से अविकसित स्त्री, पुरुषों की संतानें पैतृक उत्तराधिकार के रूप में
अदक्षता लेकर जन्मता है और फिर बच्चों के मानसिक परिष्कार की कोई व्यवस्था न
होने से वे क्रमशः बढ़ती ही जाती हैं।
|
|||||