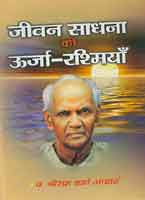|
आचार्य श्रीराम शर्मा >> आत्मा और परमात्मा का मिलन संयोग आत्मा और परमात्मा का मिलन संयोगश्रीराम शर्मा आचार्य
|
111 पाठक हैं |
||||||
आत्मा और परमात्मा का मिलन संयोग
क्या 'मैं' शरीर ही हूँ-उससे भिन्न नहीं?
मैं क्या हूँ ? मैं कौन हूँ? मैं क्यों हूँ ? इस छोटे से प्रश्न का सही समाधान न कर सकने के कारण 'मैं' को कितनी विषम विडम्बनाओं में उलझना पड़ता है और विभीषिकाओं में संत्रस्त होना पड़ता है, यदि यह समय रहते समझा जा सके तो हम वह न रहें, जो आज हैं। वह न सोचें जो आज सोचते हैं। वह न करें जो आज करते हैं।
हम कितने बुद्धिमान् हैं कि धरती आकाश का चप्पा-चप्पा छान डाला और प्रकृति के रहस्यों को प्रत्यक्ष करके सामने रख दिया। इस बुद्धिमत्ता की जितनी प्रशंसा की जाय उतनी कम और अपने आपके बारे में जितनी उपेक्षा बरती गई उसकी जितनी निन्दा की जाय वह भी कम ही है।
जिस काया को शरीर समझा जाता है क्या यही मैं हूँ? क्या कष्ट, चोट, भूख, शीत, आतप आदि से पग-पग पर व्याकुल होने वाला अपनी सहायता के लिये बजाज, दर्जी, किसान, रसोइया, चर्मकार, चिकित्सक आदि पर निर्भर रहने वाला ही मैं हूँ? दूसरों की सहायता के बिना जिसके लिए जीवन धारण कर सकना कठिन हो-जिसकी सारी हँसी-खुशी और प्रगति दूसरों की कृपा पर निर्भर हो, क्या वही असहाय, असमर्थ, मैं हूँ? मेरी आत्म-निर्भरता क्या कुछ भी नहीं है? यदि शरीर ही मैं हूँ तो निस्संदेह अपने को सर्वथा पराश्रित और दीन, दुर्बल ही माना जाना चाहिए।
परसों पैदा हुआ, खेल-कूद, पढ़ने-लिखने में बचपन चला गया। कल जवानी आई थी। नशीले उन्माद की तरह आँखों में, दिमाग में छाई रही। चंचलता और अतृप्ति से बेचैन बनाये रही। आज ढलती उम्र आ गई। शरीर ढलने गलने लगा। इन्द्रियाँ जवाब देने लगीं। सत्ता, बेटे, पोतों के हाथ चली गई। लगता है एक उपेक्षित और निरर्थक जैसी अपनी स्थिति है। अगली कल यही काया जराजीर्ण होने वाली है। आँखों में मोतिया बिन्द, कमर घुटनों में दर्द, खाँसी, अनिद्रा जैसी व्याधियाँ, घायल गधे पर उड़ने वाले कौओं की तरह आक्रमण की तैयारी कर रही है। अपाहिज और अपंग की तरह कटने वाली जिंदगी कितनी भारी पडेगी। यह सोचने को जी नहीं चाहता, वह डरावना और घिनौना दृश्य एक क्षण के लिए भी आँखों के सामने आ खड़ा होता है तो रोम-रोम काँपने लगता है ? पर उस अवश्यम्भावी भवितव्यता से बचा जाना सम्भव नहीं? जीवित रहना है तो इसी दुर्दशाग्रस्त स्थिति में पिसना पड़ेगा। बच निकलने का कोई रास्ता नहीं।
क्या यही मैं हूँ? क्या इसी निरर्थक विडम्बना के कोल्हू के चक्कर काटने के लिए 'मैं' जन्मा? क्या जीवन का यही स्वरूप है? मेरा अस्तित्व क्या इतना ही तुच्छ है?
आत्म चिन्तन कहेगा-नहीं-नहीं-नहीं। आत्मा इतना हेय और हीन नहीं हो सकता। वह इतना अपङ्ग और असमर्थपराश्रित और दुर्बल कैसे होगा? यह तो प्रकृति के पराधीन पेड़-पौधों जैसा-मक्खी, मच्छरों जैसा जीवन हुआ। क्या इसी को लेकर-मात्र जीने के लिए मैं जन्मा। सो भी जीना ऐसा जिसमें न चैन, न खुशी, न शान्ति, न आनन्द, न सन्तोष। यदि आत्मा-सचमुच परमात्मा का अंश है तो वह ऐसी हेय स्थिति में पड़ा रहने वाला हो ही नहीं सकता। या तो मैं हँ ही नहीं। नास्तिकों के प्रतिपादन के अनुसार या तो पाँच तत्वों के प्रवाह में एक भँवर जैसी बबले जैसी क्षणिक काया लेकर उपज पड़ा हूँ और अगले ही क्षण अभाव के विस्मृति गर्त में समा जाने वाला हूँ। या फिर कुछ हूँ तो इतना तुच्छ और अपङ्ग हूँ जिसमें उल्लास और सन्तोष जैसा-गर्व और गौरव जैसा-कोई तत्व नहीं है। यदि मैं शरीर हूँ तो-हेय हूँ। अपने लिए और इस धरती के लिए भारभूत। पवित्र अन्न को खाकर घृणित मल में परिवर्तन करते रहने वाले-कोटि-कोटि छिद्रों वाले इस कलेवर से दुर्गन्ध और मलीनता निसृत करते रहने वाला-अस्पर्श्य-घिनौना हूँ 'मैं'। यदि शरीर हूँ तो इससे अधिक मेरी सत्ता होगी भी क्या?
|
|||||