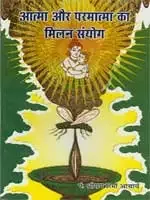|
आचार्य श्रीराम शर्मा >> आत्मा और परमात्मा का मिलन संयोग आत्मा और परमात्मा का मिलन संयोगश्रीराम शर्मा आचार्य
|
111 पाठक हैं |
||||||
आत्मा और परमात्मा का मिलन संयोग
व्यक्ति जब अपने को ईश्वर का परम-पवित्र अविनाशी अंश समझता है; आत्मा के रूप में अनुभव करता है और शरीर को एक उपकरण भर स्वीकार करता है। तो उसे अपनी पिछली मान्यताओं, आकाँक्षाओं योजनाओं और गतिविधियों में आमूल चूल परिवर्तन करने की आवश्यकता अनुभव होती है। सम्बन्धित वस्तुएँ संग्रह करके निरर्थक मोह बढ़ाने के लिए नहीं, वरन् सदुपयोग भर के लिए अपने पास एकत्रित हुई हैं। यह निष्ठा जब जमती है तो फिर लोभ और मोह में परले सिरे की मूर्खता ही दिखाई देती है। सम्पदा प्रकृति का ही एक रूप है। यह अनादि काल से चली आ रही है और अनन्तकाल तक चली जायेगी। जो सोना अपने पास आज है वह सृष्टि के जन्मकाल से ही इस संसार में विद्यमान था। उस पर लाखों व्यक्ति कुछ-कुछ देर के लिए अपना अधिकार बनाते चले आ रहे हैं। प्रलय-काल तक वह सोना बना रहेगा और उस पर करोड़ों व्यक्ति अपना अधिकार जमाते चले जायेंगे। जमीन, जायदाद, वस्तुएँ आदि सृष्टि के साथ जन्मी और उसके रहने तक इस दुनिया में बनी रहेंगी, कुछ समय के लिए वे अपने साथ संयोगवश जुड़ गईं तो उन्हें अपनी मान बैठना, उनके संग्रह का लोभ करना, कैसे उचित ठहराया जा सकता है? पदार्थों का मोह जिस शरीर के साथ जुड़ा हुआ है वह शरीर ही कल परसों जाने की तैयारी में बैठा है फिर पदार्थों का-सम्पदा साधनों का लोभ किए लिए?
उपलब्ध सम्पत्ति का सदुपयोग ही सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता है उसकी जमाखोरी में कोई समझदारी नहीं। उपार्जन को श्रेष्ठ प्रयोजनों में लगाना चाहिए। बेटे-पोतों के लिए उत्तराधिकार का ताना बाना बुनना सदुपयोग नहीं। अपने साथ मोह बन्धनों में बँधे हुए चन्द व्यक्तियों को अपने श्रम का सार उपार्जन सौंप दिया जाय और वे उस हराम की कमाई पर गुलछर्रे उड़ायें इस विडम्बना में क्या औचित्य है? श्रम उपार्जन का खाकर ही कोई व्यक्ति उसका लाभ लेता है, हराम की कमाई तो हर किसी को गलाती है। आत्मवादी की सनिश्चित मान्यता यही हो सकती है। जिसकी समझ में यह तथ्य आ गया उसे नये सिरे से अपनी सम्पत्ति के बारे में चिन्तन करना पड़ेगा और आश्रित, असमर्थ परिजनों की उचित व्यवस्था के अतिरिक्त जो कछ उसके पास बच जाता है उसे लोक-मङ्गल के लिए नियोजित करने का ही निर्णय करना पड़ता है। आत्म-बोध के साथ यदि इस स्तर का दुस्साहस जुड़ा हुआ न हो तो उसे बकवादियों का बाल-विनोद ही कहा जायेगा। असंख्यों व्यक्ति स्वाध्याय सत्संग के नाम पर धर्म और अध्यात्म की लम्बी-चौड़ी बकवास करते और सुनते रहते हैं। जो चिन्तन-जीवन को प्रभावित न कर सके उसे मनोविनोद के अतिरिक्त और क्या कहा समझा जा सकता है।
परिवार के रूप में जुड़े हुए कुछ व्यक्ति ही अपने हैं? अपना प्यार उन्हीं तक सीमित रहना चाहिए? उन्हीं तक अपनी सारी महत्वाकांक्षायें सीमित कर लेनी चाहिए, यह रीति-नीति उससे बन ही नहीं पड़ेगी जो अपने को 'आत्मा' मानेगा। आत्म-ज्ञान का प्रकाश आते ही दृष्टिकोण में उस विशालता का समावेश होता है जिसके अनुसार 'वसुधैव कुटुम्बकम्' मानने से कम में किसी भी प्रकार संतोष नहीं हो सकता।
|
|||||