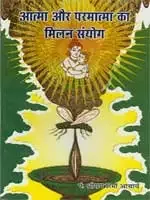|
आचार्य श्रीराम शर्मा >> आत्मा और परमात्मा का मिलन संयोग आत्मा और परमात्मा का मिलन संयोगश्रीराम शर्मा आचार्य
|
111 पाठक हैं |
||||||
आत्मा और परमात्मा का मिलन संयोग
भगवान् के उद्यान के रूप में-सम्बन्धित परिवार को कर्तव्य-निष्ठ माली की तरह सींचना सँजोना बिलकुल अलग बात है और बेटे-पोतों के लिए मरते-खपते रहना अलग बात, बाहर से देखने में यह अन्तर भले ही दिखाई न पड़े पर दृष्टिकोण की कसौटी पर रखने पर जमीन आसमान जितना अन्तर मिलेगा। मोहग्रस्त मनुष्य अपने कुटुम्बियों की सुविधा, सम्पदा बढ़ाने और इच्छा पूरी करने की धुन में उचित अनुचित-आवश्यक-अनावश्यक का भेद भूल जाता है और घरवालों की इच्छा तथा खुशी के लिए वह व्यवस्था भी जुटाता है जो न आवश्यक है न उपयुक्त। मोह-ग्रस्त के पास विवेक रह ही नहीं सकता।
परिष्कृत दृष्टि से कुटुम्बियों को समुन्नत, सुसंस्कारी, सुविकसित बनाने के कर्तव्य को ही ध्यान में रखकर पारिवारिक विधि-व्यवस्था निर्धारित की जाती है। उसमें यह नहीं सोचा जाता कि कौन राजी रहा कौन नाराज हुआ। चतुर माली अपनी दृष्टि से पौधों को काटता छाँटता-निराता गोड़ता है, पौधों की मर्जी से नहीं। विवेकवान् गृह-पति केवल एक ही दृष्टि रखता है कि परिवार को सुसंस्कारी और सुविकसित बनाने के लिए जो कठोर कर्तव्य पालने चाहिए उनका पालन अपनी ओर से किया जा रहा है या नहीं। परिजनों की इच्छाओं का नहीं उनके हित साधन का ही उसे ध्यान रहता है। आत्मबोध के साथ परिवार के प्रति इसी दृष्टिकोंण के अनुरूप आवश्यक हेर-फेर करना पड़ता है। तब वह मोह छोड़ता है और प्यार करता है। प्यार के आधार पर की गई परिवार सेवा उसके स्वयं के लिए और समस्त परिवार के लिए परम-मङ्गलमय सिद्ध होती है।
अपने शरीर के बारे में भी आत्म-बोध के प्रकाश में नई रीति-नीति ही. अपनानी पड़ती है। उसे वाहन उपकरण मात्र मानना पड़ता है। आत्मा की भूख के लिए शरीर से काम लेने और शरीर की लिप्सा के लिए आत्मा को पतन के गर्त में डालने की दृष्टि में जमीन आसमान जितना अन्तर है। शरीर और मन को 'मैं' मान बैठने पर इन्द्रियों की वासनायें और मन की तृष्णायें ही जीवनोद्देश्य बन जाती हैं और उन्हीं की पूर्ति में निरन्तर लगा रहना पड़ता है। पर जब वह मान्यता हट जाती और अपने को आत्मा स्वीकार कर लिया जाता है तो मन को बलात् उस चिन्तन में नियोजित किया जाता है जिससे आत्म-कल्याण हो और शरीर से वह कार्य कराये जाते हैं जो आत्मा का गौरव बढ़ाते हों उसका भविष्य उज्ज्वल बनाते हों।
आत्म-बोध, एक श्रद्धा है। आत्म-साक्षात्कार एक दर्शन है, जिसे यदि सचाई के साथ हृदयंगम किया जाय तो दृष्टिकोण ही नहीं बदलता वरन् क्रिया-कलाप भी बदल जाता है। इस परिवर्तन को ही आत्मिक कायाकल्प कहते हैं। यह जिस क्षण भी सम्भव हो जाय उसी दिन अपने में भारी शान्ति, संतोष, उल्लास और उत्साह दृष्टिगोचर होता है और लगता है मानो नरक से निकल कर स्वर्ग में आ गये।
|
|||||