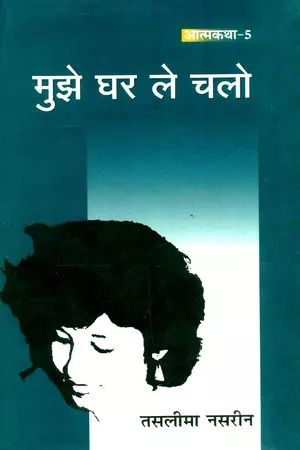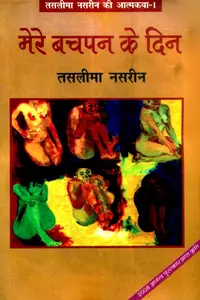|
जीवनी/आत्मकथा >> मुझे घर ले चलो मुझे घर ले चलोतसलीमा नसरीन
|
419 पाठक हैं |
|||||||
औरत की आज़ादी में धर्म और पुरुष-सत्ता सबसे बड़ी बाधा बनती है-बेहद साफ़गोई से इसके समर्थन में, बेबाक बयान
लेकिन अन्य भाषाओं में बांग्ला का अनुवादक पाना आज तक संभव नहीं हो सका है। आज भी वे लाग ता अंग्रेजी या फ्रेंच से या अन्य किसी यूरोपीय भाषा से ही अनुवाद किया जाता है, लेकिन 'लज्जा' के बाद, अव वह आग्रह भी नहीं रहा। फ्रेंच और जर्मन के अलावा, यूरोप की अन्य भापाओं के प्रकाशक भी मेरी खोज करते है, लेकिन वहद कम! मुझे विल्कुल आसमान पर चढ़ा दिया था। आसमान से अगर धप्प से ज़मीन पर आ गिरे तो बेहद कम समय में काम निवट जाता है। ऐसी स्थिति में या तो मौत हो जाती है या लोगों की भीड़ में घुल-मिल जाती है और अलग से उसकी पहचान ख़त्म हो जाती है, लेकिन आसमान से ज़मीन पर अगर धीरे-धीरे उतारा जाता है तो बहुत-बहुत-सी जगहों में चोट-ज़ख्म खाते-खाते, खून में तर-ब-तर हो जाते हैं! बेहद अकेले भी हो जाते हैं। आस-पास भला कोई रहता है? हाँ, शायद रहता है, हमें नीचे उतरते हुए देखते रहने के लिए! जो लोग मेरे बारे में बड़े-बड़े सपने देख रहे थे, अब उन्हीं लोगों ने मुँह फेर लिया है और दूसरों से बातचीत में व्यस्त हो गए है। उन लोगा के सपनं, भले ही मुझम मामूला ढंग से सक्रमित हए हों, मुमकिन है टूटने का दर्द भी वर्दाश्त-लायक हो, मगर अंदर ही अंदर अकेले हो जान की दुःसह पीड़ा भी विद्यमान है। धीरे-धीरे सैकड़ों चमगादगड़, हताशा के पंख फैलाए, मेरी तरफ बढ़ते रहे। चारों तरफ घुप्प अंधेरा ही अंधेरा!
साल-दर-साल गुज़रते जा रहे हैं। अभी भी जिस देश में निवास कर रही हूँ, उस देश की भापा मैं नहीं सीख पाई, सीखने में मेरी कोई दिलचस्पी भी नहीं है। कोई इसकी वजह जानना चाहता है तो मैं वजह भी बता देती हूँ। वजह यह है कि मैं विदेश में रहने तो आई नहीं। यहाँ मैं मेहमान के तौर पर, बस कुछ दिनों के लिए आई हूँ। मेरे देश के दरवाज़े, मेरे लिए खुलते ही मैं अपने देश लौट जाऊँगी। अपनी भाषा अच्छी तरह सीख नहीं पाई, दूसरों की भाषा क्या सीखूगी! लेकिन दिन गुजरते जा रहे हैं, अभी तक मेरी वापसी नहीं हुई। विदेश की धरती पर मैं विदेशी के तौर पर ही दिन गुज़ार रही हूँ। अतिथि से ज़्यादा आगन्तुक बनकर! यहाँ की भापा मुझे नहीं आती। यहाँ के रास्ते-घाट, दुकान-पाट में, मैं घरेलू नहीं, कोई बाहरी प्राणी हूँ। मुझे यहाँ की भाषा की ही समझ नहीं है! मामूली-से औपचारिक वाक्य तक मैंने नहीं सीखे। कैसे हो? मैं ठीक हूँ-जैसे अति आसान वाक्य भी, इन तीन वर्षों में, मैं नहीं सीख पाई। यह अनिच्छा आखिर आई कहाँ से? अवज्ञा की वजह से या भय की वजह से? शायद भय की वजह से ही। कहीं मुझे यह न लगे कि भाषा सीखने का मतलव है कि इस समाज के साथ अपना तालमेल बिठा लेना, इस परिवश में भी स्वच्छंदता महसूस करना। हाँ, मुझे भाषा सीखने में डर लगता है, मैंने न स्वीडिश सीखी, न जर्मन, न फ्रेंच! अंग्रेजी ही अच्छी तरह सीख लूँ, मुझसे यह भी नहीं हुआ। जितनी मामूली-सी अंग्रेज़ी जानती हूँ, अगर उतने-से ही वक्त गुजरता रहे तो ज़्यादा जानकारी की आखिर क्या ज़रूरत है? वल्कि वांग्ला में वातचीत बंद हो जाने की वजह से, मेरी वांग्ला भी जाने किस नर्क में जा पड़ी है, मैं तो इसी दुश्चिंता में पड़ी रहती हूँ। कागज-कलम लेकर यूँ कम्प्यूटर के सामने बैठे-बैठे, कई-कई दिन गुज़र जाते हैं, कुछ भी लिखा नहीं जाता। प्रकाशकों की फर्माइश है कि पूरे साठ दिनों तक मैंने जो छिप-छिपकर जिंदगी गुज़ारो, मैं वह सारा कुछ लिख डालूँ! अंकुर नामक एक प्रकाशक ने तो 'वे साठ दिन' का कवर भी तैयार कर डाला है! लेकिन नहीं, मेरे लिए और सव भले ही संभव हो, लिखना संभव नहीं होता। उन साठ दिनों की भयावह याद, मुझमें फिर-फिर कंपकंपी भर देती है, उसके बाद सब कुछ स्तब्ध हो जाता है। मुझसे एक अक्षर भी लिखा नहीं जाता। मैं जैसे किसी अनाम-लेखिका की तरह जिंदगी गुज़ार रही हूँ। वंस, खाती-पीती हूँ, घूमती-फिरती हूँ, नाटक-फिल्में देखती हूँ, अड्डा देती हूँ, सो जाती हूँ। सेमिनार-कांफ्रेंस में शामिल होती हूँ। किसी ज़माने में किसी देश में, मैं लेखिका भी थी, कभी-कभी मैं यह भी भूल जाती हूँ। भाई ने अखबारों की तमाम कटिंग्स चिपकाकर एक फाइल भेजी है। सारी कहानियाँ, औरतों पर अत्याचार के वारे में हैं। उत्साह से भरकर उन्होंने उस किताब का नाम भी दे डाला है-'व्हिप ऑन वुमेन' ! लेकिन वह चाबुक भी धीरे-धीरे कागजों के ढेर तले गुम हो गया।
|
|||||
- जंजीर
- दूरदीपवासिनी
- खुली चिट्टी
- दुनिया के सफ़र पर
- भूमध्य सागर के तट पर
- दाह...
- देह-रक्षा
- एकाकी जीवन
- निर्वासित नारी की कविता
- मैं सकुशल नहीं हूँ