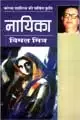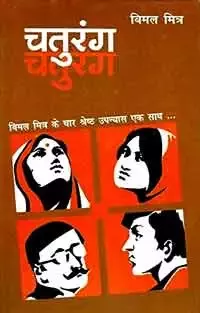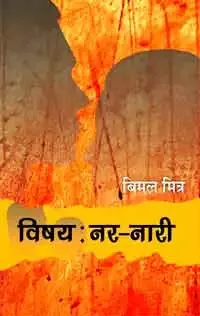|
कहानी संग्रह >> विमल मित्र की चुनिंदा कहानियाँ विमल मित्र की चुनिंदा कहानियाँविमल मित्र
|
416 पाठक हैं |
||||||
जीवन की, जिन्दगी की, इंसानियत की, अनेकों विविधायामी आयामों की सतरंगी आभा को उकेरती ये कहानियां
प्रस्तुत हैं पुस्तक के कुछ अंश
बाँग्ला साहित्य विशेषकर विमल मित्र का कथा-साहित्य विपुल मात्रा में
हिन्दी में अनूदित होकर खूब पढ़ा और सराहा जा रहा है, तो उसका कारण है
अनुवादकों की निष्ठा जो हिन्दी पाठक को उन कहानियों के परिवेश, वैचारिक
जगत व अन्य आयामों के इतने सूक्ष्म स्तर तक ले जाते हैं जहां मूल और
अनुवाद एकाकार होकर पाठकीय मनो-जगत को अपने साथ तादात्म कर लेते हैं। यही
बिन्दु इन कहानियों को पठनीय और संग्रहणीय बनाता है।
जीवन की, जिन्दगी की, इंसानियत की, अनेकों विविधायामी आयामों की सतरंगी आभा को उकेरती, नदी की अजस्र धारा की तरह कहीं अवरुद्ध, कहीं तरंगायित तो कहीं भयावह उद्दामता की कही, अनकही बाहर-भीतरी परतों को उकेरती ये कहानियां सच में ही पाठक को दूर तक और देर तक अपने साथ बनाये रखती हैं इसीलिये इन्हें विमल मित्र की चुनिन्दा कहानियां कहा ही नहीं जा सकता वरन् ये अपनी सार्वकालिकता में चुनिंदा और प्रतिनिधि हैं।
जीवन की, जिन्दगी की, इंसानियत की, अनेकों विविधायामी आयामों की सतरंगी आभा को उकेरती, नदी की अजस्र धारा की तरह कहीं अवरुद्ध, कहीं तरंगायित तो कहीं भयावह उद्दामता की कही, अनकही बाहर-भीतरी परतों को उकेरती ये कहानियां सच में ही पाठक को दूर तक और देर तक अपने साथ बनाये रखती हैं इसीलिये इन्हें विमल मित्र की चुनिन्दा कहानियां कहा ही नहीं जा सकता वरन् ये अपनी सार्वकालिकता में चुनिंदा और प्रतिनिधि हैं।
-कान्ती प्रसाद शर्मा
संपादकीय
विश्व साहित्य हो या एक सम्पूर्ण राष्ट्रभाषा का साहित्य हो या कोई
क्षेत्रीय भाषा का साहित्य हो उसमें से किसी विशेष लेखक की प्रतिनिधि
रचनाओं का चयन करना अत्यंत दुष्कर कार्य है। एक रचनाकार की प्रतिनिधि
कविताओं या कहानियों का चयन करते समय हजारों-हजार प्रश्न, शंकाएं, कहें
अनेकों कसौटियां रू-ब-रू होती हैं। कोई रचना किसी परिप्रेक्ष्य में
प्रतिनिधित्व करती है तो कोई किसी अन्य क्षेत्र में। ऐसी कसौटियों के बीच
से किसी लेखक की प्रतिनिधि कहानियों का चयन सचमुच जीवटता और निर्मम सत्य
के उद्घाटन की जिजीविषा का जीवन्त उदाहरण है।
‘विमल मित्र की चुनिंदा कहानियां’ पुस्तक में संपादक और अनुवादक दोनों ही उपरोक्त कसौटियों पर खरे उतरे हैं। इन कहानियों से गुजरने से पहले रवीन्द्रनाथ ठाकुर के इस कथन पर विशेष गौर कर लें—‘मैं बचपन से केवल आंख के द्वारा देखने का अभ्यस्त था। आज एकाएक मैंने अपनी पूरी चेतना से देखना शुरू किया।’ तो ललाट की आंखों से देखकर समझने का गुमान कितना भ्रामक है। उनसे कुछ नहीं दिखता, केवल चैतन्य की आंखों से, आत्मा की आंखों से सत्य की झांकी मिल सकती है’ ‘सहज को दुरूह करके जब पाया जाता है, तभी पाना सार्थक होता है।’ और हम सहज में सब कुछ हथिया लेना चाहते हैं—हिमालय को, गंगा-गोदावरी को। पर हिमालय और समूची गंगा को निगलने के बाद हमारा पेट तो वैसा ही खाली रह जायेगा। पेट की क्षुधा या शरीर की क्षुधा भला कब शान्त होने वाली है। यह जठराग्नि तो हमारी आत्मा, हमारी बुद्धि तक स्वाहा कर डालेगी। और हम पश्चिम की ही नकल करने में मगन हैं, उनके मनीषियों को महिमामंडित करने में, पढ़ने में गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं।
इस सांस्कृतिक गुलामी की ‘भूल सूधार’ के रूप में प्रस्तुत पुस्तक ‘विमल मित्र की चुनिंदा कहानियां’ का संचयन है। देश मनुष्य की सृष्टि है। वह मृण्मय नहीं, चिन्मय है। यदि मनुष्य प्रकाशमान हो तभी देश प्रकाशित होता है।...देश मिट्टी से नहीं मनुष्यों से बनता है। साथ ही साथ यह भूलने से भी काम नहीं चलेगा कि माल मनुष्य का है, मनुष्य स्वयं माल नहीं है। वह अपने विश्व-जगत को केवल माल का संसार बना लेगा तो अपने आपको मनुष्य कहकर पहचानेगा कैसे ? विमल मित्र की चुनिंदा कहानियों में ठौर-ठौर ऐसा अमृत छलक रहा है। समय काटने के निमित्त, मनोरंजन की ओट में, अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर, जो हलाहल उंडेला जा रहा है, उस घातक मंत्रणा के प्रतिरोध में ये कहानियां अपनी सम्पूर्ण क्षमता के साथ खड़ी हैं।
जब नैतिक की अपेक्षा अनैतिक का वर्चस्व हो रहा हो और अप्रत्यक्ष सच्चाई मनुष्य को विकृत, जड़, उदासीन अजनबी और निर्मम बना रही हो तब ये कहानियां मनुष्य को विकृति, जड़ता, उदासीनता, अजनबीपन और निर्ममता से मुक्त ही नहीं करती वरन् एक दिशाबोध कराती हैं। इन कहानियों से जाहिर है कि बाह्य यथार्थ को देखने के लिये अमानवीय प्रकृत नेत्रों की तुलना में में परिष्कृत कान की एक दूसरी ही विशिष्ट तासीर है। और इस तासीर का असर है कि ये कहानियां अपनी पूरी ताकत से पाठक को गुनने और समझने के लिये विवश करती हैं।
जो विद्वान जन या सुधी पाठक विमल मित्र के कथा-संसार से परिचित हैं वे प्रस्तुत पुस्तक के कहानी-क्रम को पढ़ते ही इस चयन की उदात्तता के प्रति आश्वस्त हो जायेंगे परन्तु इनसे इतर हिन्दी पाठक के लिये तो ये कहानियां सचमुच वरदान स्वरूप हैं।
इन कहानियों का अनुवाद इतना सहज, सरल और उत्कृष्ट है कि इस संग्रह से गुजरते हुए लगता नहीं कि अनुवादित कहानियों से गुजर रहे हैं। अनुवाद की जीवंतता रचनाकार और रचना के संप्रेषित सत्य तक पाठक को पहुंचाती ही नहीं है वरन् उसे उन मानवीय सरोकारों से रू-ब-रू भी कराती है जिनकी पैरोकारी हर जन-मन-कर्म और वचन से चाहता है। भाषा-शैली की रवानगी और सहजता इन कहानियों को आत्मसात् करने में विशेष सहयोग करती है।
हिन्दी साहित्य जगत इन कहानियों की विचार संपदा से और गौरवान्वित हुआ है इसमें सन्देह नहीं। यदि अन्य भाषाओं से भी चाहे वे हमारी भारतीय भाषाएं हों या विदेशी—ऐसे यानी ‘विमल मित्र की चुनिंदा कहानियां’ जैसे अनुवाद और चयन हिन्दी में आ सकें तो हिन्दी साहित्य समृद्ध होगा ही, हिन्दी भाषा को भी विश्व स्तरीयता प्राप्त होगी।
अनुवादक के शब्दों में—
विमल मित्र की चुनी हुई कहानियों का संकलन प्रस्तुत है। अब इन कहानियों के सम्बन्ध में क्या कहूं। सुधी पाठक-वृन्द का अभिमत ही सर्वोपरि माना जायेगा। मैं तो सिर्फ यही कह सकता हूं कि इन कहानियों का अनुवाद करते हुए मैंने विशिष्ट रसानुभूति और आत्मिक परितुष्टि प्राप्त की है। ऐसा न हो पर अनुवाद का यह श्रम-साध्य कार्य संभवतः मुझसे हो ही नहीं पाता। अपनी अनुवाद यात्रा के दौरान बहुधा इन कहानियों के पात्रों के साथ मेरा तादात्म्य कायम हुआ है। मैं उन पात्रों के साथ घुल-मिल गया हूं और उनके साथ रोता या हंसता हूं। कभी मैंने ‘बासमतिया’ के साथ-साथ चित्रकूट में विचरण किया है तो कभी लालाजी साहब के साथ छत्तीसगढ़ के एक छोटे-से ग्राम ‘टिल्डा’ में जा पहुंचा हूं। ‘पाप’ के रंजन हलदर की पीड़ा को जहां मैंने समझने की कोशिश की है, वहीं ‘बेशर्म’ के नायक ने मुझे चमत्कृत भी किया है। ‘नाम’ के परेश सान्याल, पन्ना लाल और हरीश बाबू के आचरण से जहां मैंने यह समझा है कि आज का तथाकथित भद्र-समाज कितना अभद्र है, वहीं ‘दूसरा पहलू’ की शकीला बाई के चरित्र से यह भी जान सका हूं कि ‘मुखौटा ही मुख नहीं होता !’
प्रस्तुत संग्रह में संकलित कहानी ‘महाराजा नन्दकुमार’ अर्थ-पिपासा के घिनौने और खतरनाक स्वरूप को उपस्थित करती है। यह कहानी ‘अवकाश’ में छपी थी और इस कहानी के संबंध में ‘अवकाश’ की यह टिप्पणी दृष्टव्य है—
‘अर्थ-पिपासा एक मुद्दत से प्रेत की तरह आदमी के पीछे लगी है। इतिहास के किसी टुकड़े में कभी भी किसी के कर्त्तव्यच्युत होने की घटना घटी है, उसके पीछे वित्तैषणा ही मुख्य प्रेरक तत्त्व रही है। आदमी की रोजमर्रा की जिंदगी में भी इस अनर्थमूलक अर्थ से किसी का पिण्ड नहीं छूटता। व्यक्ति के विवेक को कुंठित करने वाली इस धन-लिप्सा को ऐतिहासिक धरातल पर कथा-शिल्प में बांध रहे हैं बांग्ला के यशस्वी कथाकार श्री विमल मित्र....।’
‘महेश्वर बाबू’ की ही बात लीजिए। क्या यह सहज एक हास्य-कथा है ? शायद नहीं...! महेश्वर बाबू’ की यह उक्ति हमारे शिक्षित और सभ्य समाज के सामने एक विराट प्रश्नचिह्न खड़ा कर देती है, ‘भाई, तुम लोग इतना झगड़ते क्यों हो ? मैं तो समझता था कि जो पढ़े-लिखे नहीं होते, वही झगड़ते हैं। झगड़ा करना उन लोगों को शोभा देता है, जो कि पढ़े-लिखे नहीं हैं। तुम लोग तो सभी शिक्षित आदमी हो...।’ ‘दिल्ली की गद्दी’ जहां राजनीति के खोखलेपन को उजागर करती है, वहीं आज की छल-छन्दों की दुनिया में भी सत्य, ईमानदारी और परोपकार की राह चलने वाले लोगों का प्रतिनिधित्व करता है ‘पर हित सरिस’ का तारानाथ। नकद-नारायण को ही इस युग का नारायण मानने वाली तथा जमाने के साथ ताल-से-ताल मिलाकर मोटर और बंगला हासिल कर लेने को ही जीवन का चरम साफल्य समझने वाली इस दुनिया में सचमुच तारानाथ का कोई स्थान नहीं। वह तो इस दुनिया की नजर में सिर्फ एक बुद्धू है—निरा बुद्धू...!
विमल मित्र साहित्य को समाज-विज्ञान का शिल्प मानते हैं। नयी कहानी और पुरानी कहानी—जैसे विभाजनों में उनकी आस्था नहीं। उनका कहना है कि चांद और सूरज पुराने पड़ गये हैं ? क्या समुद्र नया नहीं रह गया ? उनकी विभिन्न कृतियों के नायकों में आप अद्भु साम्य पाएंगे। चाहे वह भूतनाथ हो, दीपांकर हो, सदानन्द हो या फिर इस संसार में संकलित कहानी का नायक तारानाथ हो। श्री विमल मित्र से अक्सर प्रश्न किया जाता है कि उनकी विभिन्न कृतियों में चरित्रों का वही दुहराव क्यों है ? विमल मित्र ने इसके जवाब में कहा है कि गंगा के अलग-अलग बहुत-से घाट होने पर भी गंगा तो एक ही है।
बांग्ला साहित्य विशेषकर विमल मित्र का कथा-साहित्य विपुल मात्रा में हिंदी में अनूदित होकर खूब पढ़ा और सराहा जा रहा है, तो उसका कारण है अनुवादकों की निष्ठा जो हिन्दी पाठक को उन कहानियों के परिवेश, वैचारिक जगत व अन्य आयामों के इतने सूक्ष्म स्तर तक ले जाते हैं जहां मूल और अनुवाद एकाकार होकर पाठकीय मनो-जगत को अपने साथ तादात्म कर लेते हैं। यही बिंदु इन कहानियों को पठनीय और संग्रहणीय बनाता है।
जीवन की, जिन्दगी की, इंसानियत की, अनेकों विविधायामी आयामों की सतरंगी आभा को उकेरती, नदी की अजस्र धारा की तरह कहीं अवरुद्, कहीं तरंगायित तो कहीं भयावह उद्दामता की कही, अनकही बाहरी-भीतरी परतों को उकेरती ये कहानियां सच में ही पाठक को दूर तक और देर तक अपने साथ बनाये रखने की क्षमता रखती हैं इसीलिये इन्हें विमल मित्र की चुनिंदा कहानियां कहा हीं नहीं जा सकता वरन् ये अपनी सार्वकालिकता में चुनिंदा और प्रतिनिधि हैं।
‘विमल मित्र की चुनिंदा कहानियां’ पुस्तक में संपादक और अनुवादक दोनों ही उपरोक्त कसौटियों पर खरे उतरे हैं। इन कहानियों से गुजरने से पहले रवीन्द्रनाथ ठाकुर के इस कथन पर विशेष गौर कर लें—‘मैं बचपन से केवल आंख के द्वारा देखने का अभ्यस्त था। आज एकाएक मैंने अपनी पूरी चेतना से देखना शुरू किया।’ तो ललाट की आंखों से देखकर समझने का गुमान कितना भ्रामक है। उनसे कुछ नहीं दिखता, केवल चैतन्य की आंखों से, आत्मा की आंखों से सत्य की झांकी मिल सकती है’ ‘सहज को दुरूह करके जब पाया जाता है, तभी पाना सार्थक होता है।’ और हम सहज में सब कुछ हथिया लेना चाहते हैं—हिमालय को, गंगा-गोदावरी को। पर हिमालय और समूची गंगा को निगलने के बाद हमारा पेट तो वैसा ही खाली रह जायेगा। पेट की क्षुधा या शरीर की क्षुधा भला कब शान्त होने वाली है। यह जठराग्नि तो हमारी आत्मा, हमारी बुद्धि तक स्वाहा कर डालेगी। और हम पश्चिम की ही नकल करने में मगन हैं, उनके मनीषियों को महिमामंडित करने में, पढ़ने में गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं।
इस सांस्कृतिक गुलामी की ‘भूल सूधार’ के रूप में प्रस्तुत पुस्तक ‘विमल मित्र की चुनिंदा कहानियां’ का संचयन है। देश मनुष्य की सृष्टि है। वह मृण्मय नहीं, चिन्मय है। यदि मनुष्य प्रकाशमान हो तभी देश प्रकाशित होता है।...देश मिट्टी से नहीं मनुष्यों से बनता है। साथ ही साथ यह भूलने से भी काम नहीं चलेगा कि माल मनुष्य का है, मनुष्य स्वयं माल नहीं है। वह अपने विश्व-जगत को केवल माल का संसार बना लेगा तो अपने आपको मनुष्य कहकर पहचानेगा कैसे ? विमल मित्र की चुनिंदा कहानियों में ठौर-ठौर ऐसा अमृत छलक रहा है। समय काटने के निमित्त, मनोरंजन की ओट में, अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर, जो हलाहल उंडेला जा रहा है, उस घातक मंत्रणा के प्रतिरोध में ये कहानियां अपनी सम्पूर्ण क्षमता के साथ खड़ी हैं।
जब नैतिक की अपेक्षा अनैतिक का वर्चस्व हो रहा हो और अप्रत्यक्ष सच्चाई मनुष्य को विकृत, जड़, उदासीन अजनबी और निर्मम बना रही हो तब ये कहानियां मनुष्य को विकृति, जड़ता, उदासीनता, अजनबीपन और निर्ममता से मुक्त ही नहीं करती वरन् एक दिशाबोध कराती हैं। इन कहानियों से जाहिर है कि बाह्य यथार्थ को देखने के लिये अमानवीय प्रकृत नेत्रों की तुलना में में परिष्कृत कान की एक दूसरी ही विशिष्ट तासीर है। और इस तासीर का असर है कि ये कहानियां अपनी पूरी ताकत से पाठक को गुनने और समझने के लिये विवश करती हैं।
जो विद्वान जन या सुधी पाठक विमल मित्र के कथा-संसार से परिचित हैं वे प्रस्तुत पुस्तक के कहानी-क्रम को पढ़ते ही इस चयन की उदात्तता के प्रति आश्वस्त हो जायेंगे परन्तु इनसे इतर हिन्दी पाठक के लिये तो ये कहानियां सचमुच वरदान स्वरूप हैं।
इन कहानियों का अनुवाद इतना सहज, सरल और उत्कृष्ट है कि इस संग्रह से गुजरते हुए लगता नहीं कि अनुवादित कहानियों से गुजर रहे हैं। अनुवाद की जीवंतता रचनाकार और रचना के संप्रेषित सत्य तक पाठक को पहुंचाती ही नहीं है वरन् उसे उन मानवीय सरोकारों से रू-ब-रू भी कराती है जिनकी पैरोकारी हर जन-मन-कर्म और वचन से चाहता है। भाषा-शैली की रवानगी और सहजता इन कहानियों को आत्मसात् करने में विशेष सहयोग करती है।
हिन्दी साहित्य जगत इन कहानियों की विचार संपदा से और गौरवान्वित हुआ है इसमें सन्देह नहीं। यदि अन्य भाषाओं से भी चाहे वे हमारी भारतीय भाषाएं हों या विदेशी—ऐसे यानी ‘विमल मित्र की चुनिंदा कहानियां’ जैसे अनुवाद और चयन हिन्दी में आ सकें तो हिन्दी साहित्य समृद्ध होगा ही, हिन्दी भाषा को भी विश्व स्तरीयता प्राप्त होगी।
अनुवादक के शब्दों में—
विमल मित्र की चुनी हुई कहानियों का संकलन प्रस्तुत है। अब इन कहानियों के सम्बन्ध में क्या कहूं। सुधी पाठक-वृन्द का अभिमत ही सर्वोपरि माना जायेगा। मैं तो सिर्फ यही कह सकता हूं कि इन कहानियों का अनुवाद करते हुए मैंने विशिष्ट रसानुभूति और आत्मिक परितुष्टि प्राप्त की है। ऐसा न हो पर अनुवाद का यह श्रम-साध्य कार्य संभवतः मुझसे हो ही नहीं पाता। अपनी अनुवाद यात्रा के दौरान बहुधा इन कहानियों के पात्रों के साथ मेरा तादात्म्य कायम हुआ है। मैं उन पात्रों के साथ घुल-मिल गया हूं और उनके साथ रोता या हंसता हूं। कभी मैंने ‘बासमतिया’ के साथ-साथ चित्रकूट में विचरण किया है तो कभी लालाजी साहब के साथ छत्तीसगढ़ के एक छोटे-से ग्राम ‘टिल्डा’ में जा पहुंचा हूं। ‘पाप’ के रंजन हलदर की पीड़ा को जहां मैंने समझने की कोशिश की है, वहीं ‘बेशर्म’ के नायक ने मुझे चमत्कृत भी किया है। ‘नाम’ के परेश सान्याल, पन्ना लाल और हरीश बाबू के आचरण से जहां मैंने यह समझा है कि आज का तथाकथित भद्र-समाज कितना अभद्र है, वहीं ‘दूसरा पहलू’ की शकीला बाई के चरित्र से यह भी जान सका हूं कि ‘मुखौटा ही मुख नहीं होता !’
प्रस्तुत संग्रह में संकलित कहानी ‘महाराजा नन्दकुमार’ अर्थ-पिपासा के घिनौने और खतरनाक स्वरूप को उपस्थित करती है। यह कहानी ‘अवकाश’ में छपी थी और इस कहानी के संबंध में ‘अवकाश’ की यह टिप्पणी दृष्टव्य है—
‘अर्थ-पिपासा एक मुद्दत से प्रेत की तरह आदमी के पीछे लगी है। इतिहास के किसी टुकड़े में कभी भी किसी के कर्त्तव्यच्युत होने की घटना घटी है, उसके पीछे वित्तैषणा ही मुख्य प्रेरक तत्त्व रही है। आदमी की रोजमर्रा की जिंदगी में भी इस अनर्थमूलक अर्थ से किसी का पिण्ड नहीं छूटता। व्यक्ति के विवेक को कुंठित करने वाली इस धन-लिप्सा को ऐतिहासिक धरातल पर कथा-शिल्प में बांध रहे हैं बांग्ला के यशस्वी कथाकार श्री विमल मित्र....।’
‘महेश्वर बाबू’ की ही बात लीजिए। क्या यह सहज एक हास्य-कथा है ? शायद नहीं...! महेश्वर बाबू’ की यह उक्ति हमारे शिक्षित और सभ्य समाज के सामने एक विराट प्रश्नचिह्न खड़ा कर देती है, ‘भाई, तुम लोग इतना झगड़ते क्यों हो ? मैं तो समझता था कि जो पढ़े-लिखे नहीं होते, वही झगड़ते हैं। झगड़ा करना उन लोगों को शोभा देता है, जो कि पढ़े-लिखे नहीं हैं। तुम लोग तो सभी शिक्षित आदमी हो...।’ ‘दिल्ली की गद्दी’ जहां राजनीति के खोखलेपन को उजागर करती है, वहीं आज की छल-छन्दों की दुनिया में भी सत्य, ईमानदारी और परोपकार की राह चलने वाले लोगों का प्रतिनिधित्व करता है ‘पर हित सरिस’ का तारानाथ। नकद-नारायण को ही इस युग का नारायण मानने वाली तथा जमाने के साथ ताल-से-ताल मिलाकर मोटर और बंगला हासिल कर लेने को ही जीवन का चरम साफल्य समझने वाली इस दुनिया में सचमुच तारानाथ का कोई स्थान नहीं। वह तो इस दुनिया की नजर में सिर्फ एक बुद्धू है—निरा बुद्धू...!
विमल मित्र साहित्य को समाज-विज्ञान का शिल्प मानते हैं। नयी कहानी और पुरानी कहानी—जैसे विभाजनों में उनकी आस्था नहीं। उनका कहना है कि चांद और सूरज पुराने पड़ गये हैं ? क्या समुद्र नया नहीं रह गया ? उनकी विभिन्न कृतियों के नायकों में आप अद्भु साम्य पाएंगे। चाहे वह भूतनाथ हो, दीपांकर हो, सदानन्द हो या फिर इस संसार में संकलित कहानी का नायक तारानाथ हो। श्री विमल मित्र से अक्सर प्रश्न किया जाता है कि उनकी विभिन्न कृतियों में चरित्रों का वही दुहराव क्यों है ? विमल मित्र ने इसके जवाब में कहा है कि गंगा के अलग-अलग बहुत-से घाट होने पर भी गंगा तो एक ही है।
बांग्ला साहित्य विशेषकर विमल मित्र का कथा-साहित्य विपुल मात्रा में हिंदी में अनूदित होकर खूब पढ़ा और सराहा जा रहा है, तो उसका कारण है अनुवादकों की निष्ठा जो हिन्दी पाठक को उन कहानियों के परिवेश, वैचारिक जगत व अन्य आयामों के इतने सूक्ष्म स्तर तक ले जाते हैं जहां मूल और अनुवाद एकाकार होकर पाठकीय मनो-जगत को अपने साथ तादात्म कर लेते हैं। यही बिंदु इन कहानियों को पठनीय और संग्रहणीय बनाता है।
जीवन की, जिन्दगी की, इंसानियत की, अनेकों विविधायामी आयामों की सतरंगी आभा को उकेरती, नदी की अजस्र धारा की तरह कहीं अवरुद्, कहीं तरंगायित तो कहीं भयावह उद्दामता की कही, अनकही बाहरी-भीतरी परतों को उकेरती ये कहानियां सच में ही पाठक को दूर तक और देर तक अपने साथ बनाये रखने की क्षमता रखती हैं इसीलिये इन्हें विमल मित्र की चुनिंदा कहानियां कहा हीं नहीं जा सकता वरन् ये अपनी सार्वकालिकता में चुनिंदा और प्रतिनिधि हैं।
-कान्ती प्रसाद शर्मा
लालजी साहब
इस बार नागपुर जाने पर उससे मुलाकात हुई। पहले-पहल मैं पहचान ही नहीं
पाया। विराट् सम्मेलन का पंडाल सजा हुआ था। असल काम चाहे जो भी क्यों न
हो, इतने लोगों का एक स्थान पर इकट्ठा होना ही अपने आप में एक बड़ी घटना
थी। अधिकांश चेहरे अजनबी ही थे। कोई भी किसी को पहचानता नहीं। पहले किसी
ने किसी को देखा तक नहीं। सुबह के नौ बजे जो मीटिंग शुरू होती, वह खत्म
होती दोपहर के एक बजे। उसके बाद फिर अपराह्न में तीन बजे से सभा आरम्भ हो
जाती। उस सभा की समाप्ति होते-होते शाम के छः बज जाते। उसके बाद रात आठ
बजे से प्रारम्भ होते सांस्कृतिक कार्यक्रम।
हम सब हजारों –हजार लोग जुटे थे—दुनिया के भिन्न-भिन्न देशों से। हम लोगों के ठहरने का और खाने-पीने का बहुत बढ़िया इंतजाम था। कहीं भी कोई शिकवा-शिकायत नहीं।
पहले ही दिन से आयोजन बहुत बढ़िया लग रहा था।
ठीक दूसरे दिन की घटना है।
मैं बिलकुल सामने की तरफ दूसरी पंक्ति में बैठा हुआ था। जो मुझे व्यक्तिगत रूप से पहचानते नहीं थे, ऐसे लोग भी आकर मुझसे बातचीत कर जाते थे। सबों ने मेरा नाम ही सुना था किन्तु देखा नहीं था कभी भी।
और फिर मैं तो सभा-समितियों में प्रायः कभी जाता ही नहीं, सभा-समितियों में जाने का मैं आदी हूं ही नहीं। एकांत में अकेले-अकेले देश-प्रदेश में घूमना ही मुझे भला लगता है। मैं जहां भी जाऊं, वहां मैं सबों को देखूं—मैं यही चाहता हूं; कोई मुझे भी देखे, यह मुझे पसंद नहीं।
जिन्दगी का तीन-चौथाई जब इसी तरह बीत गया तो बचा हुआ एक चौथाई हिस्सा भी इसी तरह बीत जाएगा—यही मैंने मान लिया है। लेकिन नागपुर आने का कारण कुछ और ही था। पहली बात तो यह है कि कलकत्ते की जिन्दगी की कुटिलता-जटिलता ने मुझे प्रायः मृतप्राय कर दिया था। मैंने उस जिन्दगी से कुछ दिनों के लिए थोड़ा अवकाश चाहा था। कलकत्ते से आमंत्रित संयोजकों में मैं ही एक मात्र बंगाली था।
लेकिन वहां जाकर भी कलकत्ते के जीवन से फिर इस तरह जुड़ जाना होगा, इसका मैंने कल्पना भी नहीं की थी।
कोई मुझसे आटोग्राफ लेने आता, तो कोई आकर मुझे प्रणाम करता। या फिर कोई नमस्कार कर अपना परिचय देता और चला जाता।
लेकिन उनके बीच से ही एक व्यक्ति ने आकर नमस्कार किया और पूछा, ‘‘मुझे पहचान पा रहे हैं क्या ?’’
स्पष्ट बंगला में प्रश्न किया गया था—उच्चारण था ठीक बंगालियों जैसा।
मैंने मुह उठाकर उसके चेहरे की तरफ देखा।
लेकिन मैं किसी भी तरह पहचान नहीं पाया।
‘‘मुझे पहचान नहीं पा रहे हैं। मैं वसंत हूं। वसंत कुमार सरकार।’’
फिर भी पहचान नहीं सका। वसंत कुमार सरकार नाम के किसी भी आदमी को कभी भी मैं जानता था, ऐसा याद नहीं आया।
मैंने कहा, ‘‘भाई, मैं तो आपको ठीक पहचान नहीं पा रहा हूं।
वसंत ने कहा, ‘‘मुझे बार-बार ‘आप’ क्यों कह रहे हैं ? क्या आपको याद नहीं कि कलकत्ते में मैं आपके घर पर जाया करता था ?’’
मैंने कहा हो सकता है, पर मुझे तो इस समय ठीक-ठीक कुछ भी याद नहीं आ रहा है।’’
वसंत ने कहा, ‘‘यह क्या ? आप इतनी जल्दी सबकुछ भूल गए ? आज से प्रायः बीस साल पहले मैंने आपसे मुलाकात की थी। क्या आपको याद नहीं आ रहा है।’’
‘‘बीस साल पहले !’’
बीस साल के बीच न जाने कितनी घटनाएं घट चुकी हैं, इस दुनिया का इतिहास-भूगोल भी कितना कुछ बदल गया है—वह सब याद रखना क्या कोई आसान बात है ?
मेरा चेहरा देखकर संभवतः वसंत समझ गया कि मैं उसे पहचान नहीं पाया था.... और यह समझ पाने पर भी इसके लिए मेरे शर्मिन्दा होने की कोई वजह नहीं थी, इसका कारण यह था कि वसंत निश्चय ही जानता होगा कि बीस साल पहले मेरे दिन-रात कैसी व्यस्तता में बीतते थे, उस समय मेरे जीवन में मात्र एक ही समस्या थी, समस्या यह कि मैं किस तरह सबकी जिम्मेदारी संभालूं।
मैंने कहा, ‘‘मुझे ठीक याद नहीं आ रहा है।’’
हम सब हजारों –हजार लोग जुटे थे—दुनिया के भिन्न-भिन्न देशों से। हम लोगों के ठहरने का और खाने-पीने का बहुत बढ़िया इंतजाम था। कहीं भी कोई शिकवा-शिकायत नहीं।
पहले ही दिन से आयोजन बहुत बढ़िया लग रहा था।
ठीक दूसरे दिन की घटना है।
मैं बिलकुल सामने की तरफ दूसरी पंक्ति में बैठा हुआ था। जो मुझे व्यक्तिगत रूप से पहचानते नहीं थे, ऐसे लोग भी आकर मुझसे बातचीत कर जाते थे। सबों ने मेरा नाम ही सुना था किन्तु देखा नहीं था कभी भी।
और फिर मैं तो सभा-समितियों में प्रायः कभी जाता ही नहीं, सभा-समितियों में जाने का मैं आदी हूं ही नहीं। एकांत में अकेले-अकेले देश-प्रदेश में घूमना ही मुझे भला लगता है। मैं जहां भी जाऊं, वहां मैं सबों को देखूं—मैं यही चाहता हूं; कोई मुझे भी देखे, यह मुझे पसंद नहीं।
जिन्दगी का तीन-चौथाई जब इसी तरह बीत गया तो बचा हुआ एक चौथाई हिस्सा भी इसी तरह बीत जाएगा—यही मैंने मान लिया है। लेकिन नागपुर आने का कारण कुछ और ही था। पहली बात तो यह है कि कलकत्ते की जिन्दगी की कुटिलता-जटिलता ने मुझे प्रायः मृतप्राय कर दिया था। मैंने उस जिन्दगी से कुछ दिनों के लिए थोड़ा अवकाश चाहा था। कलकत्ते से आमंत्रित संयोजकों में मैं ही एक मात्र बंगाली था।
लेकिन वहां जाकर भी कलकत्ते के जीवन से फिर इस तरह जुड़ जाना होगा, इसका मैंने कल्पना भी नहीं की थी।
कोई मुझसे आटोग्राफ लेने आता, तो कोई आकर मुझे प्रणाम करता। या फिर कोई नमस्कार कर अपना परिचय देता और चला जाता।
लेकिन उनके बीच से ही एक व्यक्ति ने आकर नमस्कार किया और पूछा, ‘‘मुझे पहचान पा रहे हैं क्या ?’’
स्पष्ट बंगला में प्रश्न किया गया था—उच्चारण था ठीक बंगालियों जैसा।
मैंने मुह उठाकर उसके चेहरे की तरफ देखा।
लेकिन मैं किसी भी तरह पहचान नहीं पाया।
‘‘मुझे पहचान नहीं पा रहे हैं। मैं वसंत हूं। वसंत कुमार सरकार।’’
फिर भी पहचान नहीं सका। वसंत कुमार सरकार नाम के किसी भी आदमी को कभी भी मैं जानता था, ऐसा याद नहीं आया।
मैंने कहा, ‘‘भाई, मैं तो आपको ठीक पहचान नहीं पा रहा हूं।
वसंत ने कहा, ‘‘मुझे बार-बार ‘आप’ क्यों कह रहे हैं ? क्या आपको याद नहीं कि कलकत्ते में मैं आपके घर पर जाया करता था ?’’
मैंने कहा हो सकता है, पर मुझे तो इस समय ठीक-ठीक कुछ भी याद नहीं आ रहा है।’’
वसंत ने कहा, ‘‘यह क्या ? आप इतनी जल्दी सबकुछ भूल गए ? आज से प्रायः बीस साल पहले मैंने आपसे मुलाकात की थी। क्या आपको याद नहीं आ रहा है।’’
‘‘बीस साल पहले !’’
बीस साल के बीच न जाने कितनी घटनाएं घट चुकी हैं, इस दुनिया का इतिहास-भूगोल भी कितना कुछ बदल गया है—वह सब याद रखना क्या कोई आसान बात है ?
मेरा चेहरा देखकर संभवतः वसंत समझ गया कि मैं उसे पहचान नहीं पाया था.... और यह समझ पाने पर भी इसके लिए मेरे शर्मिन्दा होने की कोई वजह नहीं थी, इसका कारण यह था कि वसंत निश्चय ही जानता होगा कि बीस साल पहले मेरे दिन-रात कैसी व्यस्तता में बीतते थे, उस समय मेरे जीवन में मात्र एक ही समस्या थी, समस्या यह कि मैं किस तरह सबकी जिम्मेदारी संभालूं।
मैंने कहा, ‘‘मुझे ठीक याद नहीं आ रहा है।’’
|
|||||
अन्य पुस्तकें
लोगों की राय
No reviews for this book