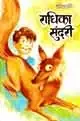|
संस्मरण >> जालक जालकशिवानी
|
444 पाठक हैं |
||||||
शिवानी के अंतर्दृष्टिपूर्ण संस्मरणों का संग्रह...
अड़तीस
भारतीय समाज में वर्णव्यवस्था आदिकाल से चली आ रही है। किन्तु यदि हम प्राचीन वर्णव्यवस्था का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें, तो यह स्पष्ट हो उठता है कि तब वर्णव्यवस्था गुण-कर्मानुसार थी। महाभारत में भी कहा गया है कि सत्य, दान, अक्रूरता, लज्जा, करुणा, तप और अद्रोह जहाँ दिखाई दें, वही ब्राह्मण है, किन्तु किसी शूद्र में ये गुण हों, तो वह शूद्र नहीं ब्राह्मण है और यदि किसी ब्राह्मण में, ब्राह्मण होकर भी ये गुण न हों तो वह ब्राह्मण नहीं है-
शूद्रे तु यद भवेल्लक्ष्य
द्विजे तच्च न दृश्यते!
न वै शूद्रो भवेच्छद्रो
ब्राह्मणो ब्राह्मणो न च!!
यही कारण है कि हमारी वर्णव्यवस्था अपनी विषमताओं के बावजूद हमें आज भी उतनी ही प्रिय है। इसमें यदि कुछ गुण न होते तो विदेशी इतिहासकार क्यों प्रशंसा करते? स्मिथ के शब्दों में, "वर्णव्यवस्था में कुछ न कुछ गुण अवश्य हैं। इसी प्रकार वह उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक सहस्रों वर्षों से विद्यमान है। यदि वर्णव्यवस्था में यह आवश्यक गुण न होता तो उसका अब तक पतन अवश्य हो गया होता।" देखा जाए तो इसी वर्णव्यवस्था ने कभी भारत को एकता के सूत्र में बाँध संस्कृति की रक्षा की थी। इसी से आश्चर्य होता है कि जिस व्यवस्था ने कभी हमारी संस्कृति की अमूल्य धरोहर को सहेजने में अपूर्व योगदान दिया था आज उसी में धुन लग गया है। आज स्वयं हम ही इस प्रथा की आलोचना करते हैं, अंतर्जातीय विवाहों के लिए पुरस्कारों की घोषणा करते हैं और जैसे भी हो, वर्णव्यवस्था के वैषम्य की एक-एक पुरानी ईंट को पटककर दूर फेंकना चाहते हैं।
प्राचीन समय में जातिबन्धन उदार थे, स्थान-स्थान पर यह उल्लेख मिलता है कि धर्माचरण से नीच वर्ण पूर्व उच्च वर्ण को प्राप्त हो जाता है, और उसकी जाति बदल जाती है। किन्तु समय के साथ-साथ हमने स्वयं ही वर्णव्यवस्था को जटिल बना लिया है। आज जाति संस्था, ब्राह्मणवादी नहीं रही। मनुस्मृति ने जो ब्राह्मणों के सर्वाधिक महत्त्व की उद्घोषणा की थी उसका स्वर अब स्वयं डूब गया है।
प्रश्न यह उठता है कि वर्णव्यवस्था की यह अधपकी खिचड़ी खाकर हम कमजोर हाजमेवाले भारतीयों को अपच होने का भय क्या और नहीं बढ़ गया?
हम अपने उदार विचारों को कितना ही प्रतिपादित करने की चेष्टा क्यों न करें, इतना हमें स्वीकार करना ही पड़ेगा कि मनुष्य के संस्कारों की गाँठ बड़ी जटिल होती है। यौवनावस्था में हम भले ही अपने अन्तर्जातीय विवाह के पक्ष में सौ-सौ पुष्ट दलीलें दे दें, जीवन की गोधूलि में हमारे दबे संस्कारों की ये ही दबी धमनियाँ बुढ़ापे में उभरकर सख्त हो गई धमनियों की ही भाँति कभी-कभी बुरी तरह धमकने लगती हैं। मेरे पति के एक मित्र ने भी, कभी 'सकामायाः सकामेन निर्मन्त्रः श्रेष्ठ उच्चते' वाला गान्धर्व विवाह किया था। वैसे तो यह प्राचीनतम विवाह प्रकारों में से एक है, हिमाचल के निकट भूभाग में अधिक प्रचलित होने के कारण, इसकी गान्धर्व नाम से प्रसिद्धि हुई। महाभारत में तो इस प्रकार के विवाह की प्रशंसा की गई है क्योंकि इसके मूल में दो व्यक्तियों का पारस्परिक प्रेम होता है, किन्तु हमारा भारतीय धार्मिक दृष्टिकोण इसे अच्छा नहीं मानता। तब हमारे समाज में इस विवाह का बहुचर्चित होना स्वाभाविक ही था, क्योंकि पात्र उच्चपदस्थ, उच्च ब्राह्मण कुल का रत्न था। पद की महत्ता एवं अर्जित वैभव-ख्याति ने मेरे पति के उक्त मित्र को समाज के बहिष्कार की भी कोई चिन्ता नहीं रहने दी, किन्तु अवकाश-प्राप्ति के पश्चात् स्वर्गादपि गरीयसी जन्मभूमि की ललक, उन्हें कभी-कभी कैसा व्याकुल कर उठती है, यह देखकर मुझे आश्चर्य भी हुआ, दुख भी। पहाड़ की सामान्य सरल जम्बू की छौंक या बड़ी-सी लोहे की कड़ाही में पकते श्यामवर्णी 'रस' की स्मृति में, उनके मुँह की लार टपकते देख मुझे बार-बार यही लगता है कि जन्मभूमि की सोंधी मिट्टी कभी न कभी मनुष्य की स्मृति के नथुने फड़काती अवश्य है। पिता की मृत्यु में उन्होंने अशौच को कोई महत्ता नहीं दी, बाल नहीं उतरवाए, मूंछे नहीं मुड़वाईं, आज वे ही असंख्य अक्षम्य त्रुटियाँ शक्तिशाली शत्रु की भाँति उनकी छाती पर चढ़ गला घोंटने लगती हैं। मनुष्य की इसी वानप्रस्थी अवस्था में, यौवनावस्था के प्रेम की मदिर मन्द सुगन्ध कपूर के चूर्ण की भाँति विलीयमान हो जाती है।
ऐसे ही मेरे पिता के एक अत्यन्त समृद्ध डाक्टर मित्र ने एक आइरिश महिला से विवाह किया था। तब मेरे पिता रामपुर नवाब के गृहमन्त्री थे और उक्त डॉक्टर थे नवाब साहब के निजी चिकित्सक। हमें डॉक्टर साहब की कोठी का साहबी परिवेश; उनकी गोरी-चिट्टी मेमसाहब मोनोग्राम वाले बैरेबटलर बहुत अच्छे लगते थे। प्रायः ही हमें उनकी आइरिश पत्नी खाने पर बुलाती और भाँति-भाँति के व्यंजनों से मेज भर देतीं। उनके स्वयं कोई सन्तान नहीं थी, इसी से हमें बड़ा दुलार करतीं। उनके बनाए केक, मेकरोनी, चीज कैबेज तो हमें बहुत रुचते, किन्तु लम्बी-लम्बी काँच की शीशियों में सिरके में डले उनके ककड़ी, सेम के विचित्र अचार देख, हमें दूर से ही उबकाई आने लगती। बार-बार वह बड़े आग्रहपूर्ण दुलार से उस अचार की फाँक हमारी प्लेट में डाल देतीं। एक दिन, जब उसी प्रेम से अचार परोस, भीतर कुछ लेने गईं तो डॉक्टर साहब का उफनता क्रोध मेज पर ही बिखर गया-"देख रहे हो पांडे," मेरे पिता से बोले, "कहती है इसके आयरलैंड का अचार है, भाड़ में जाए इसका आयरलैंड! हम तो अपने हिन्दुस्तान के सौंफ-किलौजी-तेल सनी आम की फाड़ी खाने को तरस गए! सोचते हैं, ऐसे पैर न फिसला होता तो क्या आज ये चरी-भूसा खाते?"
हमारा ही एक पठान ड्राइवर था शफीकुल बारी। एक बार कहने लगा, "बिन्नो, हमारे घर से बड़ी जिद कर रही हैं कि तुमसे मिलेंगी। कल लिवा लाएँगे।" दूसरे दिन रेशमी बुकों में सहमी-सी आकृतियाँ हमारे दीवानखाने में सिमट आईं। बुर्का उठाया तो हम देखती ही रहीं-कैसा परिचित-सा कटाव था चेहरे का, वैसा ही रंग। दोनों बहनें दो सगे भाइयों को ब्याही थीं, सुस्पष्ट उर्दू उच्चारण, उठने-बैठने का ठेठ पठानी लटका, आँखों में सुरमे की प्रगाढ़ रेखा, किन्तु चेहरे पर अजीब उदासी। उस दिन हमारे यहाँ पहाड़ का एक विशिष्ट पकवान 'सिंगल' बना था, माँ ने उनके सम्मुख प्लेट रखी ही थी कि दोनों एक-दूसरे से लिपटकर रोने लगीं। पहले तो हमारी समझ में ही नहीं आया, फिर सौ-सौ कसमें देकर, हमें उनकी दर्दनाक कहानी सुनने का सौभाग्य मिला। दोनों बहनें कुमाऊँ के सम्भ्रान्त वैश्य परिवार की थीं। जब बागेश्वर में ब्याही गईं तो वयस थी आठ और दस। उनसे बड़ी बहन भी वहीं ब्याही गई थी। एक तो पहाड़ की शाहनियाँ वैसे ही अपने सौन्दर्य के लिए प्रख्यात होती हैं, उस पर वे दोनों बहनें साक्षात् देवांगनाएँ थीं। शफीकुल बारी तब उसी इलाके में बस चलाता था। बड़ी बहन के श्वसुर की सब्जी की बहुत बड़ी दुकान थी पर दिल था बेहद छोटा। सास मारती, ससुर घर से निकाल देने की धमकी देता, अकर्मण्य जुआरी-शराबी पति, दिन-रात एक प्रख्यात वारांगना के कोठे में पड़ा रहता।
एक दिन चार बजे सुबह, वह पूर्व परिचित बारी का हाथ पकड़कर चुपचाप उसी की बस में भागकर पहुंची हैदराबाद-अपने जिस मित्र के यहाँ उसे लेकर बारी पहुँचा, वह उर्दू के किसी प्रख्यात पत्रिका का सम्पादक था। कुमाऊँ के इस तोहफे को देख वह मुग्ध ही नहीं हुआ, उसी रात धर्म-परिवर्तन करा उसने उसे अपनी बेगम बना लिया। अपने वैभव एवं समृद्धि पर स्वयं ही सौ-सौ बार निछावर होती, वह अपनी दो बहनों को भी वहाँ खींच लाई। वे ही दोनों बहनें, उस दिन हमसे मिलने आई थीं और वर्षों के विस्मृत उस पहाड़ी सिंगल को देख ऐसे टूट पड़ी थीं।
"तो अब तुम दोनों सुखी हो क्या?"
मेरी माँ ने अपना स्पष्ट तीखा प्रश्न पूछा तो दोनों तिलमिला गईं।
"सुखी?" बड़ी बहन की आँखों से फिर अविरल अश्रुधार बहने लगी थी-“वैसे तो सब सुख है माँजी, पर अपने पहाड़ को क्या कभी भूल सकती हैं? आहा रे-भट्ट के डुबके, कड़ाही-भर रस, पेड़ों से लटके काफल, हिसालू, खुबानी, सेब, गाढ़ का सुसाट (नदी की कलकल ध्वनि), दयार (देवदार) की हवा-उन्हें कैसे भूल सकती हैं हम? यही है संस्कारों की टपकन, जो मनुष्य की रक्तमज्जा में तब तक रची-बसी रहती है, जब तक वह चिता पर नहीं चढ़ता।
|
|||||
अन्य पुस्तकें
लोगों की राय
No reviews for this book











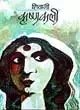
_s.webp)