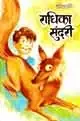|
संस्मरण >> जालक जालकशिवानी
|
444 पाठक हैं |
||||||
शिवानी के अंतर्दृष्टिपूर्ण संस्मरणों का संग्रह...
उनतालीस
स्वाधीनता प्राप्ति के सत्ताईस वर्ष पश्चात् भी कभी-कभी ऐसा प्रतीत होता है कि हमने स्वाधीनता पा तो ली, किन्तु उसका मर्म अभी भी हम हृदयंगम नहीं कर सके हैं। स्वाधीनता का यह मर्म ऐसा दुरूह नहीं है, कि हम उसे समझ ही न पाएँ। उसके इस संयम-बोध का मर्म है अत्यन्त सहज। एक लंठ गँवार देहाती भी इतना समझता है कि यदि उसकी स्वाधीनता किसी दूसरे की स्वाधीनता का क्षेत्र संकुचित करती है तो किसी की भी स्वाधीनता अक्षुण्ण नहीं रह सकती। स्वार्थपरता एवं स्वाधीनता दो तलवारों की ही भाँति एक म्यान में नहीं रह सकतीं, चाहे म्यान कितनी ही प्रशस्त क्यों न हो। आज हमारी यही उदग्र स्वार्थपरता, हमारे स्वाधीन होने पर भी रह-रहकर हमें पराधीनता के दंश से विचलित कर उठती है।
अभी कुछ ही दिन पूर्व, एक विदेशी आई.सी.एस. शासक के संस्मरण पढ़ रही थी। उसने लिखा था कि सुचारु रूप से शासनकार्य चला, एक सुयोग्य शासक की ख्याति प्राप्त करने के लिए प्रत्येक शासक में दो गुणों का होना अनिवार्य है-योग्यता एवं सहृदयसा। स्वाधीनता-प्राप्ति के पश्चात् शासक वर्ग ने अपने इन्हीं दो गुणों को लगभग खो दिया है। क्षमता पा लेना ही स्वयं में एक सम्पूर्ण उपलब्धि नहीं है, उसे अक्षुण्ण रखना ही अधिक महत्त्वपूर्ण है।
विदेशी शासकों से हमने जिस शौर्य, वीर्य, अपूर्व चरित्र एवं दृढ़ मनोबल से अपने देश को स्वाधीन किया उनकी स्याही क्रमशः धुंधली पड़ती जा रही है। पहले भय था विदेश के शत्रुओं का, आज भय है देश के शत्रुओं का। पहले की शत्रुता की सीमारेखा बड़े औदार्य से अपना परिचय भी दे देती थी किन्तु अब देश के नए शत्रुओं का छुरा कभी भी अनजान में पीठ में भी भोंका जा सकता है। विदेशी शासक अपने स्वार्थ के पहले अपने देश के स्वार्थ को ध्यान में रखते थे। हमारे देश का शोषण कर, यदि उनके देश की श्रीवृद्धि होती थी, तो वही था उनका स्वार्थ। किन्तु स्वाधीन होने पर हमारा निजी स्वार्थ ही हमारे लिए अधिक महत्त्वपूर्ण बन गया है। अपने शासन तन्त्र के मशीनी कलपुर्जी में समय-समय पर तेल देने, उसे विश्राम देने, वर्षा-आतप से उसकी रक्षा करने के महत्त्व को भी समझते थे। इसका यह अर्थ कदापि नहीं है कि विदेशी शासन ही काम्य है, किन्तु इतना हमें स्वीकार करना ही पड़ेगा कि हमारे देश में जो राजा एवं प्रजा की परिभाषा है कि राजा प्रजा का पालन करते थे, उनकी प्रत्येक सुख-सुविधा का ध्यान रखते थे, या और भी स्पष्ट कर कहें तो अधीनस्थ को अधिक योग्य बनाने के लिए ही उसे सुसभ्य जीवन जीने की प्रत्येक सुविधा प्रदान करते थे, इस परिभाषा को विदेशी शासकों ने अपने कुटिल शासन के बीच भी सदा स्मरण रखा था। विद्युत की गति से घूम रहे शासनचक्र की अस्वाभाविक तीव्रता भी कभी-कभी मानव की योग्यता, उसकी क्षमता को घटा सकती है। यह शायद हम भूल गए हैं। आज के शासनतन्त्र की शासन-प्रणाली में एक निर्जीव कम्प्यूटर की ही अस्वाभाविक तीव्रता कभी-कभी हमें आतंकित कर उठती है। जब शासनाधीन मानव मानवोचित जीवनयापन कर सकने में सक्षम हो, जब उसके व्यस्त जीवन में भी कुछ समय उसके अपने परिवार, अध्ययन, भ्रमण के लिए सुरक्षित हो या संक्षेप में कहें तो जो शासन उसे सुसभ्य जीवनयापन की स्वाधीनता प्रदान करे, वही शासन उसे वास्तविक स्वाधीनता का बोध करा सकता है।
प्रायः ही मुझे लगता है कि अफसरी वर्ग में बढ़ते रक्तचाप, अस्वाभाविक वार्धक्य, असमय के हृदयरोग की उत्सभूमि है यही शासनतन्त्र की तीव्रता। लगता है जैसे किसी कुम्भ मेले की भीड़ में क्रुद्ध नागाओं का दल उमड़ता चला जा रहा है। उस लक्ष्यहीन भीड़ के भभके में जब कोई धराशायी होकर गिर पड़ेगा तो किसी को उसे उठाने की चिन्ता भी सम्भवतः नहीं होगी और हृदयहीन तटस्थता से स्वयं उसकी अफसरी बिरादरी ही उसे भुला देगी। कोई नहीं कहेगा कि इस कठोर, परिश्रमी, निष्ठावान अफसर ने, इस ईमानदार दौड़ में अपने प्राणों की बाजी लगा दी। मनुष्य की स्मृति भी उसके जीवन की ही भाँति क्षण-भंगुर है। हम भारतीय कार्य को महत्त्व देते हैं कर्ता को नहीं। सेहरा माली गूंथता है, बाँधता है नौशा।
इस बीच मेरी भेंट कई ऐसे उच्च अफसरों की पत्नियों से हुईं, जिनके पतियों का स्थानान्तरण हुए कई महीने बीत गए किन्तु उन्हें अब तक आवास की कोई भी सुविधा प्राप्त नहीं हो सकी। 'परगेह निवासन' को हमारे शास्त्रों ने 'दुःखाति दुःख तरश्चैव' कहा है। इसी से बेचारे ऐसे स्थानांतरित अफसर जब दफ्तर से थके-माँदे लौटते हैं, तो व्यर्थ के गृहसन्धान में भटकते फिरते हैं। गृहहीनों की यह व्याधि भी बंगाल के ऐतिहासिक दुर्भिक्षों की भाँति मानवसृष्टि ही अधिक लगती है। यदि ईमानदारी से देखा जाए तो अनेक ऐसे सरकारी रिक्त फ्लैट मिलेंगे, जहाँ आजकल केवल प्रेतात्माएँ ही विचरती हैं, किन्तु प्रवेश-द्वार पर लटका रहेगा रहस्यमय ताला। जब तक गृहहीनों की यह दुर्वह वेदना स्वयं हमारे अधिकारियों के गृहस्वाच्छंद्य को पीड़ित नहीं करती तब तक इस व्याधि का कोई उपचार नहीं है। दूसरे की बिवाई की इस पीड़ा को वह अनुभव कर ही कैसे सकता है जिसकी सुकोमल एड़ी में बिवाई की एक क्षीण दरार भी कभी नहीं पड़ी? ऊँचे-ऊँचे किरायों के स्वतन्त्र फ्लैटों का स्वप्न सीमित आय का सरकारी अफसर देख नहीं सकता, रेंट कंट्रोल के मकान की प्राप्ति केवल पूर्वजन्म के पुण्य प्रताप से ही हो सकती है। तब बेचारा स्थानांतरित अफसर करे क्या? फिर जहाँ उसके दफ्तर जाने का एक नियत समय है, प्रत्यावर्तन का कोई समय नहीं है। अमानवीय धैर्य से गृहिणी अपने उस क्लांत पथिक की प्रतीक्षा में निःशब्द पलक पाँवड़े बिछाए बैठी रहती है। कहीं कुछ पूछ लिया तो खैर नहीं, जैसा कि अभी एक परिचित अफसर की पत्नी कह रही थी, "अजी इनके आने का क्या कोई वक्त है? कभी मन्त्री जी ने बुला लिया, कभी निगोड़ी कोई मीटिंग ही हो गई। सुबह नौ बजे खाकर निकल जाते हैं, दोपहर में कैंटीन से ही एक समोसा, एक स्लाइस और एक प्याला चाय मँगवाकर खा-पी लिया, घर आकर मुझे खाएँगे?" ठीक ही तो था, बेचारे थके-माँदे, झल्लाए, गृहहीन गृहस्वामी का सारा आक्रोश यदि निरीह पत्नी पर भी न उतरे तो उतरे किस पर?
हमारी पहाड़ी कहावतों में, मीठे पहाड़ी फूलों की-सी ही सहज मिठास रहती है। ऐसी ही एक कहावत कभी सुनी थी -
"कहुँणि नी संकुल तो घरै ज्वे हूँ जै के नी संकुल?"
-अजी किसी से भी नहीं जीत सका तो क्या घर में पत्नी से भी नहीं जीत सकूँगा?
|
|||||
अन्य पुस्तकें
लोगों की राय
No reviews for this book











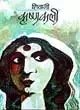
_s.webp)