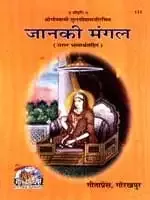|
गीता प्रेस, गोरखपुर >> जानकी मंगल जानकी मंगलहनुमानप्रसाद पोद्दार
|
313 पाठक हैं |
||||||
जानकी मंगल सरल भावार्थ सहित....
तीनि लोक अवलोकहिं नहिं उपम कोउ।
दसरथ जनक समान जनक दसरथ दोउ॥१२९॥
सजहिं सुमंगल साज रहस रनिवासहि।
गान करहिं पिकबैनि सहित परिहासहि॥१३०॥
दसरथ जनक समान जनक दसरथ दोउ॥१२९॥
सजहिं सुमंगल साज रहस रनिवासहि।
गान करहिं पिकबैनि सहित परिहासहि॥१३०॥
तीनों लोकोंको देखते हैं; [परंतु] कहीं कोई उपमा नहीं मिलती। बस, महाराज दशरथ और जनकके समान तो जनक और दशरथ दो ही हैं॥१२९।। रनिवासमें बड़ा आनन्द है। सब लोग श्रेष्ठ मंगलसाज सजा रहे हैं और कोकिलबयनी कामिनियाँ परिहास करती हुई गान कर रही हैं॥१३०॥
उमा रमादिक सुरतिय सुनि प्रमुदित भईं।
कपट नारि बर बेषं बिरचि मंडप गईं ॥१३१॥
मंगल आरति साज बरहि परिछन चलीं।
जनु बिगस रबि उदय कनक पंकज कल ॥१३२॥
कपट नारि बर बेषं बिरचि मंडप गईं ॥१३१॥
मंगल आरति साज बरहि परिछन चलीं।
जनु बिगस रबि उदय कनक पंकज कल ॥१३२॥
उसे सुनकर पार्वतीजी, लक्ष्मीजी एवं अन्य देवताओंकी स्त्रियाँ आनन्दित हुईं और स्त्रियोंको सुन्दर छद्म-वेष बनाकर मंडपमें गयीं ॥१३१॥ वे मंगल आरती सजाकर दुलहेका परिछन करने चलीं, वे ऐसी प्रसन्न हो रही हैं। मानो सोनेके कमलकी कलियाँ सूर्योदय होनेपर फूल उठी हों॥१३२॥
नखे सिख सुंदर राम रूप जब देखहिं।
सब इंद्रिन्ह महँ इंद्र बिलोचन लेखहिं॥१३३॥
परम प्रीति कुलरीति करहिं गज गामिनि।
नहिं अघाहिं अनुराग भाग भरि भामिनि ॥१३४॥
सब इंद्रिन्ह महँ इंद्र बिलोचन लेखहिं॥१३३॥
परम प्रीति कुलरीति करहिं गज गामिनि।
नहिं अघाहिं अनुराग भाग भरि भामिनि ॥१३४॥
जब वे नखसे चोटीतक श्रीरामचन्द्रजीके सुन्दर रूपको देखती हैं, तब सभी इन्द्रियों में इन्द्रके-से नेत्रोंको ही श्रेष्ठ समझती हैं। (वे सोचती हैं जिस प्रकार इन्द्रकै शरीरमें हजार नेत्र हैं, वैसे ही हमारे भी रोम-रोममें नेत्र होते तो श्रीरामचन्द्रजीकी अनुपम रूपसुधाका कुछ आस्वादन कर पातीं) ॥१३३॥ अनुराग एवं सौभाग्यसे भरी हुई वे गजगामिनी स्त्रियाँ परम प्रीतिपूर्वक कुलाचार करती हैं किंतु अघाती नहीं॥१३४॥
नेगचारु कहँ नागरि गहरु न लावहिं।
निरखि निरखि आनंद सुलोचनि पावहिं॥१३५॥
करि आरती निछावरि बरहि निहारहिं।
प्रेम मगन प्रमदागन तन न सँभारहिं॥१३६॥
निरखि निरखि आनंद सुलोचनि पावहिं॥१३५॥
करि आरती निछावरि बरहि निहारहिं।
प्रेम मगन प्रमदागन तन न सँभारहिं॥१३६॥
वे चतुरा स्त्रियाँ रीति-रस्ममें देरी नहीं लगातीं, बार-बार श्रीरघुनाथजीको देख करके सुलोचना स्त्रियाँ [महान्] आनन्दका अनुभव करती हैं॥१३५॥ आरती और निछावर करके वे दुलहाको निरखती हैं और प्रेममें मग्न हो जानेसे वे प्रेम-मसे छकी युवती स्त्रियाँ अपने शरीरको भी नहीं सँभाल पातीं ॥१३६॥
दो०-नहिं तन सम्हारहिं छबि निहारहिं निमिष रिपु जनु रनु जए।
चक्रवै लोचन राम रूप सुराज सुख भोगी भए॥
तब जनक सहित समाज राजहि उचित रुचिरासन दए।
कौसिक बसिष्ठहि पूजि पूजे रांउ है अंबर नए ॥१७॥
चक्रवै लोचन राम रूप सुराज सुख भोगी भए॥
तब जनक सहित समाज राजहि उचित रुचिरासन दए।
कौसिक बसिष्ठहि पूजि पूजे रांउ है अंबर नए ॥१७॥
वे अपने शरीरको नहीं सँभाल पातीं। भगवान् की शोभा [एकटक होकर] निहारती हैं। ऐसा जान पड़ता है, मानो उन्होंने पलकरूपी शत्रुओंको रणमें जीत लिया है। इससे उनके नेत्ररूपी चक्रवर्ती राम-छबिरूप सुराज्यके सुखके भोगी हुए हैं। तब जनकजीने समाजसहित महाराज दशरथको सुन्दर आसन दिये और कौशिकमुनि तथा वसिष्ठजीकी पूजा करके नवीन वस्त्र अर्पण कर महाराज दशरथकी पूजा की ॥१७॥
|
|||||
अन्य पुस्तकें
लोगों की राय
No reviews for this book