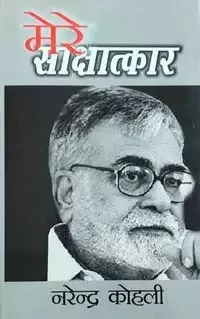|
उपन्यास >> दीक्षा दीक्षानरेन्द्र कोहली
|
|
||||||
दीक्षा
''पुत्र! मेरी कथा क्या होगी।'' अहल्या का स्वर गंभीर था, किंतु उदास नहीं, ''कितने ही समय तक मैं अपनी कुटिया से नहीं निकली। अपनी शैया पर पड़ी-पड़ी रोती रही। पर जब रो-रोकर मन की पीड़ा बहा चुकी और भूख-प्यास से पीड़ित हुई, तो उठना ही पड़ा। मेरे पास डूंडी और दो-चार गाएं थीं, फलों के कुछ वृक्ष थे, आश्रम में साग-सब्जी थी। मुझे उन सबकी रक्षा करनी थी, ताकि वे मेरी रक्षा कर सकें। मैं इन्हीं कामों में लगी रही। खाली समय में बैठकर, कभी पुरानी बातें और कभी अपने प्रियजनों की याद कर लेती; और यदि मन मानता तो ब्रह्मा का ध्यान भी करती। पुत्र! इन दिनों मैं आश्रम से बाहर कभी नहीं निकलती।
''पर लक्ष्मण, दो-तीन सप्ताह के पश्चात् एक दिन मैं कुछ अस्वस्थ हो गई। तेज ज्वर चढ़ आया और सिर पीड़ा से फटने लगा। जब तक सहन कर सकती थी, किया; किंतु जब कष्ट असहनीय हो उठा तो मैंने आश्रम के बाहर के किसी ग्राम में, किसी वैद्य की सहायता लेने की सोची। पुत्र! बिना सोचे-समझे मैं ज्वर की अवस्था में चल पड़ी। मुझे दिशा का कोई ज्ञान नहीं था, दूरी का पता नहीं था। पर मैं चलती गई।
''पहले ग्राम में जो पहला घर मुझे दिखा, मैंने उसी के द्वार पर थाप दी। द्वार खुला। एक प्रौढ़ व्यक्ति बाहर निकला। उसने मुझे पहचानकर ऐसी चीख मारी, जैसे कोई प्रेत देख लिया हो। लोग चीखते-चिल्लाते घरों से निकल आए। मैं उनकी ओर बढ़ती तो वे भाग जाते। घर में घुस जाती तो वे अपने घर-द्वार छोड़कर निकल जाते। मुझसे दूर रहकर, मेरी छाया से भी बचते हुए, वह लोग चिल्ला रहे थे, शोर मचा रहे थे। दो-एक ढेले भी मेरे सिर पर लगे।...''
''ढेले!'' लक्ष्मण बोले, ''कितने दुष्ट हैं लोग!''
''उन्हें क्या दोष लक्ष्मण!'' अहल्या बोली, ''पता नहीं वह कौन थे, पर भोले और अनजान लोग थे। मुझे पतिता घोषित करने वाले तो कोई ओर थे-ऋषि-मुनि, आचार्य, विद्वान, समाज-नियंता...पर खैर, मैं आश्रम में लौट आई। शैया पर पड़े-पड़े, दो दिनों में ज्वर अपने-आप ही उतर गया। तब से मैं अपने आश्रम से बाहर कभी नहीं गई। बाहर से, आश्रम के भीतर भी कोई नहीं आया...यह वस्त्र भी वत्स...'' अहल्या ने उत्तरीय हाथ में पकड़कर दिखाया, ''स्वयं बोई कपास से काता और बुना गया है।...इस कथा में कोई मोड़ नहीं है पुत्र! पच्चीस वर्षों में पहला मोड़, तुम लोगों ने यहां आकर दिया है...।''
''आप तो मुझे बहुत भली लगती हैं देवि!'' लक्ष्मण बोले, ''आपकी जगह मैं होता तो ऋषि गौतम और शतानन्द को कभी न जाने देता, यदि वे चले जाते तो उन्हें कभी क्षमा न करता...''
अहल्या हंसी, ''मैं भी ऐसा ही करती लक्ष्मण। यदि उनके मन में मेरे प्रति तनिक भी विरोध होता। पर उनके मन में विरोध नहीं था, द्वेष नहीं था। उन्हें मैंने भेजा है, और वे आज भी मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं...इसीलिए तो मैं भी जाने को आतुर हूं...।''
''तो उठो देवि!'' विश्वामित्र बोले, ''हम तुम्हें ऋषि गौतम को सौंपते हुए ही जनकपुर जाएंगे।''
|
|||||
- प्रथम खण्ड - एक
- दो
- तीन
- चार
- पांच
- छः
- सात
- आठ
- नौ
- दस
- ग्यारह
- द्वितीय खण्ड - एक
- दो
- तीन
- चार
- पांच
- छः
- सात
- आठ
- नौ
- दस
- ग्यारह
- बारह
- तेरह